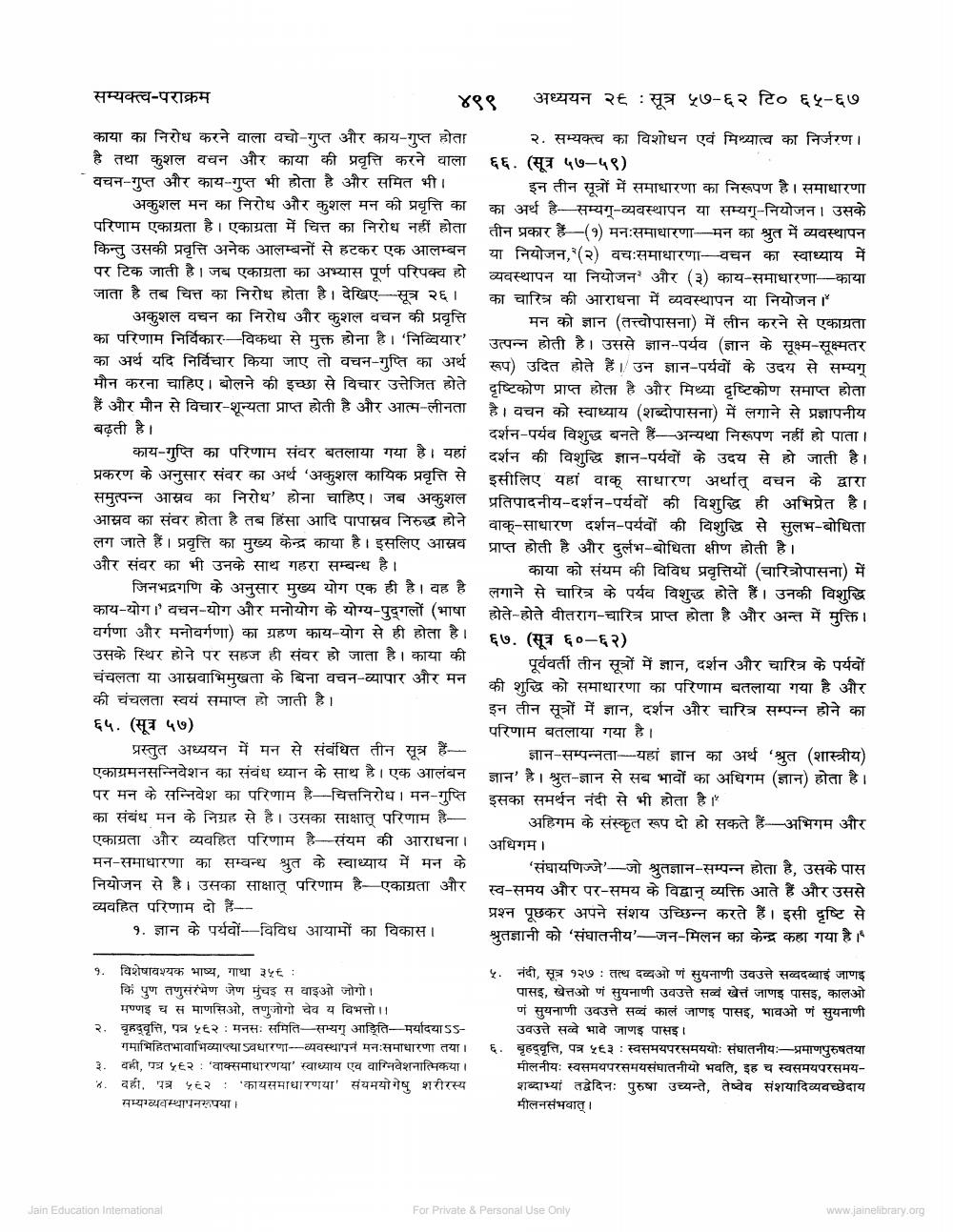________________
सम्यक्त्व-पराक्रम
४९९ अध्ययन २६ : सूत्र ५७-६२ टि० ६५-६७ काया का निरोध करने वाला वचो-गुप्त और काय-गुप्त होता २. सम्यक्त्व का विशोधन एवं मिथ्यात्व का निर्जरण। है तथा कुशल वचन और काया की प्रवृत्ति करने वाला ६६. (सूत्र ५७-५९) वचन-गुप्त और काय-गुप्त भी होता है और समित भी।
इन तीन सूत्रों में समाधारणा का निरूपण है। समाधारणा अकुशल मन का निरोध और कुशल मन की प्रवृत्ति का का अर्थ है-सम्यग-व्यवस्थापन या सम्यग्-नियोजन। उसके परिणाम एकाग्रता है। एकाग्रता में चित्त का निरोध नहीं होता तीन प्रकार हैं-(१) मनःसमाधारणा-मन का श्रुत में व्यवस्थापन किन्तु उसकी प्रवृत्ति अनेक आलम्बनों से हटकर एक आलम्बन या नियोजन, (२) वचःसमाधारणा-वचन का स्वाध्याय में पर टिक जाती है। जब एकाग्रता का अभ्यास पूर्ण परिपक्व हो व्यवस्थापन या नियोजन और (३) काय-समाधारणा–काया जाता है तब चित्त का निरोध होता है। देखिए-सूत्र २६ । का चारित्र की आराधना में व्यवस्थापन या नियोजन।
अकुशल वचन का निरोध और कुशल वचन की प्रवृत्ति मन को ज्ञान (तत्त्वोपासना) में लीन करने से एकाग्रता का परिणाम निर्विकार-विकथा से मुक्त होना है। 'निम्वियार' उत्पन्न होती है। उससे ज्ञान-पर्यव (ज्ञान के सूक्ष्म-सूक्ष्मतर का अर्थ यदि निर्विचार किया जाए तो वचन-गुप्ति का अर्थ रूप) उदित होते हैं। उन ज्ञान-पर्यवों के उदय से सम्यग् मौन करना चाहिए। बोलने की इच्छा से विचार उत्तेजित होते दृष्टिकोण प्राप्त होता है और मिथ्या दृष्टिकोण समाप्त होता हैं और मौन से विचार-शून्यता प्राप्त होती है और आत्म-लीनता है। वचन को स्वाध्याय (शब्दोपासना) में लगाने से प्रज्ञापनीय बढ़ती है।
दर्शन-पर्यव विशुद्ध बनते हैं—अन्यथा निरूपण नहीं हो पाता। काय-गुप्ति का परिणाम संवर बतलाया गया है। यहां दर्शन की विशुद्धि ज्ञान-पर्यवों के उदय से हो जाती है। प्रकरण के अनुसार संवर का अर्थ 'अकुशल कायिक प्रवृत्ति से इसीलिए यहां वाक साधारण अर्थात् वचन के द्वारा समत्पन्न आस्रव का निरोध' होना चाहिए। जब अकुशल प्रतिपादनीय-दर्शन-पर्यवों की विशद्धि ही अभिप्रेत है। आस्तव का संवर होता है तब हिंसा आदि पापानव निरुद्ध होने वाक-साधारण दर्शन-पर्यवों की विशुद्धि से सुलभ-बोधिता लग जाते हैं। प्रवृत्ति का मुख्य केन्द्र काया है। इसलिए आम्नव प्राप्त होती है और दर्लभ-बोधिता क्षीण होती है। और संवर का भी उनके साथ गहरा सम्बन्ध है।
काया को संयम की विविध प्रवृत्तियों (चारित्रोपासना) में जिनभद्रगणि के अनुसार मुख्य योग एक ही है। वह है लगाने से चारित्र के पर्यव विशुद्ध होते हैं। उनकी विशुद्धि काय-योग।' वचन-योग और मनोयोग के योग्य-पुद्गलों (भाषा होते-होते वीतराग-चारित्र प्राप्त होता है और अन्त में मुक्ति। वर्गणा और मनोवर्गणा) का ग्रहण काय-योग से ही होता है। EG (सन ED_ER) उसके स्थिर होने पर सहज ही संवर हो जाता है। काया की
पूर्ववर्ती तीन सूत्रों में ज्ञान, दर्शन और चारित्र के पर्यवों चंचलता या आस्रवाभिमुखता के बिना वचन-व्यापार और मन
की शुद्धि को समाधारणा का परिणाम बतलाया गया है और की चंचलता स्वयं समाप्त हो जाती है।
इन तीन सूत्रों में ज्ञान, दर्शन और चारित्र सम्पन्न होने का ६५. (सूत्र ५७)
परिणाम बतलाया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में मन से संबंधित तीन सूत्र हैं- ज्ञान-सम्पन्नता----यहां ज्ञान का अर्थ 'श्रुत (शास्त्रीय) एकाग्रमनसन्निवेशन का संबंध ध्यान के साथ है। एक आलंबन ज्ञान' है। श्रृत-ज्ञान से सब भावों का अधिगम (ज्ञान) होता है। पर मन के सन्निवेश का परिणाम है--चित्तनिरोध। मन-गुप्ति इसका समर्थन नंदी से भी होता है। का संबंध मन के निग्रह से है। उसका साक्षात् परिणाम है- अहिगम के संस्कृत रूप दो हो सकते हैं-अभिगम और एकाग्रता और व्यवहित परिणाम है--संयम की आराधना। अधिगम। मन-समाधारणा का सम्बन्ध श्रुत के स्वाध्याय में मन के 'संघायणिज्जे'-जो श्रुतज्ञान-सम्पन्न होता है, उसके पास नियोजन से है। उसका साक्षात परिणाम है—एकाग्रता और स्व-समय और पर-समय के विद्वान् व्यक्ति आते हैं और उससे व्यवहित परिणाम दो हैं
प्रश्न पूछकर अपने संशय उच्छिन्न करते हैं। इसी दृष्टि से १. ज्ञान के पर्यवों-विविध आयामों का विकास।
श्रुतज्ञानी को 'संघातनीय'—जन-मिलन का केन्द्र कहा गया है।
१. विशेषावश्यक भाष्य, गाथा ३५६ :
५. नंदी, सूत्र १२७ : तत्थ दव्वओ णं सुयनाणी उवउत्ते सव्वदचाई जाणइ कि पुण तणुसरंभेण जेण मुंचइ स वाइओ जोगो।
पासइ, खेत्तओ णं सुयनाणी उवउत्ते सव्वं खेत्तं जाणइ पासइ, कालओ मण्णइ च स माणसिओ, तणुजोगो चेव य विभत्तो।।
णं सुयनाणी उवउत्ते सव्वं कालं जाणइ पासइ, भावओ णं सुयनाणी २. वृहद्वृत्ति, पत्र ५६२ : मनसः समिति-सम्यग् आति -मर्यादयाऽऽ- उवउत्ते सव्वे भावे जाणइ पासइ।
गमाभिहितभावाभिव्याप्याऽवधारणा-व्यवस्थापन मनःसमाधारणा तया। ६. बृहवृत्ति, पत्र ५६३ : स्वसमयपरसमययोः संघातनीयः-प्रमाणपुरुषतया ३. वही, पत्र ५६२ : 'वाक्समाधारणया' स्वाध्याय एव वाग्निवेशनात्मिकया। मीलनीयः स्वसमयपरसमयसंघातनीयो भवति, इह च स्वसमयपरसमय४. वही, पत्र ५८२ : 'कायसमाधारणया' संयमयोगेषु शरीरस्य शब्दाभ्यां तद्वेदिनः पुरुषा उच्यन्ते, तेष्वेव संशयादिव्यवच्छेदाय सभ्यग्व्यवस्थापनरूपया।
मीलनसंभवात्।
Jain Education Intemational
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org