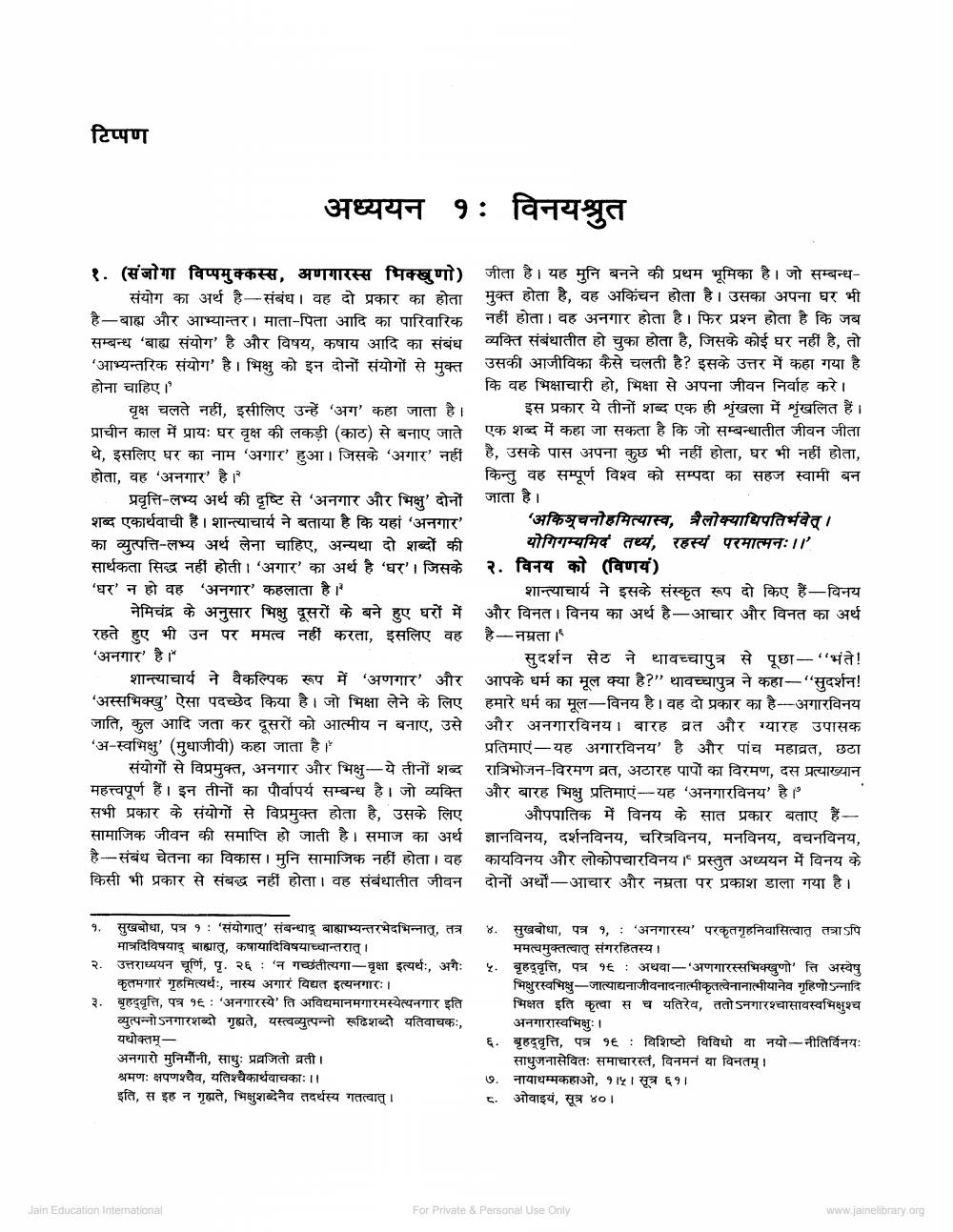________________
टिप्पण
अध्ययन
१. ( संजोगा विप्पमुक्कस्स, अणगारस्स भिक्खुणो ) संयोग का अर्थ है— संबंध । वह दो प्रकार का होता है - बाह्य और आभ्यान्तर । माता-पिता आदि का पारिवारिक सम्बन्ध 'बाह्य संयोग' है और विषय, कषाय आदि का संबंध 'आभ्यन्तरिक संयोग' है। भिक्षु को इन दोनों संयोगों से मुक्त होना चाहिए।'
वृक्ष चलते नहीं, इसीलिए उन्हें 'अग' कहा जाता है। प्राचीन काल में प्रायः घर वृक्ष की लकड़ी (काठ) से बनाए जाते थे, इसलिए घर का नाम 'अगार' हुआ। जिसके 'अगार' नहीं होता, वह 'अनगार' है ।"
१ :
प्रवृत्ति - लभ्य अर्थ की दृष्टि से 'अनगार और भिक्षु' दोनों शब्द एकार्थवाची हैं। शान्त्याचार्य ने बताया है कि यहां 'अनगार' का व्युत्पत्ति-लभ्य अर्थ लेना चाहिए, अन्यथा दो शब्दों की सार्थकता सिद्ध नहीं होती। 'अगार' का अर्थ है 'घर'। जिसके 'घर' न हो वह 'अनगार' कहलाता है।'
नेमिचंद्र के अनुसार भिक्षु दूसरों के बने हुए घरों में रहते हुए भी उन पर ममत्व नहीं करता, इसलिए वह 'अनगार' है। *
शान्त्याचार्य ने वैकल्पिक रूप में 'अणगार' और 'अस्सभिक्खु' ऐसा पदच्छेद किया है। जो भिक्षा लेने के लिए जाति, कुल आदि जता कर दूसरों को आत्मीय न बनाए, उसे 'अ-स्वभिक्षु' (मुधाजीवी) कहा जाता है।
संयोगों से विप्रमुक्त, अनगार और भिक्षु ये तीनों शब्द महत्त्वपूर्ण हैं। इन तीनों का पौर्वापर्य सम्बन्ध है । जो व्यक्ति सभी प्रकार के संयोगों से विप्रमुक्त होता है, उसके लिए सामाजिक जीवन की समाप्ति हो जाती है। समाज का अर्थ है - संबंध चेतना का विकास। मुनि सामाजिक नहीं होता। वह किसी भी प्रकार से संबद्ध नहीं होता। वह संबंधातीत जीवन
१. सुखबोधा, पत्र १ : 'संयोगात्' संबन्धाद् बाह्याभ्यन्तरभेदभिन्नात्, तत्र मात्रदिविषयाद् बाह्यात्, कषायादिविषयाच्चान्तरात् ।
२.
उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ. २६ : 'न गच्छंतीत्यगा- वृक्षा इत्यर्थः, अगैः कृतमगारं गृहमित्यर्थः, नास्य अगारं विद्यत इत्यनगारः ।
३. बृहद्वृत्ति, पत्र १६ : 'अनगारस्ये' ति अविद्यमानमगारमस्यैत्थनगार इति व्युत्पन्नोऽनगारशब्दो गृह्यते, यस्त्वव्युत्पन्नो रूढिशब्दो यतिवाचकः, यथोक्तम्
अनगारी मुनिर्मीनी, साधुः प्रव्रजितो व्रती ।
श्रमणः क्षपणश्चैव, यतिश्चैकार्थवाचकाः ।।
इति, स इह न गृह्यते, भिक्षुशब्देनैव तदर्थस्य गतत्वात् ।
Jain Education International
विनयश्रुत
जीता है। यह मुनि बनने की प्रथम भूमिका है। जो सम्बन्धमुक्त होता है, वह अकिंचन होता है। उसका अपना घर भी नहीं होता। वह अनगार होता है। फिर प्रश्न होता है कि जब व्यक्ति संबंधातीत हो चुका होता है, जिसके कोई घर नहीं है, तो उसकी आजीविका कैसे चलती है? इसके उत्तर में कहा गया है। कि वह भिक्षाचारी हो, भिक्षा से अपना जीवन निर्वाह करे ।
इस प्रकार ये तीनों शब्द एक ही श्रृंखला में श्रृंखलित हैं। एक शब्द में कहा जा सकता है कि जो सम्बन्धातीत जीवन जीता है, उसके पास अपना कुछ भी नहीं होता, घर भी नहीं होता, किन्तु वह सम्पूर्ण विश्व को सम्पदा का सहज स्वामी बन जाता है।
'अकिञ्चनो हमित्यास्व, त्रैलोक्याधिपतिर्भवेत् । योगिगम्यमिदं तथ्यं, रहस्यं परमात्मनः ।।' २. विनय को (विणयं)
शान्त्याचार्य ने इसके संस्कृत रूप दो किए हैं- विनय और विनत । विनय का अर्थ है - आचार और विनत का अर्थ है - नम्रता । "
सुदर्शन सेठ ने थावच्चापुत्र से पूछा - "भंते! आपके धर्म का मूल क्या है?" थावच्चापुत्र ने कहा- "सुदर्शन ! हमारे धर्म का मूल - विनय है। वह दो प्रकार का है-अगारविनय और अनगारविनय । बारह व्रत और ग्यारह उपासक प्रतिमाएं - यह अगारविनय' है और पांच महाव्रत, छठा रात्रिभोजन- विरमण व्रत, अठारह पापों का विरमण, दस प्रत्याख्यान और बारह भिक्षु प्रतिमाएं - यह 'अनगारविनय' है।"
औपपातिक में विनय के सात प्रकार बताए हैंज्ञानविनय, दर्शनविनय, चरित्रविनय, मनविनय, वचनविनय, कायविनय और लोकोपचारविनय । प्रस्तुत अध्ययन में विनय के दोनों अर्थों - आचार और नम्रता पर प्रकाश डाला गया है।
४. सुखबोधा, पत्र १, 'अनगारस्य' परकृतगृहनिवासित्वात् तत्राऽपि ममत्वमुक्तत्वात् संगरहितस्य ।
५. बृहद्वृत्ति, पत्र १६ अथवा - - 'अणगारस्सभिक्खुणो' त्ति अस्वेषु मिधुरस्वभिषु जात्याद्यनाजीवनादनात्मीकृतत्वेनानात्मीयानेव गृहिणीनादि भिक्षत इति कृत्वा स च यतिरेव ततोऽनगारश्चासावस्वभिक्षुश्च अनगारास्वभिक्षुः ।
६. बृहद्वृत्ति, पत्र १६ : विशिष्टो विविधो वा नयो– नीतिर्विनयः साधुजनासेवितः समाचारस्तं विनमनं वा विनतम् ।
७. नायाथम्मकहाओ, ११५। सूत्र ६१ ।
८.
ओवाइयं, सूत्र ४०।
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org