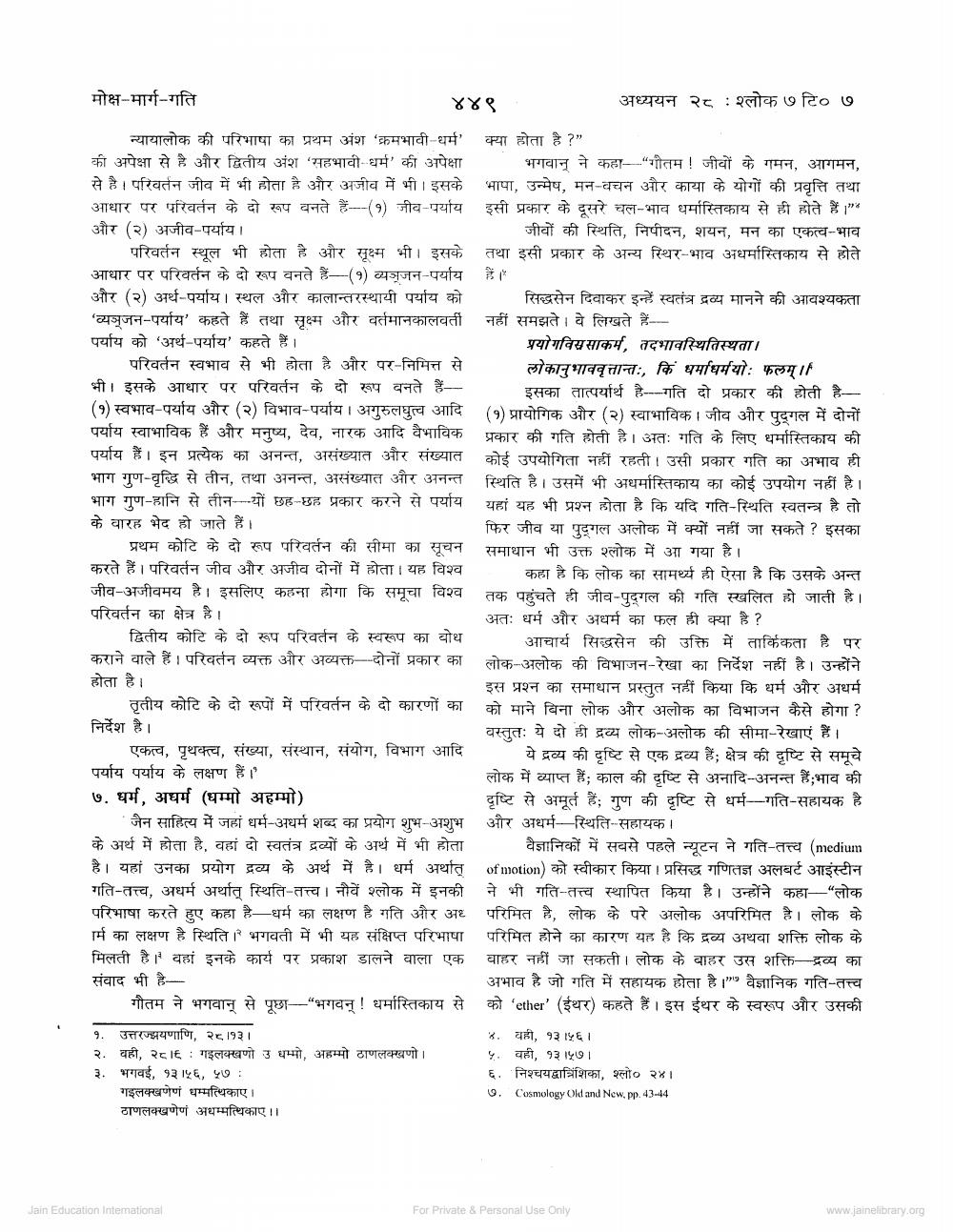________________
मोक्ष-मार्ग-गति
४४९
अध्ययन २८ : श्लोक ७ टि०७
न्यायालोक की परिभाषा का प्रथम अंश 'क्रमभावी-धर्म' क्या होता है?" की अपेक्षा से है और द्वितीय अंश 'सहभावी-धर्म' की अपेक्षा भगवान् ने कहा-“गीतम! जीवों के गमन, आगमन, से है। परिवर्तन जीव में भी होता है और अजीब में भी। इसके भाषा, उन्मेष, मन-बचन और काया के योगों की प्रवृत्ति तथा आधार पर परिवर्तन के दो रूप बनते हैं--(१) जीव-पर्याय इसी प्रकार के दूसरे चल-भाव धर्मास्तिकाय से ही होते हैं।" और (२) अजीव-पर्याय।
जीवों की स्थिति, निषीदन, शयन, मन का एकत्व-भाव परिवर्तन स्थूल भी होता है और सूक्ष्म भी। इसके तथा इसी प्रकार के अन्य स्थिर-भाव अधर्मास्तिकाय से होते आधार पर परिवर्तन के दो रूप बनते हैं—(१) व्य जन-पर्याय हैं।"
और (२) अर्थ-पर्याय। स्थल और कालान्तरस्थायी पर्याय को सिद्धसेन दिवाकर इन्हें स्वतंत्र द्रव्य मानने की आवश्यकता 'व्यञ्जन-पर्याय' कहते हैं तथा सूक्ष्म और वर्तमानकालवी नहीं समझते। वे लिखते हैंपर्याय को 'अर्थ-पर्याय' कहते हैं।
प्रयोगविससाकर्म, तदभावस्थितिस्थता। परिवर्तन स्वभाव से भी होता है और पर-निमित्त से
लोकानुभाववृत्तान्त:, किं धर्माधर्मयोः फलम्।। भी। इसके आधार पर परिवर्तन के दो रूप बनते हैं
इसका तात्पर्यार्थ है---गति दो प्रकार की होती है(१) स्वभाव-पर्याय और (२) विभाव-पर्याय । अगुरुलघुत्व आदि (१) प्रायोगिक और (२) स्वाभाविक । जीव और पुद्गल में दोनों पर्याय स्वाभाविक हैं और मनुष्य, देव, नारक आदि वैभाविक प्रकार की गति होती है। अतः गति के लिए धर्मास्तिकाय की पर्याय हैं। इन प्रत्येक का अनन्त, असंख्यात और संख्यात कोई उपयोगिता नहीं रहती। उसी प्रकार गति का अभाव ही भाग गुण-वृद्धि से तीन, तथा अनन्त, असंख्यात और अनन्त स्थिति है। उसमें भी अधर्मास्तिकाय का कोई उपयोग नहीं है। भाग गुण-हानि से तीन-यों छह-छह प्रकार करने से पयोय यहां यह भी प्रश्न होता है कि यदि गति-स्थिति स्वतन्त्र है तो के वारह भेद हो जाते हैं।
फिर जीव या पुद्गल अलोक में क्यों नहीं जा सकते? इसका प्रथम कोटि के दो रूप परिवर्तन की सीमा का सूचन समाधान भी उक्त श्लोक में आ गया है। करते हैं। परिवर्तन जीव और अजीव दोनों में होता। यह विश्व कहा है कि लोक का सामर्थ्य ही ऐसा है कि उसके अन्त जीव-अजीवमय है। इसलिए कहना होगा कि समूचा विश्व तक पहुंचते ही जीव-पदगल की गति स्खलित हो जाती है। परिवर्तन का क्षेत्र है।
अतः धर्म और अधर्म का फल ही क्या है? द्वितीय कोटि के दो रूप परिवर्तन के स्वरूप का बोध आचार्य सिद्धसेन की उक्ति में तार्किकता है पर कराने वाले हैं। परिवर्तन व्यक्त और अव्यक्त-दोनों प्रकार का लोक-अलोक की विभाजन-रेखा का निर्देश नहीं है। उन्होंने होता है।
इस प्रश्न का समाधान प्रस्तुत नहीं किया कि धर्म और अधर्म ततीय कोटि के दो रूपों में परिवर्तन के दो कारणों का को माने बिना लोक और अलोक का विभाजन कैसे होगा? निर्देश है।
वस्तुतः ये दो ही द्रव्य लोक-अलोक की सीमा-रेखाएं हैं। एकत्व, पृथक्त्व, संख्या, संस्थान, संयोग, विभाग आदि ये द्रव्य की दृष्टि से एक द्रव्य हैं; क्षेत्र की दृष्टि से समूचे पर्याय पर्याय के लक्षण हैं।'
लोक में व्याप्त हैं; काल की दृष्टि से अनादि-अनन्त हैं;भाव की ७. धर्म, अधर्म (धम्मो अहम्मो)
दृष्टि से अमूर्त हैं; गुण की दृष्टि से धर्म-गति-सहायक है जैन साहित्य में जहां धर्म-अधर्म शब्द का प्रयोग शुभ-अशुभ और अधर्म-स्थिति-सहायक। के अर्थ में होता है, वहां दो स्वतंत्र द्रव्यों के अर्थ में भी होता वैज्ञानिकों में सबसे पहले न्यूटन ने गति-तत्त्व (medium है। यहां उनका प्रयोग द्रव्य के अर्थ में है। धर्म अर्थात् of motion) को स्वीकार किया। प्रसिद्ध गणितज्ञ अलबर्ट आइंस्टीन गति-तत्त्व, अधर्म अर्थात् स्थिति-तत्त्व। नौवें श्लोक में इनकी ने भी गति-तत्त्व स्थापित किया है। उन्होंने कहा—“लोक परिभाषा करते हुए कहा है-धर्म का लक्षण है गति और अ परिमित है, लोक के परे अलोक अपरिमित है। लोक के गर्म का लक्षण है स्थिति। भगवती में भी यह संक्षिप्त परिभाषा परिमित होने का कारण यह है कि द्रव्य अथवा शक्ति लोक के मिलती है। वहां इनके कार्य पर प्रकाश डालने वाला एक बाहर नहीं जा सकती। लोक के बाहर उस शक्ति-द्रव्य का संवाद भी है
अभाव है जो गति में सहायक होता है। वैज्ञानिक गति-तत्त्व गौतम ने भगवान् से पूछा-"भगवन् ! धर्मास्तिकाय से को 'ether' (ईथर) कहते हैं। इस ईथर के स्वरूप और उसकी
१. उत्तरज्झयणाणि, २८।१३। २. वही, २८६ : गइलक्खणो उ धम्मो, अहम्मो ठाणलक्खणो। ३. भगवई, १३।५६, ५७ :
गइलक्खणेणं धम्मत्थिकाए। ठाणलक्खणेणं अधम्मत्थिकाए।।
४. वही, १३५६। ५. वही, १३१५७। ६. निश्चयद्वात्रिंशिका, श्लो० २४। ७. Cosmology od and New. pp. 43-44
Jain Education Intemational
For Private & Personal use only
www.jainelibrary.org