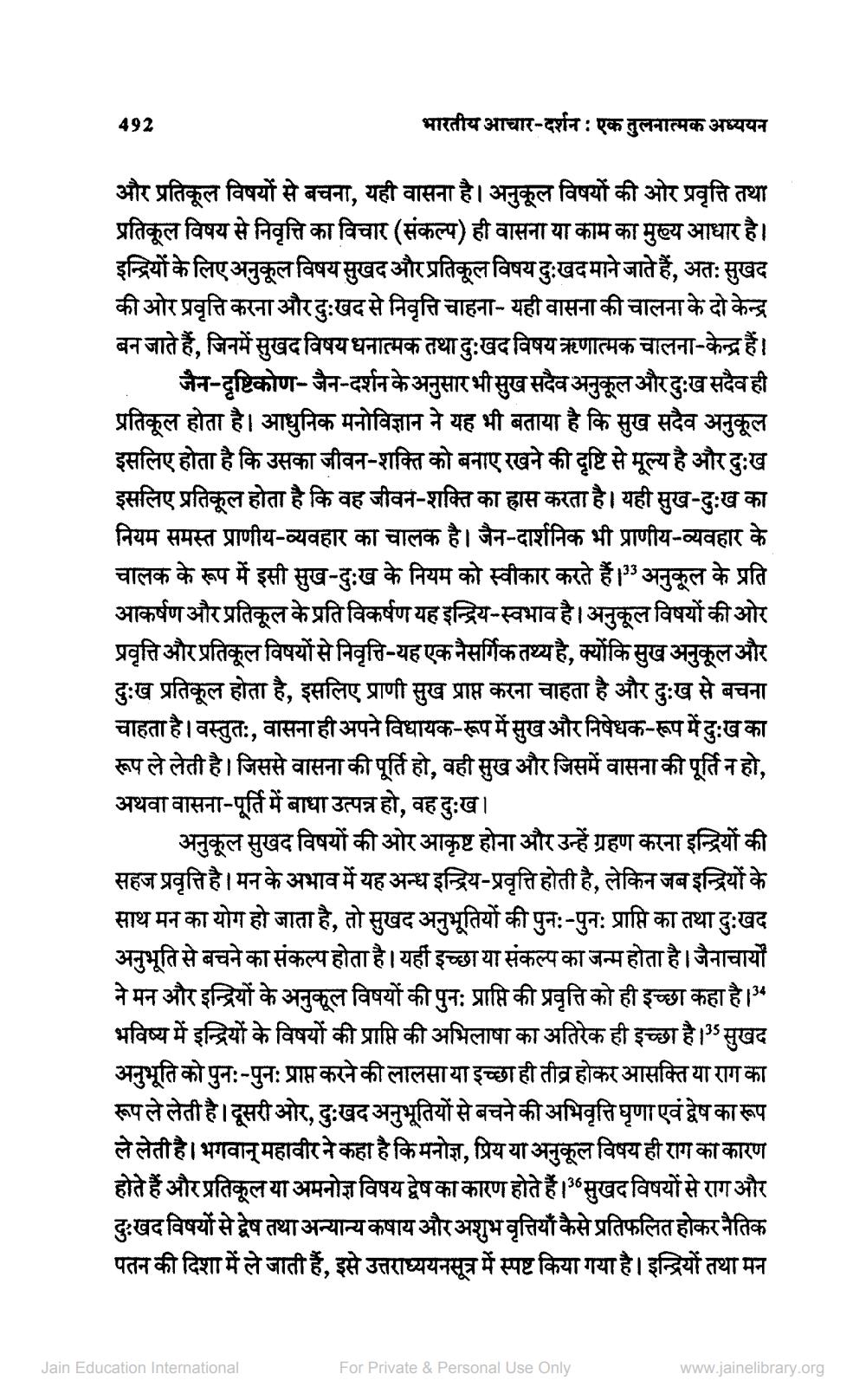________________
492
भारतीय आचार-दर्शन : एक तुलनात्मक अध्ययन
और प्रतिकूल विषयों से बचना, यही वासना है। अनुकूल विषयों की ओर प्रवृत्ति तथा प्रतिकूल विषय से निवृत्ति का विचार (संकल्प) ही वासना या काम का मुख्य आधार है। इन्द्रियों के लिए अनुकूल विषय सुखद और प्रतिकूल विषय दुःखदमाने जाते हैं, अत: सुखद की ओर प्रवृत्ति करना और दुःखद से निवृत्ति चाहना- यही वासना की चालना के दो केन्द्र बन जाते हैं, जिनमें सुखद विषय धनात्मक तथा दु:खद विषय ऋणात्मक चालना-केन्द्र हैं।
जैन-दृष्टिकोण-जैन-दर्शन के अनुसार भी सुख सदैव अनुकूल और दुःख सदैव ही प्रतिकूल होता है। आधुनिक मनोविज्ञान ने यह भी बताया है कि सुख सदैव अनुकूल इसलिए होता है कि उसका जीवन-शक्ति को बनाए रखने की दृष्टि से मूल्य है और दुःख इसलिए प्रतिकूल होता है कि वह जीवन-शक्ति का ह्रास करता है। यही सुख-दुःख का नियम समस्त प्राणीय-व्यवहार का चालक है। जैन-दार्शनिक भी प्राणीय-व्यवहार के चालक के रूप में इसी सुख-दुःख के नियम को स्वीकार करते हैं। अनुकूल के प्रति आकर्षण और प्रतिकूल के प्रति विकर्षण यह इन्द्रिय-स्वभाव है। अनुकूल विषयों की ओर प्रवृत्ति और प्रतिकूल विषयों से निवृत्ति-यह एक नैसर्गिक तथ्य है, क्योंकि सुख अनुकूल और दुःख प्रतिकूल होता है, इसलिए प्राणी सुख प्राप्त करना चाहता है और दुःख से बचना चाहता है। वस्तुतः, वासना ही अपने विधायक-रूप में सुख और निषेधक-रूप में दुःख का रूप ले लेती है। जिससे वासना की पूर्ति हो, वही सुख और जिसमें वासना की पूर्ति न हो, अथवा वासना-पूर्ति में बाधा उत्पन्न हो, वह दुःख।
अनुकूल सुखद विषयों की ओर आकृष्ट होना और उन्हें ग्रहण करना इन्द्रियों की सहज प्रवृत्ति है। मन के अभाव में यह अन्ध इन्द्रिय-प्रवृत्ति होती है, लेकिन जब इन्द्रियों के साथ मन का योग हो जाता है, तो सुखद अनुभूतियों की पुन:-पुन: प्राप्ति का तथा दु:खद अनुभूति से बचने का संकल्प होता है। यही इच्छा या संकल्प का जन्म होता है। जैनाचार्यों ने मन और इन्द्रियों के अनुकूल विषयों की पुन: प्राप्ति की प्रवृत्ति को ही इच्छा कहा है। भविष्य में इन्द्रियों के विषयों की प्राप्ति की अभिलाषा का अतिरेक ही इच्छा है। सुखद अनुभूति को पुन: पुन: प्राप्त करने की लालसाया इच्छा ही तीव्र होकर आसक्ति या राग का रूप ले लेती है। दूसरी ओर, दुःखद अनुभूतियों से बचने की अभिवृत्ति घृणा एवंद्वेष का रूप ले लेती है। भगवान् महावीर ने कहा है कि मनोज्ञ, प्रिय या अनुकूल विषय ही राग का कारण होते हैं और प्रतिकूल या अमनोज्ञ विषय द्वेष का कारण होते हैं। सुखद विषयों से राग और दुःखद विषयों से द्वेष तथा अन्यान्य कषाय और अशुभवृत्तियाँ कैसे प्रतिफलित होकर नैतिक पतन की दिशा में ले जाती हैं, इसे उत्तराध्ययनसूत्र में स्पष्ट किया गया है। इन्द्रियों तथा मन
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org