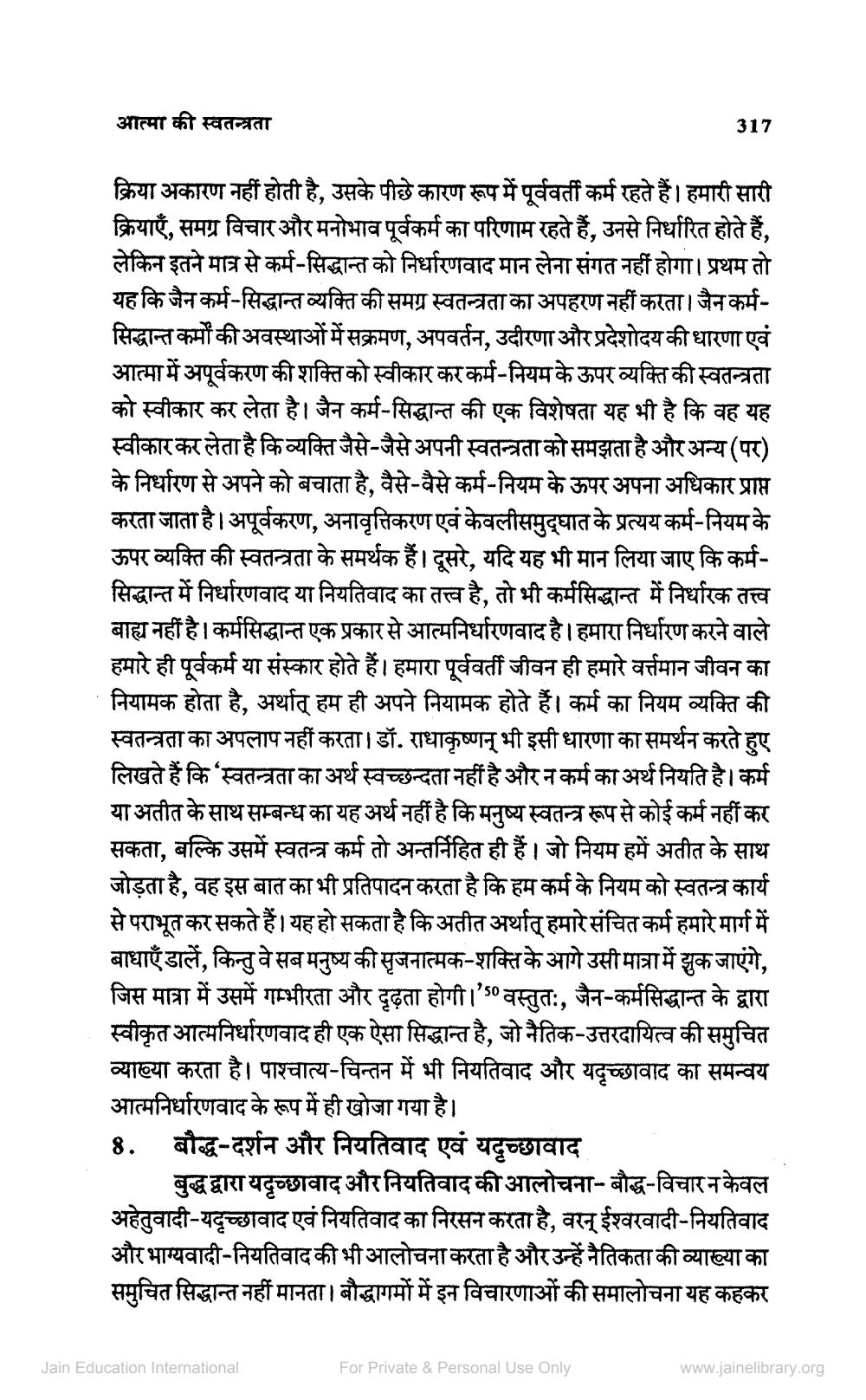________________
आत्मा की स्वतन्त्रता
317
क्रिया अकारण नहीं होती है, उसके पीछे कारण रूप में पूर्ववर्ती कर्म रहते हैं। हमारी सारी क्रियाएँ, समग्र विचार और मनोभाव पूर्वकर्म का परिणाम रहते हैं, उनसे निर्धारित होते हैं, लेकिन इतने मात्र से कर्म-सिद्धान्त को निर्धारणवाद मान लेना संगत नहीं होगा। प्रथम तो यह कि जैन कर्म-सिद्धान्त व्यक्ति की समग्र स्वतन्त्रता का अपहरण नहीं करता। जैन कर्मसिद्धान्त कर्मों कीअवस्थाओं में सक्रमण, अपवर्तन, उदीरणा और प्रदेशोदय की धारणा एवं आत्मा में अपूर्वकरण की शक्ति को स्वीकार कर कर्म-नियम के ऊपर व्यक्ति की स्वतन्त्रता को स्वीकार कर लेता है। जैन कर्म-सिद्धान्त की एक विशेषता यह भी है कि वह यह स्वीकार कर लेता है कि व्यक्ति जैसे-जैसे अपनी स्वतन्त्रता को समझता है और अन्य (पर) के निर्धारण से अपने को बचाता है, वैसे-वैसे कर्म-नियम के ऊपर अपना अधिकार प्राप्त करता जाता है। अपूर्वकरण, अनावृत्तिकरण एवं केवलीसमुद्घात के प्रत्यय कर्म-नियम के ऊपर व्यक्ति की स्वतन्त्रता के समर्थक हैं। दूसरे, यदि यह भी मान लिया जाए कि कर्मसिद्धान्त में निर्धारणवाद या नियतिवाद का तत्त्व है, तो भी कर्मसिद्धान्त में निर्धारक तत्त्व बाह्य नहीं है। कर्मसिद्धान्त एक प्रकार से आत्मनिर्धारणवाद है। हमारा निर्धारण करने वाले हमारे ही पूर्वकर्म या संस्कार होते हैं। हमारा पूर्ववर्ती जीवन ही हमारे वर्तमान जीवन का नियामक होता है, अर्थात् हम ही अपने नियामक होते हैं। कर्म का नियम व्यक्ति की स्वतन्त्रता का अपलाप नहीं करता। डॉ. राधाकृष्णन् भी इसी धारणा का समर्थन करते हुए लिखते हैं कि स्वतन्त्रता का अर्थ स्वच्छन्दता नहीं है और न कर्म का अर्थ नियति है। कर्म या अतीत के साथ सम्बन्ध का यह अर्थ नहीं है कि मनुष्य स्वतन्त्र रूप से कोई कर्म नहीं कर सकता, बल्कि उसमें स्वतन्त्र कर्म तो अन्तर्निहित ही हैं। जो नियम हमें अतीत के साथ जोड़ता है, वह इस बात का भी प्रतिपादन करता है कि हम कर्म के नियम को स्वतन्त्र कार्य से पराभूत कर सकते हैं। यह हो सकता है कि अतीत अर्थात् हमारे संचित कर्म हमारे मार्ग में बाधाएँडालें, किन्तु वे सब मनुष्य की सृजनात्मक-शक्ति के आगे उसी मात्रा में झुक जाएंगे, जिस मात्रा में उसमें गम्भीरता और दृढ़ता होगी। वस्तुत:, जैन-कर्मसिद्धान्त के द्वारा स्वीकृत आत्मनिर्धारणवाद ही एक ऐसा सिद्धान्त है, जो नैतिक-उत्तरदायित्व की समुचित व्याख्या करता है। पाश्चात्य-चिन्तन में भी नियतिवाद और यदृच्छावाद का समन्वय आत्मनिर्धारणवाद के रूप में ही खोजा गया है। 8. बौद्ध-दर्शन और नियतिवाद एवं यदृच्छावाद
बुद्ध द्वारा यदृच्छावाद और नियतिवाद की आलोचना- बौद्ध-विचार न केवल अहेतुवादी-यदृच्छावाद एवं नियतिवाद का निरसन करता है, वरन् ईश्वरवादी-नियतिवाद
और भाग्यवादी-नियतिवाद की भी आलोचना करता है और उन्हें नैतिकता की व्याख्या का समुचित सिद्धान्त नहीं मानता। बौद्धागों में इन विचारणाओं की समालोचना यह कहकर
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org