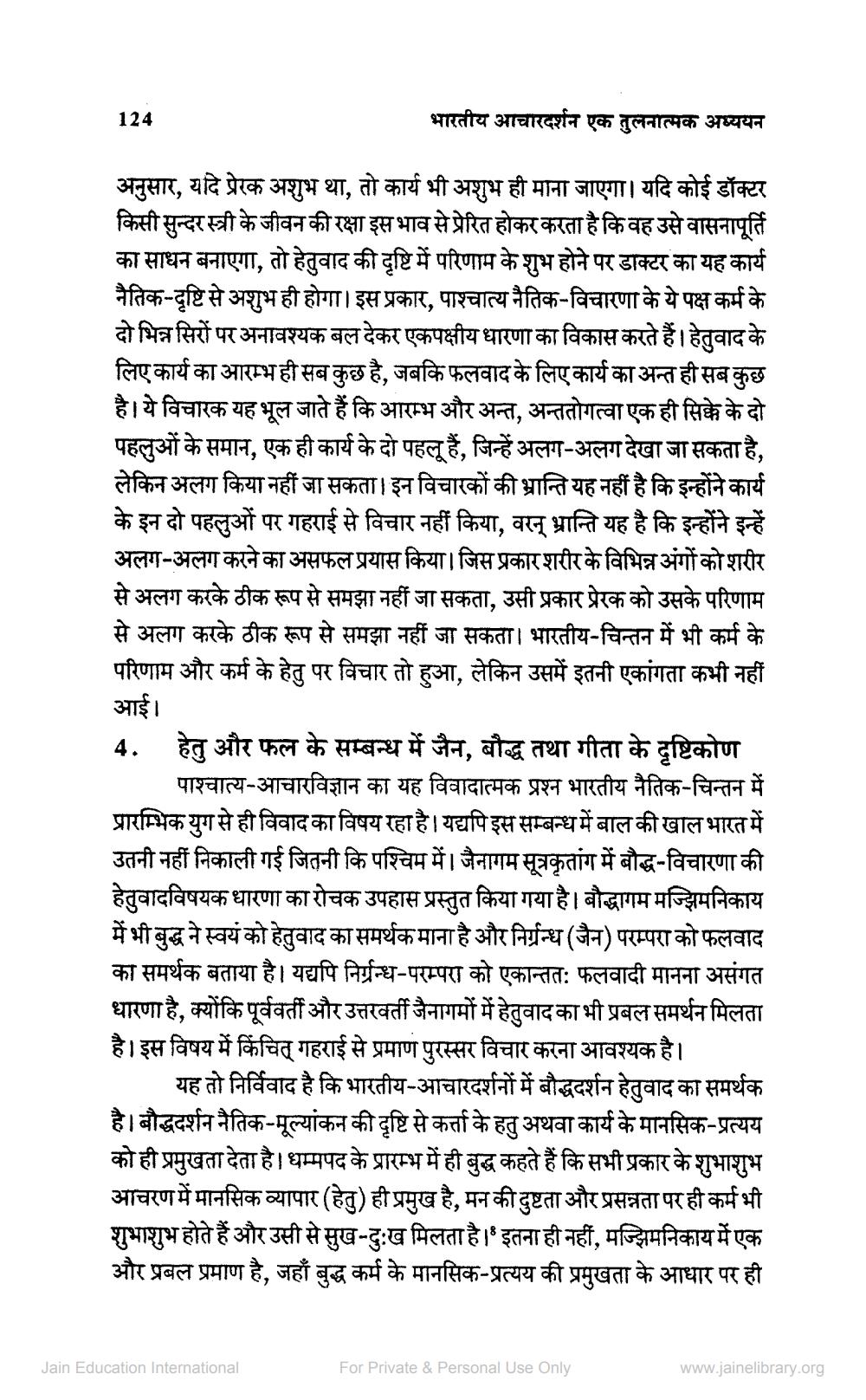________________
124
भारतीय आचारदर्शन एक तुलनात्मक अध्ययन
अनुसार, यदि प्रेरक अशुभ था, तो कार्य भी अशुभ ही माना जाएगा। यदि कोई डॉक्टर किसी सुन्दर स्त्री के जीवन की रक्षा इस भाव से प्रेरित होकर करता है कि वह उसे वासनापूर्ति का साधन बनाएगा, तो हेतुवाद की दृष्टि में परिणाम के शुभ होने पर डाक्टर का यह कार्य नैतिक-दृष्टि से अशुभ ही होगा। इस प्रकार, पाश्चात्य नैतिक-विचारणा के ये पक्ष कर्म के दो भिन्न सिरों पर अनावश्यक बल देकर एकपक्षीय धारणा का विकास करते हैं। हेतुवाद के लिए कार्य का आरम्भही सब कुछ है, जबकि फलवाद के लिए कार्य का अन्त ही सब कुछ है। ये विचारक यह भूल जाते हैं कि आरम्भ और अन्त, अन्ततोगत्वा एक ही सिक्के के दो पहलुओं के समान, एक ही कार्य के दो पहलू हैं, जिन्हें अलग-अलग देखा जा सकता है, लेकिन अलग किया नहीं जा सकता। इन विचारकों की भ्रान्ति यह नहीं है कि इन्होंने कार्य के इन दो पहलुओं पर गहराई से विचार नहीं किया, वरन् भ्रान्ति यह है कि इन्होंने इन्हें अलग-अलग करने का असफल प्रयास किया। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों को शरीर से अलग करके ठीक रूप से समझा नहीं जा सकता, उसी प्रकार प्रेरक को उसके परिणाम से अलग करके ठीक रूप से समझा नहीं जा सकता। भारतीय-चिन्तन में भी कर्म के परिणाम और कर्म के हेतु पर विचार तो हुआ, लेकिन उसमें इतनी एकांगता कभी नहीं आई। 4. हेतु और फल के सम्बन्ध में जैन, बौद्ध तथा गीता के दृष्टिकोण
पाश्चात्य-आचारविज्ञान का यह विवादात्मक प्रश्न भारतीय नैतिक-चिन्तन में प्रारम्भिक युग से ही विवाद का विषय रहा है। यद्यपि इस सम्बन्ध में बाल की खाल भारत में उतनी नहीं निकाली गई जितनी कि पश्चिम में। जैनागम सूत्रकृतांग में बौद्ध-विचारणा की हेतुवादविषयक धारणा का रोचक उपहास प्रस्तुत किया गया है। बौद्धागम मज्झिमनिकाय में भी बुद्ध ने स्वयं को हेतुवाद का समर्थकमाना है और निर्ग्रन्ध (जैन) परम्परा को फलवाद का समर्थक बताया है। यद्यपि निर्गन्ध-परम्परा को एकान्तत: फलवादी मानना असंगत धारणा है, क्योंकि पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती जैनागमों में हेतुवाद का भी प्रबल समर्थन मिलता है। इस विषय में किंचित् गहराई से प्रमाण पुरस्सर विचार करना आवश्यक है।
यह तो निर्विवाद है कि भारतीय-आचारदर्शनों में बौद्धदर्शन हेतुवाद का समर्थक है। बौद्धदर्शन नैतिक-मूल्यांकन की दृष्टि से कर्ता के हतु अथवा कार्य के मानसिक-प्रत्यय को ही प्रमुखता देता है। धम्मपद के प्रारम्भ में ही बुद्ध कहते हैं कि सभी प्रकार के शुभाशुभ आचरण में मानसिक व्यापार (हेतु) ही प्रमुख है, मन की दुष्टता और प्रसन्नता पर ही कर्म भी शुभाशुभ होते हैं और उसी से सुख-दुःख मिलता है। इतना ही नहीं, मज्झिमनिकाय में एक और प्रबल प्रमाण है, जहाँ बुद्ध कर्म के मानसिक-प्रत्यय की प्रमुखता के आधार पर ही
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org