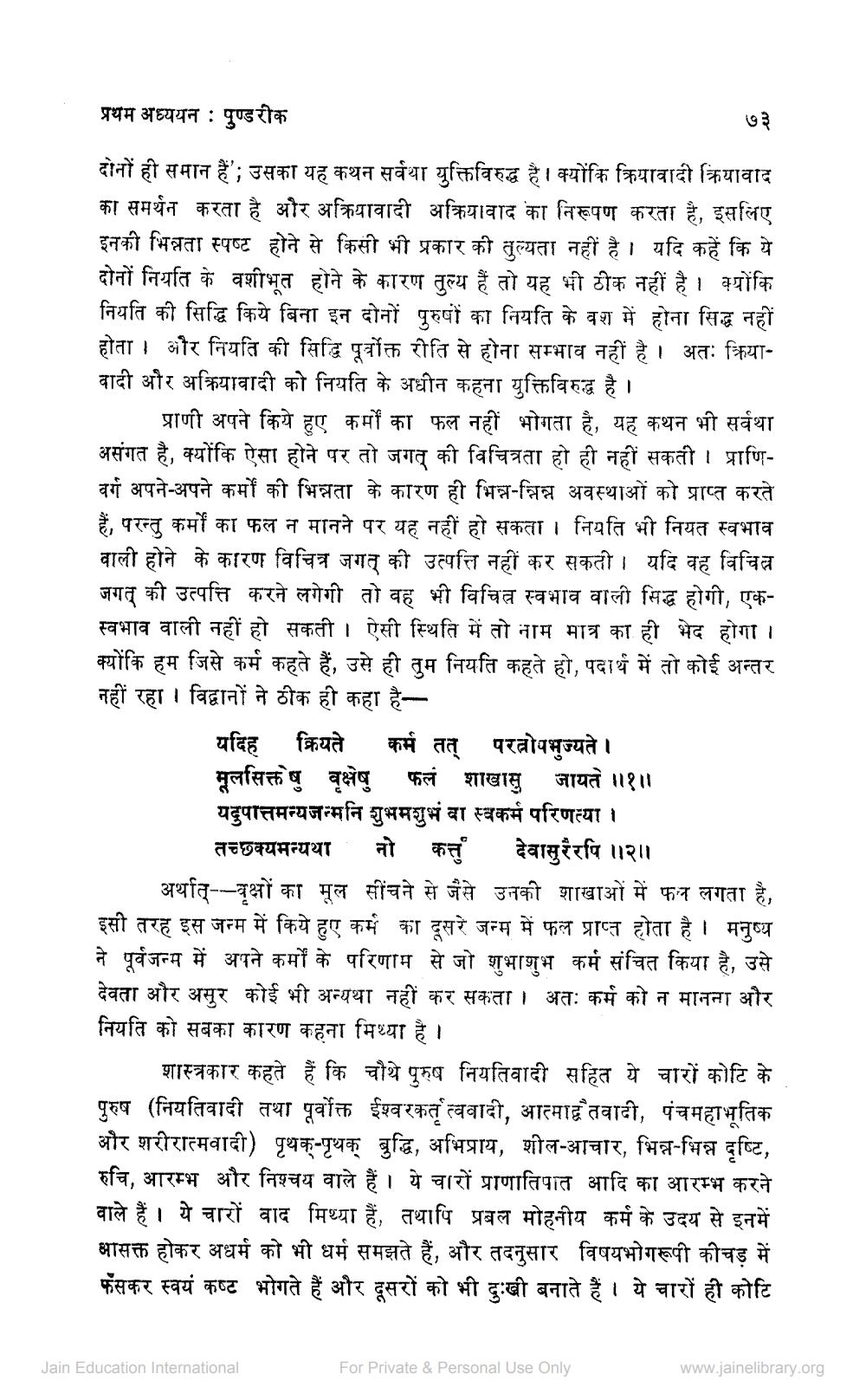________________
प्रथम अध्ययन : पुण्डरीक
७३
दोनों ही समान हैं'; उसका यह कथन सर्वथा युक्तिविरुद्ध है। क्योंकि क्रियावादी क्रियावाद का समर्थन करता है और अक्रियावादी अक्रियावाद का निरूपण करता है, इसलिए इनकी भिन्नता स्पष्ट होने से किसी भी प्रकार की तुल्यता नहीं है। यदि कहें कि ये दोनों नियति के वशीभूत होने के कारण तुल्य हैं तो यह भी ठीक नहीं है। क्योंकि नियति की सिद्धि किये बिना इन दोनों पुरुषों का नियति के वश में होना सिद्ध नहीं होता। और नियति की सिद्धि पूर्वोक्त रीति से होना सम्भाव नहीं है। अतः क्रियावादी और अक्रियावादी को नियति के अधीन कहना युक्तिविरुद्ध है।
प्राणी अपने किये हुए कर्मों का फल नहीं भोगता है, यह कथन भी सर्वथा असंगत है, क्योंकि ऐसा होने पर तो जगत् की विचित्रता हो ही नहीं सकती। प्राणिवर्ग अपने-अपने कर्मों की भिन्नता के कारण ही भिन्न-निन्न अवस्थाओं को प्राप्त करते हैं, परन्तु कर्मों का फल न मानने पर यह नहीं हो सकता। नियति भी नियत स्वभाव वाली होने के कारण विचित्र जगत् की उत्पत्ति नहीं कर सकती। यदि वह विचित्र जगत् की उत्पत्ति करने लगेगी तो वह भी विचित्र स्वभाव वाली सिद्ध होगी, एकस्वभाव वाली नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में तो नाम मात्र का ही भेद होगा। क्योंकि हम जिसे कर्म कहते हैं, उसे ही तुम नियति कहते हो, पदार्थ में तो कोई अन्तर नहीं रहा । विद्वानों ने ठीक ही कहा है
यदिह क्रियते कर्म तत् परनोपभुज्यते। मूलसिक्तषु वृक्षेषु फलं शाखासु जायते ॥१॥ यदुपात्तमन्यजन्मनि शुभमशुभं वा स्वकर्म परिणत्या ।
तच्छक्यमन्यथा नो कर्तुं देवासुरैरपि ॥२॥ अर्थात्---वक्षों का मुल सींचने से जैसे उनकी शाखाओं में फल लगता है, इसी तरह इस जन्म में किये हुए कर्म का दूसरे जन्म में फल प्राप्त होता है। मनुष्य ने पूर्वजन्म में अपने कर्मों के परिणाम से जो शुभाशुभ कर्म संचित किया है, उसे देवता और असुर कोई भी अन्यथा नहीं कर सकता। अतः कर्म को न मानना और नियति को सबका कारण कहना मिथ्या है।
शास्त्रकार कहते हैं कि चौथे पुरुष नियतिवादी सहित ये चारों कोटि के पुरुष (नियतिवादी तथा पूर्वोक्त ईश्वरकर्तृत्ववादी, आत्माद्वैतवादी, पंचमहाभूतिक
और शरीरात्मवादी) पृथक्-पृथक् बुद्धि, अभिप्राय, शील-आचार, भिन्न-भिन्न दृष्टि, रुचि, आरम्भ और निश्चय वाले हैं। ये चारों प्राणातिपात आदि का आरम्भ करने वाले हैं। ये चारों वाद मिथ्या हैं, तथापि प्रबल मोहनीय कर्म के उदय से इनमें आसक्त होकर अधर्म को भी धर्म समझते हैं, और तदनुसार विषयभोगरूपी कीचड़ में फंसकर स्वयं कष्ट भोगते हैं और दूसरों को भी दुःखी बनाते हैं। ये चारों ही कोटि
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org