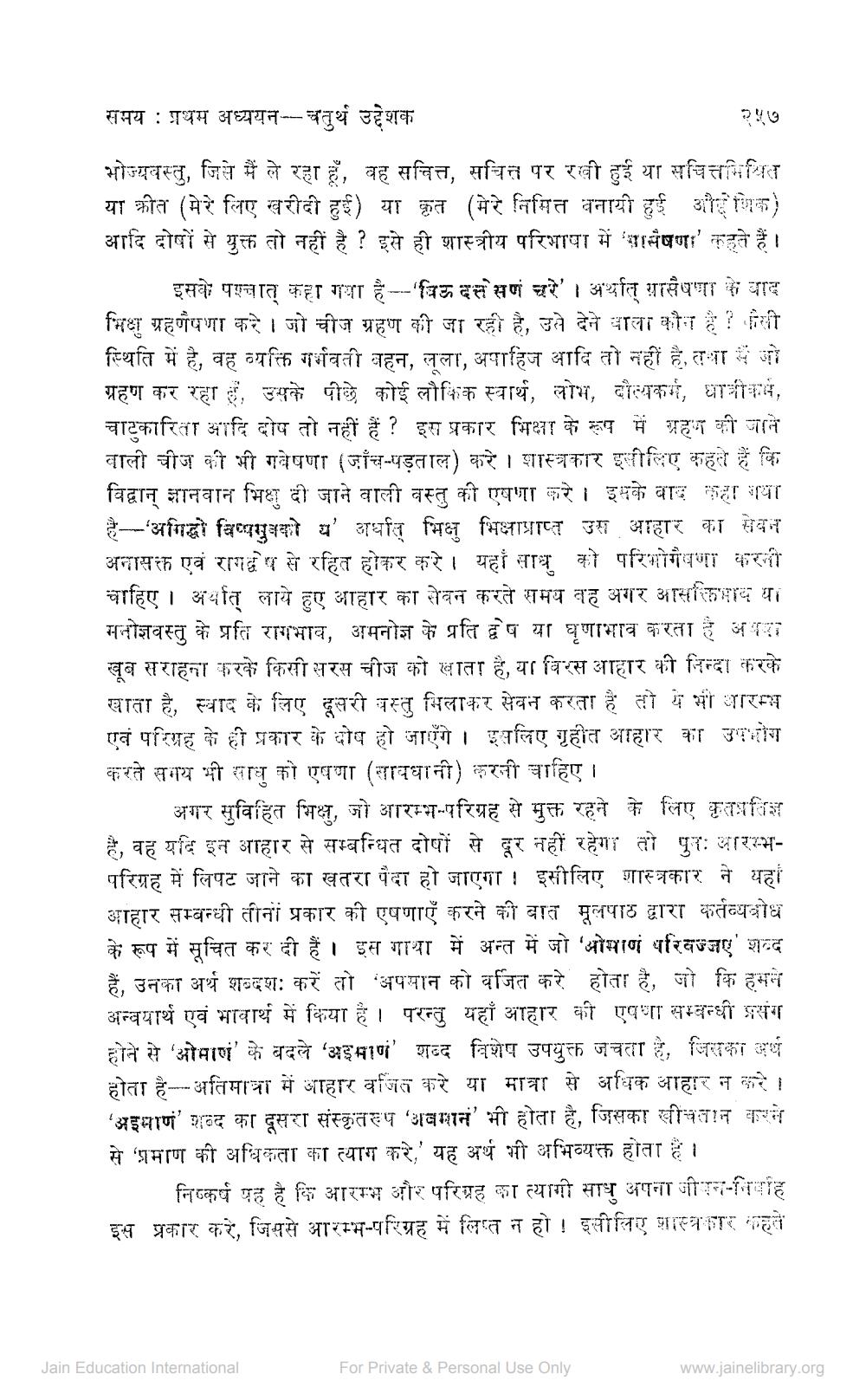________________
समय : प्रथम अध्ययन-- चतुर्थ उद्देशक
२५७
भोज्यवस्तु, जिसे मैं ले रहा हूँ, वह सचित्त, सचित्त पर रखी हुई या सचित्तमिथित या क्रीत (मेरे लिए खरीदी हुई) या कृत (मेरे निमित्त वनायी हुई औदोगिक आदि दोषों से युक्त तो नहीं है ? इसे ही शास्त्रीय परिभाषा में शासैषणा' कहते हैं।
__ इसके पश्चात् कहा गया है.---'विऊ दत्त सणं चरे' । अर्थात् ग्रासैषणा के बाद भिक्षु ग्रहणैषणा करे । जो चीज ग्रहण की जा रही है, उसे देने वाला कौन है ? सी स्थिति में है, वह व्यक्ति गर्भवती बहन, लला, अपाहिज आदि तो नहीं है, तथा मैं जो ग्रहण कर रहा है, उसके पीछे कोई लौकिक स्वार्थ, लोभ, दौत्यकर्म, धात्रीका, चाटुकारिता आदि दोष तो नहीं हैं ? इस प्रकार भिक्षा के रूप में ग्रहण की जाने वाली चीज की भी गवेषणा (जाँच-पड़ताल) करे । शास्त्रकार इसीलिए कहते हैं कि विद्वान् ज्ञानवान भिक्षु दी जाने वाली वस्तु की एषणा करे। इसके बाद कहा गया है-'अगिद्धो विषमुक्को य' अर्थात् भिक्षु भिक्षाप्राप्त उस आहार का सेवन अनासक्त एवं रागद्वेष से रहित होकर करे। यहाँ साधु को परिमोगैषणा करनी चाहिए। अर्थात् लाये हुए आहार का सेवन करते समय वह अगर आसक्तिभाव या मनोज्ञवस्तु के प्रति रागभाव, अमनोज्ञ के प्रति द्वष या घृणाभाव करता है अपर खूब सराहना करके किसी सरस चीज को खाता है, या विरस आहार की निन्दा करके खाता है, स्वाद के लिए दूसरी वस्तु मिलाकर सेवन करता है तो ये भी आरम्भ एवं परिग्रह के ही प्रकार के दोष हो जाएँगे। इसलिए गृहीत आहार का उपयोग करते समय भी साधु को एषणा (सावधानी) करनी चाहिए।
अगर सुविहित भिक्षु, जो आरम्भ-परिग्रह से मुक्त रहने के लिए कृतातिज्ञ है, वह यदि इन आहार से सम्बन्धित दोषों से दूर नहीं रहेगा तो पुरः आरम्भपरिग्रह में लिपट जाने का खतरा पैदा हो जाएगा। इसीलिए शास्त्रकार ने यहां आहार सम्बन्धी तीनों प्रकार की एषणाएँ करने की बात मूलपाठ द्वारा कर्तव्यबोध के रूप में सूचित कर दी हैं। इस गाथा में अन्त में जो 'ओमाणं परिवज्जए' शब्द हैं, उनका अर्थ शब्दश: करें तो 'अपमान को वजित करे होता है, जो कि हमने अन्वयार्थ एवं भावार्थ में किया है। परन्तु यहाँ आहार की एपधा सम्बन्धी प्रसंग होने से 'ओमाणं' के बदले 'अइमाणं' शब्द विशेष उपयुक्त जचता है, जिसका अर्थ होता है--अतिमात्रा में आहार वजित करे या मात्रा से अधिक आहार न करे। 'अइमाणं' शब्द का दूसरा संस्कृतरूप 'अवान' भी होता है, जिसका खीचतान करने से 'प्रमाण की अधिकता का त्याग करे,' यह अर्थ भी अभिव्यक्त होता है।
निष्कर्ष पह है कि आरम्भ और परिग्रह का त्यागी साधु अपना जीवन-निर्वाह इस प्रकार करे, जिससे आरम्भ-परिग्रह में लिप्त न हो ! इसीलिए शास्त्रकार कहते
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org