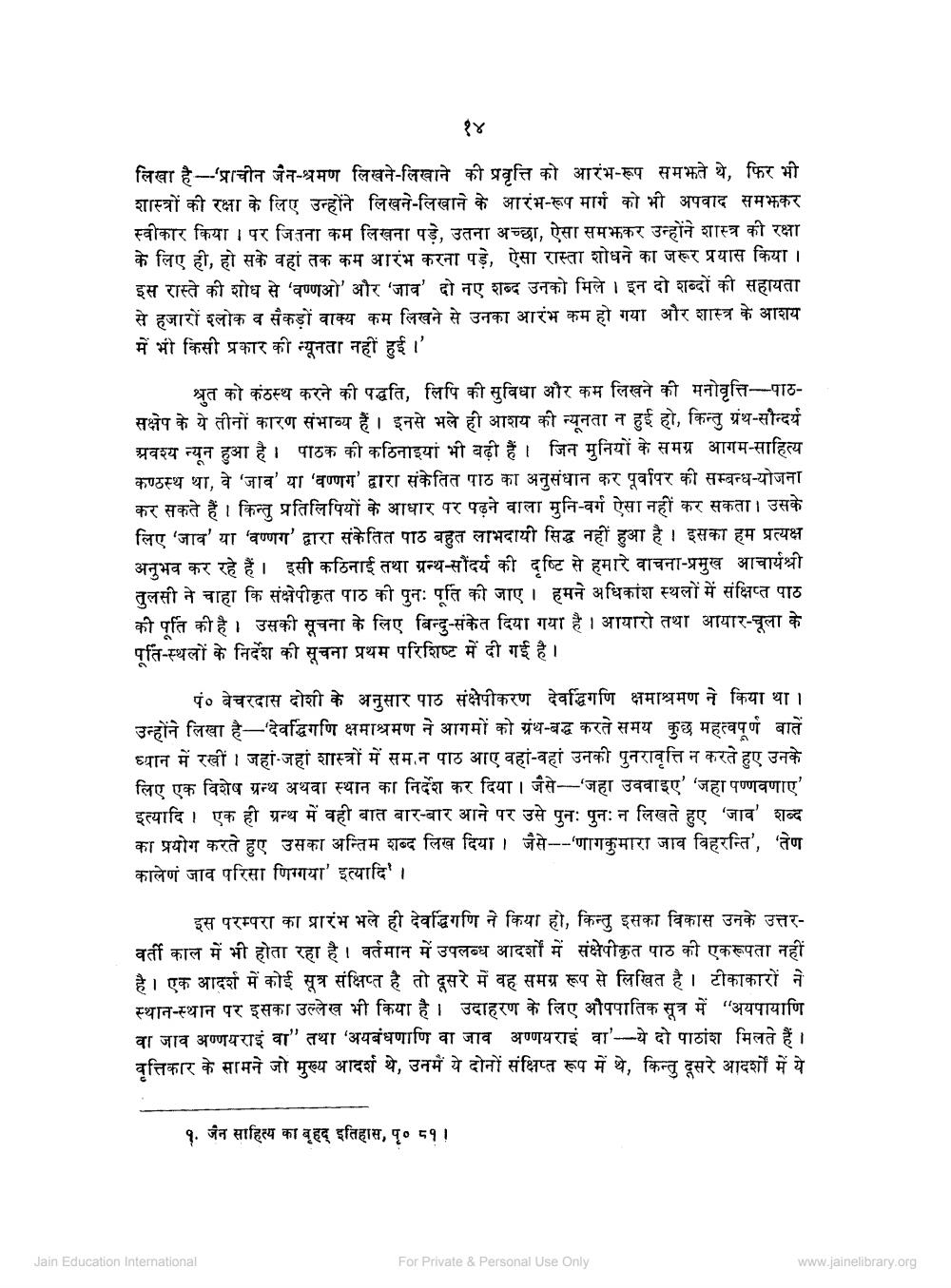________________
लिखा है-'प्राचीन जैन-श्रमण लिखने-लिखाने की प्रवृत्ति को आरंभ-रूप समझते थे, फिर भी शास्त्रों की रक्षा के लिए उन्होंने लिखने-लिखाने के आरंभ-रूप मार्ग को भी अपवाद समझकर स्वीकार किया। पर जितना कम लिखना पड़े, उतना अच्छा, ऐसा समझकर उन्होंने शास्त्र की रक्षा के लिए ही, हो सके वहां तक कम आरंभ करना पड़े, ऐसा रास्ता शोधने का जरूर प्रयास किया। इस रास्ते की शोध से 'वण्णओ' और 'जाव' दो नए शब्द उनको मिले । इन दो शब्दों की सहायता से हजारों श्लोक व सैकड़ों वाक्य कम लिखने से उनका आरंभ कम हो गया और शास्त्र के आशय में भी किसी प्रकार की न्यूनता नहीं हुई।'
श्रुत को कंठस्थ करने की पद्धति, लिपि की सुविधा और कम लिखने की मनोवृत्ति-पाठसक्षेप के ये तीनों कारण संभाव्य हैं। इनसे भले ही आशय की न्यूनता न हुई हो, किन्तु ग्रंथ-सौन्दर्य अवश्य न्यून हुआ है। पाठक की कठिनाइयां भी बढ़ी हैं। जिन मुनियों के समग्र आगम-साहित्य कण्ठस्थ था, वे 'जाव' या 'वण्णग' द्वारा संकेतित पाठ का अनुसंधान कर पूर्वापर की सम्बन्ध-योजना कर सकते हैं। किन्तु प्रतिलिपियों के आधार पर पढ़ने वाला मुनि-वर्ग ऐसा नहीं कर सकता। उसके लिए 'जाव' या 'वण्णग' द्वारा संकेतित पाठ बहुत लाभदायी सिद्ध नहीं हुआ है। इसका हम प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं। इसी कठिनाई तथा ग्रन्थ-सौंदर्य की दृष्टि से हमारे वाचना-प्रमुख आचार्यश्री तुलसी ने चाहा कि संक्षेपीकृत पाठ की पुनः पूर्ति की जाए। हमने अधिकांश स्थलों में संक्षिप्त पाठ की पूर्ति की है। उसकी सूचना के लिए बिन्दु-संकेत दिया गया है । आयारो तथा आयार-चूला के पूर्ति-स्थलों के निर्देश की सूचना प्रथम परिशिष्ट में दी गई है।
पं० बेचरदास दोशी के अनुसार पाठ संक्षेपीकरण देवद्धिगणि क्षमाश्रमण ने किया था। उन्होंने लिखा है-'देवद्धिगणि क्षमाश्रमण ने आगमों को ग्रंथ-बद्ध करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखीं । जहां-जहां शास्त्रों में समान पाठ आए वहां-वहां उनकी पुनरावृत्ति न करते हुए उनके लिए एक विशेष ग्रन्थ अथवा स्थान का निर्देश कर दिया। जैसे-'जहा उववाइए' 'जहा पण्णवणाए' इत्यादि । एक ही ग्रन्थ में वही बात बार-बार आने पर उसे पुनः पुनः न लिखते हुए 'जाव' शब्द का प्रयोग करते हए उसका अन्तिम शब्द लिख दिया। जैसे--'णागकूमारा जाव विहरन्ति', 'तेण कालेणं जाव परिसा णिग्गया' इत्यादि।
इस परम्परा का प्रारंभ भले ही देवद्धिगणि ने किया हो, किन्तु इसका विकास उनके उत्तरवर्ती काल में भी होता रहा है। वर्तमान में उपलब्ध आदर्शों में संक्षेपीकृत पाठ की एकरूपता नहीं है। एक आदर्श में कोई सूत्र संक्षिप्त है तो दूसरे में वह समग्र रूप से लिखित है। टीकाकारों ने स्थान-स्थान पर इसका उल्लेख भी किया है। उदाहरण के लिए औपपातिक सूत्र में "अयपायाणि वा जाव अण्णयराई वा" तथा 'अयबंधणाणि वा जाव अण्णयराइं वा'-ये दो पाठांश मिलते हैं। वत्तिकार के सामने जो मुख्य आदर्श थे, उनमें ये दोनों संक्षिप्त रूप में थे, किन्तु दूसरे आदों में ये
१. जैन साहित्य का बृहद् इतिहास, पृ०८१।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org