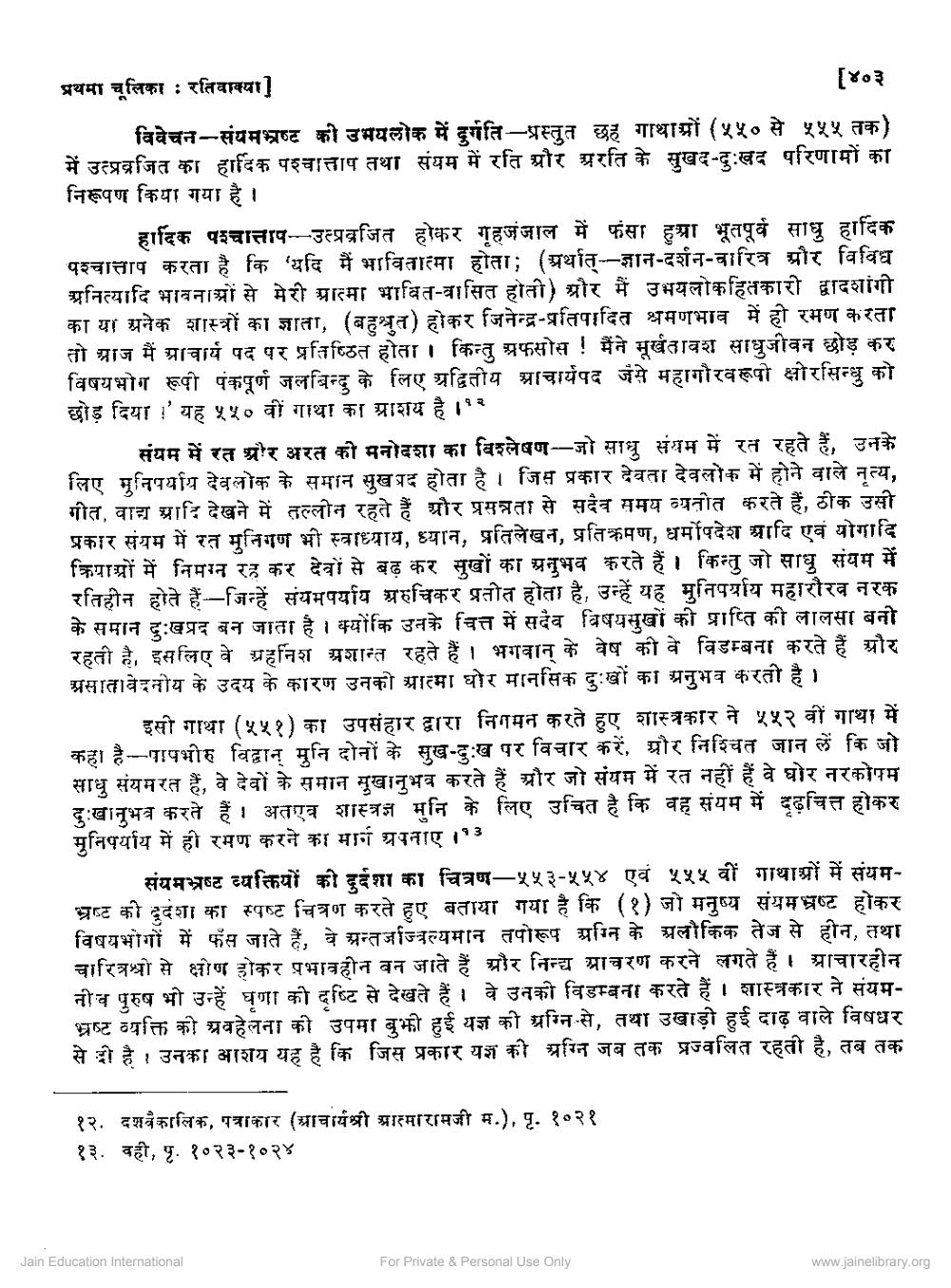________________ प्रथमा चूलिका : रतिवाक्या] [403 विवेचन-संयमभ्रष्ट की उभयलोक में दुर्गति-प्रस्तुत छह गाथानों (550 से 555 तक) में उत्प्रजित का हार्दिक पश्चात्ताप तथा संयम में रति और परति के सुखद-दुःखद परिणामों का निरूपण किया गया है। हादिक पश्चात्ताप-उत्प्रवजित होकर गहजंजाल में फंसा हा भूतपूर्व साधु हार्दिक पश्चात्ताप करता है कि 'यदि मैं भावितात्मा होता; (अर्थात्-ज्ञान-दर्शन-चारित्र और विविध अनित्यादि भावनाओं से मेरी प्रात्मा भावित-वासित होती) और मैं उभयलोकहितकारी द्वादशांगी का या अनेक शास्त्रों का ज्ञाता, (बहुश्रुत) होकर जिनेन्द्र-प्रतिपादित श्रमणभाव में हो रमण करता तो आज मैं प्राचार्य पद पर प्रतिष्ठित होता। किन्तु अफसोस ! मैंने मूर्खतावश साधुजीवन छोड़ कर विषयभोग रूपी पंकपूर्ण जलबिन्दु के लिए अद्वितीय आचार्यपद जैसे महागौरवरूपो क्षीरसिन्धु को छोड़ दिया !' यह 550 वीं गाथा का प्राशय है / 12 __संयम में रत और अरत को मनोदशा का विश्लेषण-जो साधु संयम में रत रहते हैं, उनके लिए मुनिपर्याय देवलोक के समान सुखप्रद होता है। जिस प्रकार देवता देवलोक में होने वाले नृत्य, गीत, वाद्य ग्रादि देखने में तल्लीन रहते हैं और प्रसन्नता से सदैव समय व्यतीत करते हैं, ठीक उसी प्रकार संयम में रत मुनिगण भी स्वाध्याय, ध्यान, प्रतिलेखन, प्रतिक्रमण, धर्मोपदेश आदि एवं योगादि क्रियाओं में निमग्न रह कर देवों से बढ़ कर सुखों का अनुभव करते हैं। किन्तु जो साधु संयम में रतिहीन होते हैं जिन्हें संयमपर्याय अरुचिकर प्रतीत होता है, उन्हें यह मुनिपर्याय महारौरव नरक के समान दुःखप्रद बन जाता है। क्योंकि उनके चित्त में सदैव विषयसुखों की प्राप्ति की लालसा बनी रहती है, इसलिए वे अहनिश अशान्त रहते हैं। भगवान् के वेष की वे विडम्बना करते हैं और असातावेदनोय के उदय के कारण उनको आत्मा घोर मानसिक दुःखों का अनुभव करती है। इसी गाथा (551) का उपसंहार द्वारा निगमन करते हए शास्त्रकार ने 552 वी गाथा में कहा है-पापभीरु विद्वान् मुनि दोनों के सुख-दु:ख पर विचार करें, और निश्चित जान लें कि जो साधु संयमरत हैं, वे देवों के समान सुखानुभव करते हैं और जो संयम में रत नहीं हैं वे घोर नरकोपम दुःखानुभव करते हैं। अतएव शास्त्रज्ञ मुनि के लिए उचित है कि वह संयम में दृढ़चित्त होकर मुनिपर्याय में ही रमण करने का मार्ग अपनाए / ' संयमभ्रष्ट व्यक्तियों को दुर्दशा का चित्रण-५५३-५५४ एवं 555 वीं गाथाओं में संयमभ्रष्ट की दुर्दशा का स्पष्ट चित्रण करते हुए बताया गया है कि (1) जो मनुष्य संयमभ्रष्ट होकर विषयभोगों में फंस जाते हैं, वे अन्तर्जाज्वल्यमान तपोरूप अग्नि के अलौकिक तेज से हीन, तथा चारित्रश्री से क्षीण होकर प्रभावहीन बन जाते हैं और निन्द्य पाचरण करने लगते हैं। प्राचारहीन नी व पुरुष भी उन्हें घणा की दष्टि से देखते हैं। वे उनको विडम्बना करते हैं। शास्त्रकार ने संयमभ्रष्ट व्यक्ति को अवहेलना की उपमा बुझी हुई यज्ञ की अग्नि से, तथा उखाड़ी हुई दाढ़ वाले विषधर से दी है / उनका आशय यह है कि जिस प्रकार यज्ञ की अग्नि जब तक प्रज्वलित रहती है, तब तक 12. दशवकालिक, पत्राकार (ग्राचार्यश्री आत्मारामजी म.), पृ. 1021 13. वही, पृ. 1023-1024 Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org