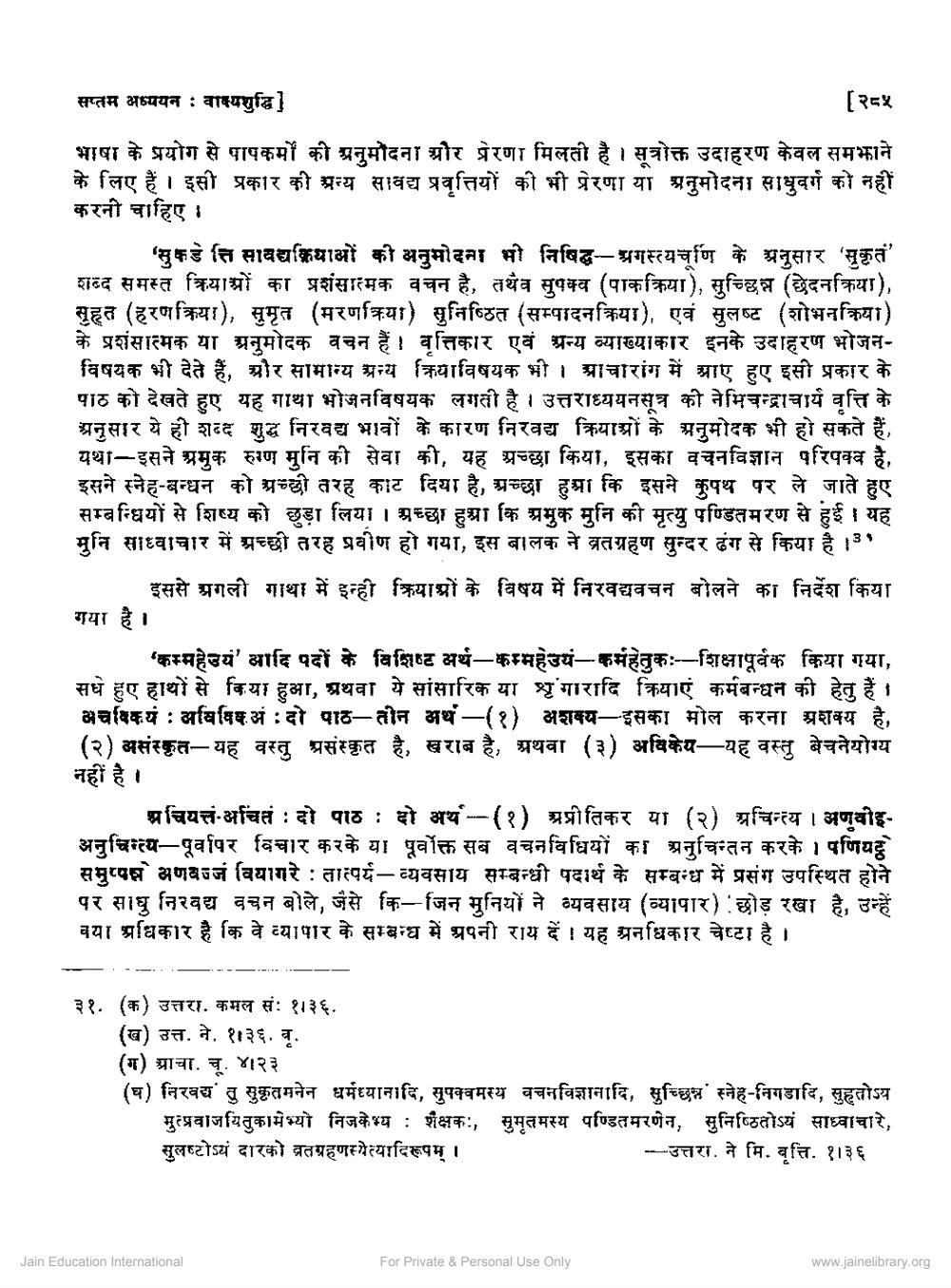________________ सप्तम अध्ययन : वाक्यशुद्धि] [285 भाषा के प्रयोग से पापकर्मों की अनुमोदना और प्रेरणा मिलती है। सूत्रोक्त उदाहरण केवल समझाने के लिए हैं। इसी प्रकार की अन्य सावद्य प्रवृत्तियों को भी प्रेरणा या अनुमोदना साधुवर्ग को नहीं करनी चाहिए। 'सुकडे ति सावधक्रियाओं की अनुमोदना भी निषिद्ध-अगस्त्यचूणि के अनुसार 'सुकृतं' शब्द समस्त क्रियाओं का प्रशंसात्मक वचन है, तथैव सुपक्व (पाकक्रिया), सुच्छिन्न (छेदनक्रिया), सुहृत (हरण क्रिया), सुमृत (मरणक्रिया) सुनिष्ठित (सम्पादनक्रिया), एवं सुलष्ट (शोभनक्रिया) के प्रशंसात्मक या अनुमोदक वचन हैं। वृत्तिकार एवं अन्य व्याख्याकार इनके उदाहरण भोजनविषयक भी देते हैं, और सामान्य अन्य क्रियाविषयक भी। प्राचारांग में आए हुए इसी प्रकार के पाठ को देखते हुए यह गाथा भोजनविषयक लगती है। उत्तराध्ययनसूत्र की नेमिचन्द्राचार्य वृत्ति के अनुसार ये ही शब्द शुद्ध निरवद्य भावों के कारण निरवद्य क्रियाओं के अनुमोदक भी हो सकते हैं, यथा-इसने अमुक रुग्ण मुनि की सेवा की, यह अच्छा किया, इसका वचनविज्ञान परिपक्व है, इसने स्नेह-बन्धन को अच्छी तरह काट दिया है, अच्छा हुआ कि इसने कुपथ पर ले जाते हुए सम्बन्धियों से शिष्य को छुड़ा लिया / अच्छा हुआ कि अमुक मुनि की मृत्यु पण्डितमरण से हुई। यह मुनि साध्वाचार में अच्छी तरह प्रवीण हो गया, इस बालक ने व्रतग्रहण सुन्दर ढंग से किया है।" इससे अगली गाथा में इन्ही क्रियाओं के विषय में निरवद्यवचन बोलने का निर्देश किया गया है। 'कम्महेउयं' आदि पदों के विशिष्ट अर्थ-कम्महउयं-कर्महेतुकः-शिक्षापूर्वक किया गया, सधे हुए हाथों से किया हुआ, अथवा ये सांसारिक या शृंगारादि क्रियाएं कर्मबन्धन की हेतु हैं। अचक्कियं : अविविध अंदो पाठ-तीन अर्थ-(१) अशक्य-इसका मोल करना अशक्य है, (2) असंस्कृत- यह वस्तु असंस्कृत है, खराब है, अथवा (3) अविकेय—यह वस्तु बेचनेयोग्य नहीं है। प्रचियत्त अचितं : दो पाठ : दो अर्थ-(१) अप्रीतिकर या (2) अचिन्त्य / अणुवीइअनुचित्य-पूर्वापर विचार करके या पूर्वोक्त सब वचन विधियों का अनुचिन्तन करके / पणिय? समुप्पन अणवज्ज वियागरे : तात्पर्य-व्यवसाय सम्बन्धी पदार्थ के सम्बन्ध में प्रसंग उपस्थित होने पर साधु निरवद्य वचन बोले, जैसे कि-जिन मुनियों ने व्यवसाय (व्यापार) छोड़ रखा है, उन्हें क्या अधिकार है कि वे व्यापार के सम्बन्ध में अपनी राय दें। यह अनधिकार चेष्टा है। 31. (क) उत्तरा. कमल संः 1136. (ख) उत्त. ने. 1136. बृ. (ग) प्राचा. च. 4 // 23 (घ) निरवद्यतु सुकृतमनेन धर्मध्यानादि, सुपक्वमस्य वचनविज्ञानादि, सुच्छिन्न स्नेह-निगडादि, सुहृतोऽय मुत्प्रवाजयितुकामेभ्यो निजके भ्य : शैक्षकः, सुमृतमस्य पण्डितमरणेन, सुनिष्ठितोऽयं साध्वाचारे, सुलष्टोऽयं दारको व्रतग्रहणस्येत्यादिरूपम् / --- उत्तरा. ने मि. बृत्ति. 1 / 36 Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org