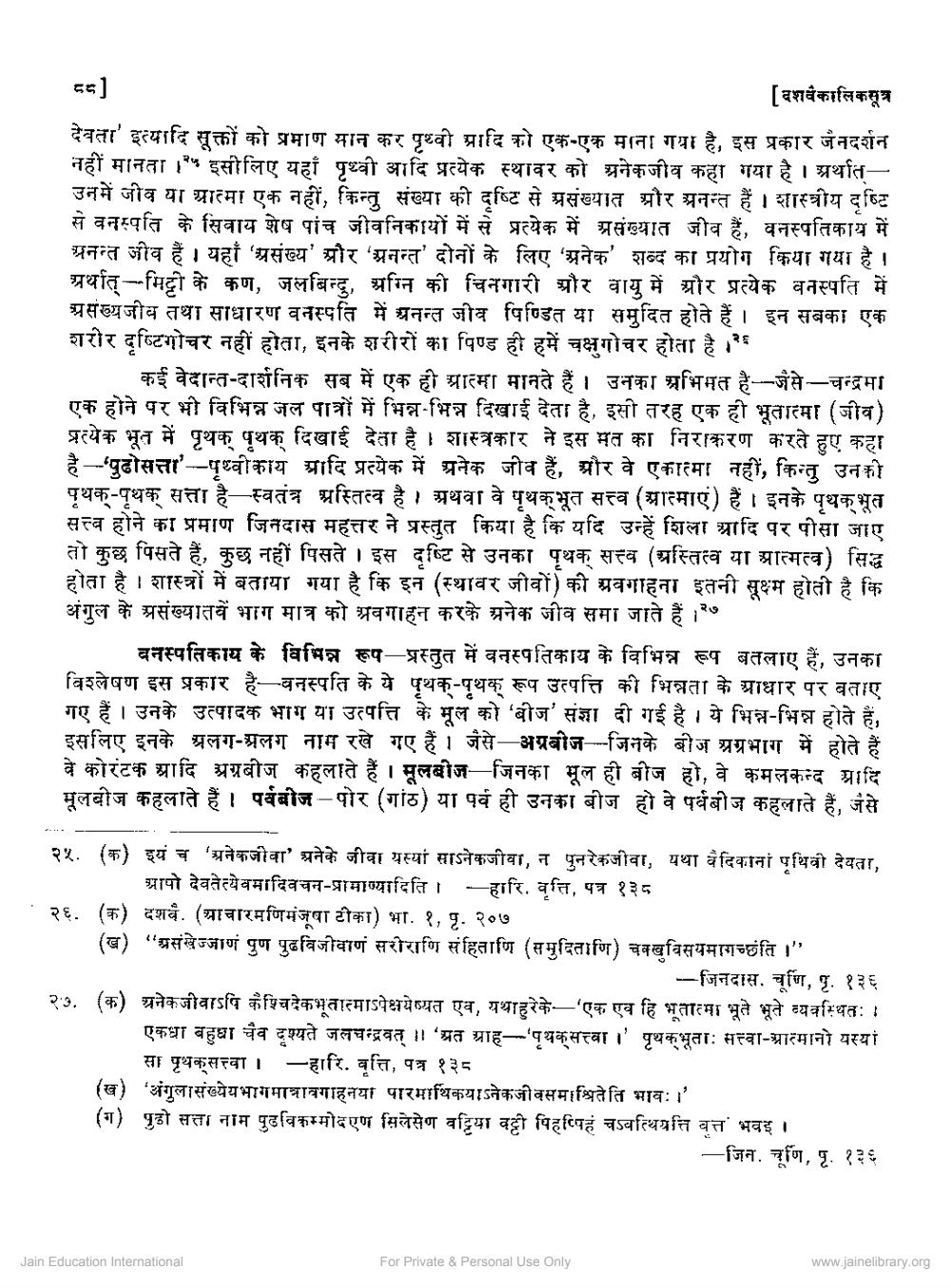________________ 88] [वशवकालिकसूत्र देवता' इत्यादि सूक्तों को प्रमाण मान कर पृथ्वी प्रादि को एक-एक माना गया है, इस प्रकार जैनदर्शन नहीं मानता / इसीलिए यहाँ पृथ्वी आदि प्रत्येक स्थावर को अनेकजीव कहा गया है / अर्थातउनमें जीव या प्रात्मा एक नहीं, किन्तु संख्या की दृष्टि से असंख्यात और अनन्त हैं / शास्त्रीय दृष्टि से वनस्पति के सिवाय शेष पांच जीवनिकायों में से प्रत्येक में असंख्यात जीव हैं, वनस्पतिकाय में अनन्त जीव हैं / यहाँ 'असंख्य' और 'अनन्त' दोनों के लिए 'अनेक' शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्थात्-मिट्टी के कण, जलबिन्दु, अग्नि की चिनगारी और वायु में और प्रत्येक वनस्पति में असंख्य जीव तथा साधारण वनस्पति में अनन्त जीव पिण्डित या समुदित होते हैं। इन सबका एक शरीर दृष्टिगोचर नहीं होता, इनके शरीरों का पिण्ड ही हमें चक्षुगोचर होता है / 26 कई वेदान्त-दार्शनिक सब में एक ही प्रात्मा मानते हैं। उनका अभिमत है-जैसे-चन्द्रमा एक होने पर भी विभिन्न जल पात्रों में भिन्न-भिन्न दिखाई देता है, इसी तरह एक ही भूतात्मा (जीव) प्रत्येक भूत में पृथक् पृथक् दिखाई देता है। शास्त्रकार ने इस मत का निराकरण करते हुए कहा है-'पुढोसत्ता'--पृथ्वीकाय आदि प्रत्येक में अनेक जीव हैं, और वे एकात्मा नहीं, किन्तु उनकी पृथक-पृथक् सत्ता है स्वतंत्र अस्तित्व है। अथवा वे पृथक्भूत सत्त्व (आत्माएं) हैं। इनके पृथक भूत सत्त्व होने का प्रमाण जिनदास महत्तर ने प्रस्तुत किया है कि यदि उन्हें शिला आदि पर पीसा जाए तो कुछ पिसते हैं, कुछ नहीं पिसते / इस दृष्टि से उनका पृथक् सत्त्व (अस्तित्व या आत्मत्व) सिद्ध होता है / शास्त्रों में बताया गया है कि इन (स्थावर जीवों) की अवगाहना इतनी सूक्ष्म होती है कि अंगुल के असंख्यातवें भाग मात्र को अवगाहन करके अनेक जीव समा जाते हैं / 27 बनस्पतिकाय के विभिन्न रूप—प्रस्तुत में वनस्पतिकाय के विभिन्न रूप बतलाए हैं, उनका विश्लेषण इस प्रकार है-वनस्पति के ये पृथक्-पृथक् रूप उत्पत्ति की भिन्नता के आधार पर बताए गए हैं। उनके उत्पादक भाग या उत्पत्ति के मूल को 'बीज' संज्ञा दी गई है / ये भिन्न-भिन्न होते हैं, इसलिए इनके अलग-अलग नाम रखे गए हैं। जैसे—अग्रबीज-जिनके बीज अग्रभाग में होते हैं वे कोरंटक आदि अग्रबीज कहलाते हैं / मूलबीज-जिनका मूल ही बीज हो, वे कमलकन्द प्रादि मूलबीज कहलाते हैं। पर्वबीज-पोर (गांठ) या पर्व ही उनका बीज हो वे पर्वबीज कहलाते हैं, जैसे 25. (क) इयं च 'अनेकजीवा' अनेके जीवा यस्यां साऽनेकजीवा, न पुनरेकजीवा, यथा वैदिकानां पथिवी देवता, पापो देवतेत्येवमादिवचन-प्रामाण्यादिति। --हारि, वत्ति, पत्र 138 26. (क) दशव. (याचारमणिमंजूषा टीका) भा. 1, पृ. 207 (ख) "असंखेज्जाणं पुण पुढविजीवाणं सरीराणि संहिताणि (समुदिताणि) चक्खुविसयमागच्छंति / " -जिनदास. चूर्णि, पृ. 136 27. (क) अनेकजीवाऽपि कैश्चिदेकभूतात्माऽपेक्षयेष्यत एव, यथाहुरेके— 'एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः / एकध्रा बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत् / / 'प्रत पाह-'पृथक्सत्त्वा।' पृथक्भूताः सत्त्वा-प्रात्मानो यस्यां सा पृथक्सत्त्वा। -हारि. वृत्ति, पत्र 138 (ख) 'अंगुलासंख्येयभागमात्रावगाहनया पारमार्थिकयाऽनेकजीवसमाश्रितेति भावः।' (ग) पुढो सत्ता नाम पुढ विकम्मोदएण सिलेसेण वट्टिया वट्टी पिहप्पिह चऽबत्थियत्ति बत्त भवई / —जिन. चूणि, पृ. 136 Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org