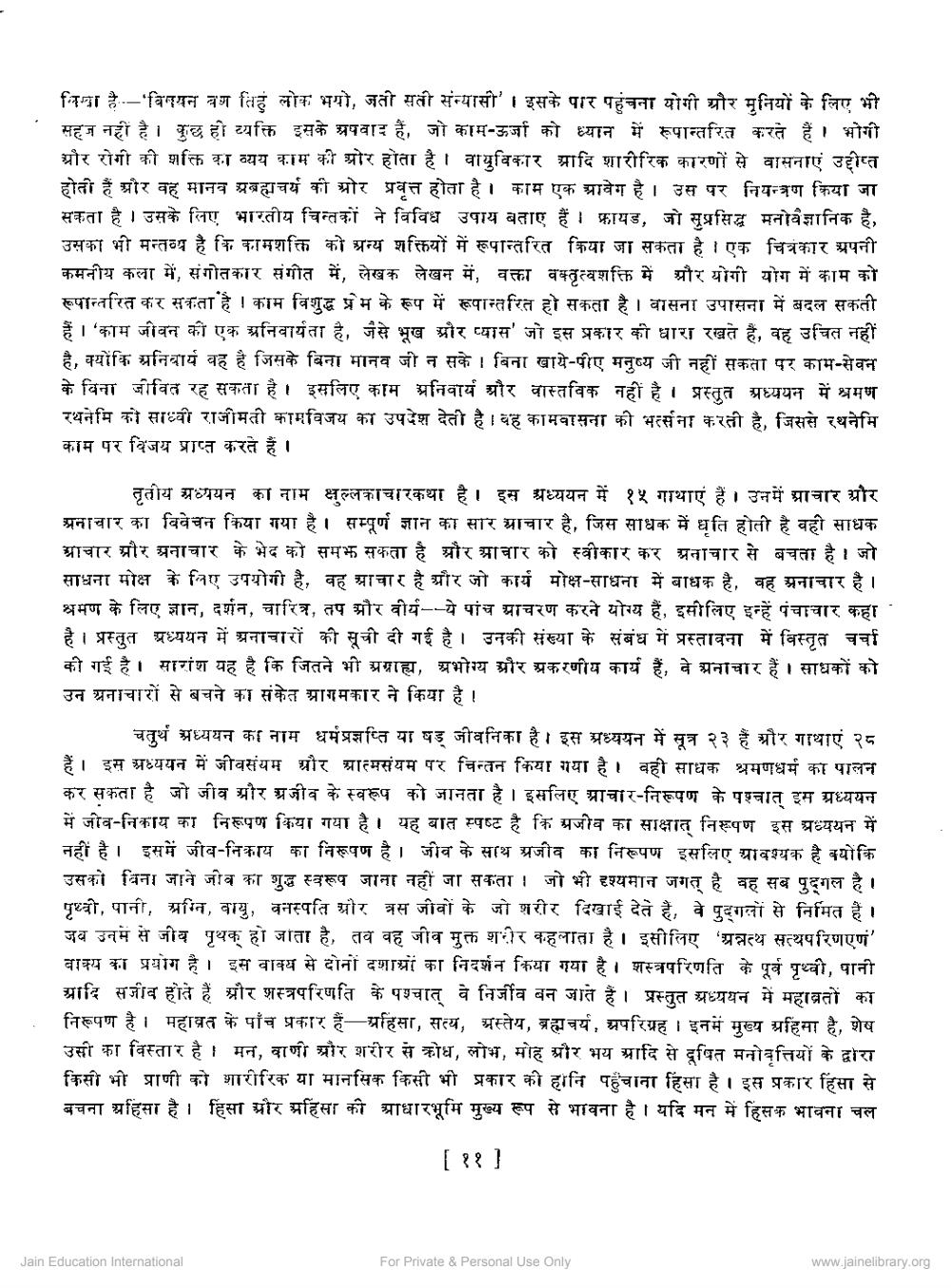________________ लिखा है...-'विपयन बग तिहं लोक भयो, जती सती संन्यासी' / इसके पार पहंचना योगी और मुनियों के लिए भी सहज नहीं है। कुछ ही व्यक्ति इसके अपवाद हैं, जो काम-ऊर्जा को ध्यान में रूपान्तरित करते हैं। भोगी और रोगी की शक्ति का व्यय काम की ओर होता है। वायुविकार आदि शारीरिक कारणों से वासनाएं उद्दीप्त होती हैं और वह मानव अब्रह्मचर्य की ओर प्रवृत्त होता है। काम एक आवेग है। उस पर नियन्त्रण किया जा सकता है। उसके लिए भारतीय चिन्तकों ने विविध उपाय बताए हैं। फ्रायड, जो सूप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है, उसका भी मन्तव्य है कि कामशक्ति को अन्य शक्तियों में रूपान्तरित किया जा सकता है। एक चित्रकार अपनी कमनीय कला में, संगीतकार संगीत में, लेखक लेखन में, वक्ता वक्तृत्वशक्ति में और योगी योग में काम को रूपान्तरित कर सकता है / काम विशुद्ध प्रेम के रूप में रूपान्तरित हो सकता है। वासना उपासना में बदल सकती हैं / 'काम जीवन की एक अनिवार्यता है, जैसे भूख और प्यास' जो इस प्रकार की धारा रखते हैं, वह उचित नहीं है, क्योंकि अनिवार्य वह है जिसके बिना मानव जी न सके / बिना खाये-पीए मनुष्य जी नहीं सकता पर काम-सेवन के बिना जीवित रह सकता है। इसलिए काम अनिवार्य और वास्तविक नहीं है। प्रस्तुत अध्ययन में श्रमण रथनेमि को साध्वी राजीमती कामविजय का उपदेश देती है। वह कामवासना की भर्त्सना करती है, जिससे रथनेमि काम पर विजय प्राप्त करते हैं / तृतीय अध्ययन का नाम क्षुल्लकाचारकथा है। इस अध्ययन में 15 गाथाएं हैं। उनमें प्राचार और अनाचार का विवेचन किया गया है। सम्पूर्ण ज्ञान का सार प्राचार है, जिस साधक में धति होती है वही साधक प्राचार और अनाचार के भेद को समझ सकता है और आवार को स्वीकार कर अनाचार से बचता है। जो साधना मोक्ष के लिए उपयोगी है, वह आचार है और जो कार्य मोक्ष-साधना में बाधक है, वह अनाचार है / श्रमण के लिए ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर्य- ये पांच आचरण करने योग्य हैं, इसीलिए इन्हें पंचाचार कहा है। प्रस्तूत अध्ययन में अनाचारों की सूची दी गई है। उनकी संख्या के संबंध में प्रस्तावना में विस्तृत चर्चा की गई है। सारांश यह है कि जितने भी अग्राह्य, अभोग्य और अकरणीय कार्य हैं, वे अनाचार हैं। साधकों को उन अनाचारों से बचने का संकेत आगमकार ने किया है। चतुर्थ अध्ययन का नाम धर्मप्रज्ञप्ति या बड़ जीवनिका है। इस अध्ययन में सूत्र 23 हैं और गाथाएं 28 हैं। इस अध्ययन में जीवसंयम और आत्मसंयम पर चिन्तन किया गया है। वही साधक श्रमणधर्म का पालन कर सकता है जो जीव और अजीव के स्वरूप को जानता है। इसलिए प्राचार-निरूपण के पश्चात इस अध्ययन में जीव-निकाय का निरूपण किया गया है। यह बात स्पष्ट है कि अजीव का साक्षात निरूपण इस अध्ययन में नहीं है। इसमें जीव-निकाय का निरूपण है। जीव के साथ अजीव का निरूपण इसलिए आवश्यक है क्योंकि उसको बिना जाने जीव का शुद्ध स्वरूप जाना नहीं जा सकता। जो भी दृश्यमान जगत् है वह सब पुदगल है। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस जीवों के जो शरीर दिखाई देते हैं, वे पुदगलों से निर्मित हैं। जब उनमें से जीव पृथक हो जाता है, तव वह जीव मुक्त शबीर कहलाता है। इसीलिए 'अन्नत्थ सत्थपरिणएणं' बाक्य का प्रयोग है। इस वाक्य से दोनों दशाओं का निदर्शन किया गया है। शस्त्रपरिणति के पूर्व पृथ्वी, पानी आदि सजीव होते हैं और शस्त्रपरिणति के पश्चात् वे निर्जीव बन जाते हैं। प्रस्तुत अध्ययन में महाव्रतों का निरूपण है। महावत के पाँच प्रकार हैं-अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह / इनमें मुख्य अहिमा है, शेष उसी का विस्तार है। मन, वाणी और शरीर से क्रोध, लोभ, मोह और भय आदि से दुषित मनोवृत्तियों के द्वारा किसी भी प्राणी को शारीरिक या मानसिक किसी भी प्रकार की हानि पहुँचाना हिंसा है। इस प्रकार हिंसा से बचना अहिंसा है। हिंसा और अहिंसा की आधारभूमि मुख्य रूप से भावना है / यदि मन में हिंसक भावना चल [11] Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org