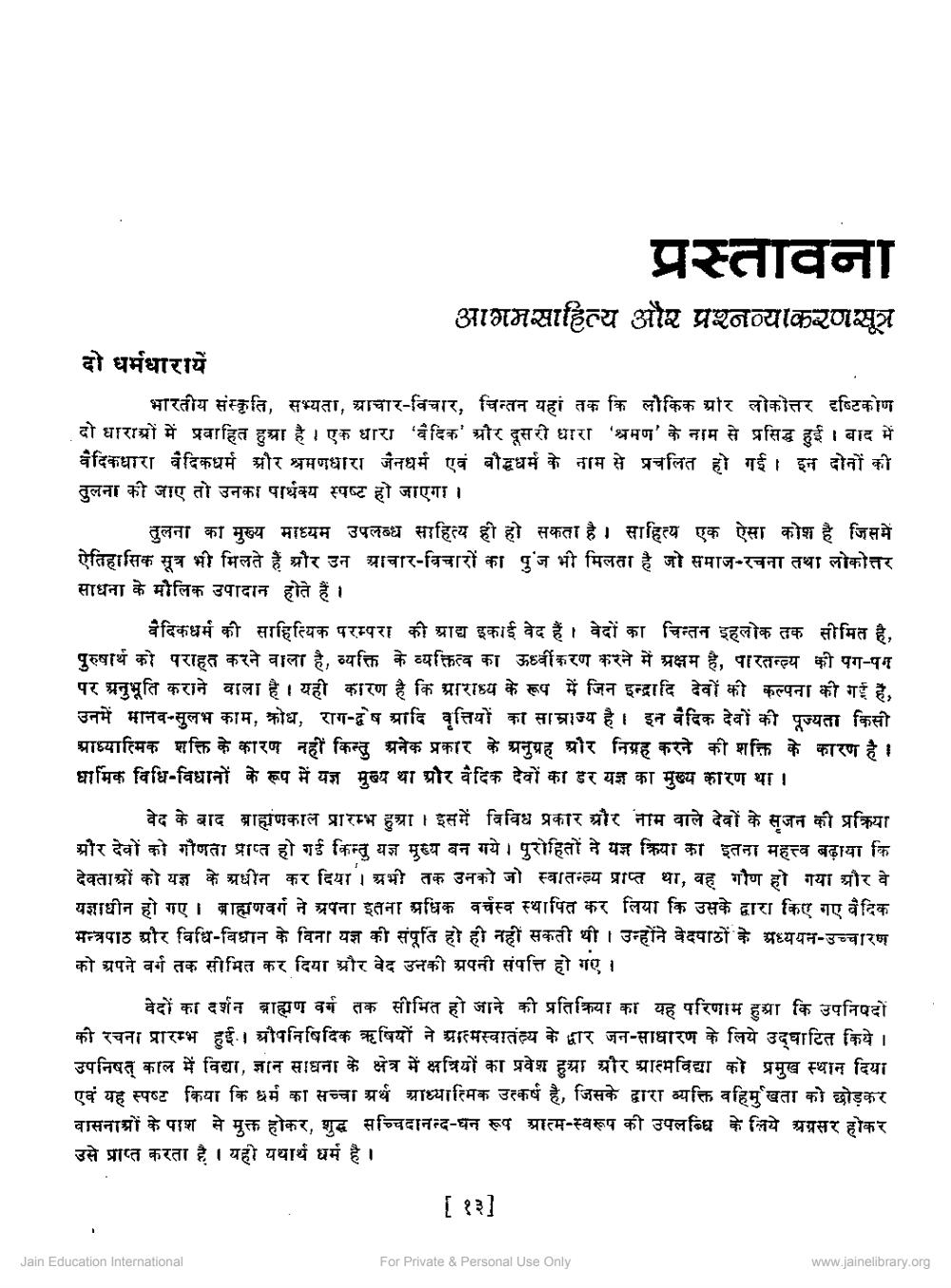________________ प्रस्तावना आगम साहित्य और प्रश्नव्याकरणसूत्र दो धर्मधारायें भारतीय संस्कृति, सभ्यता, आचार-विचार, चिन्तन यहां तक कि लौकिक और लोकोत्तर दृष्टिकोण दो धारामों में प्रवाहित हुया है। एक धारा 'वैदिक' और दूसरी धारा 'श्रमण' के नाम से प्रसिद्ध हुई। बाद में वैदिकधारा वैदिकधर्म और श्रमणधारा जैनधर्म एवं बौद्धधर्म के नाम से प्रचलित हो गई। इन दोनों की तुलना की जाए तो उनका पार्थक्य स्पष्ट हो जाएगा। तुलना का मुख्य माध्यम उपलब्ध साहित्य ही हो सकता है। साहित्य एक ऐसा कोश है जिसमें ऐतिहासिक सूत्र भी मिलते हैं और उन प्राचार-विचारों का पुज भी मिलता है जो समाज-रचना तथा लोकोत्तर साधना के मौलिक उपादान होते हैं। वैदिकधर्म की साहित्यिक परम्परा की प्राद्य इकाई वेद हैं / वेदों का चिन्तन इहलोक तक सीमित है, पुरुषार्थ को पराहत करने वाला है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का ऊध्वीकरण करने में अक्षम है, पारतन्त्र्य की पग-पग पर अनुभूति कराने वाला है। यही कारण है कि प्राराध्य के रूप में जिन इन्द्रादि देवों की कल्पना की गई है, उनमें मानव-सुलभ काम, क्रोध, राग-द्वेष आदि वृत्तियों का साम्राज्य है। इन वैदिक देवों की पूज्यता किसी प्राध्यात्मिक शक्ति के कारण नहीं किन्तु अनेक प्रकार के अनुग्रह और निग्रह करने की शक्ति के कारण है। धार्मिक विधि-विधानों के रूप में यज्ञ मूख्य था और वैदिक देवों का डर यज्ञ का मुख्य कारण था। वेद के बाद ब्राह्मणकाल प्रारम्भ हुआ। इसमें विविध प्रकार और नाम वाले देवों के सृजन की प्रक्रिया और देवों को गौणता प्राप्त हो गई किन्तु यज्ञ मुख्य बन गये। पुरोहितों ने यज्ञ क्रिया का इतना महत्त्व बढ़ाया कि देवताओं को यज्ञ के अधीन कर दिया / अभी तक उनको जो स्वातन्त्र्य प्राप्त था, वह गौण हो गया और वे यज्ञाधीन हो गए। ब्राह्मणवर्ग ने अपना इतना अधिक वर्चस्व स्थापित कर लिया कि उसके द्वारा किए गए वैदिक मन्त्रपाठ और विधि-विधान के विना यज्ञ की संपूर्ति हो ही नहीं सकती थी। उन्होंने वेदपाठों के अध्ययन-उच्चारण को अपने वर्ग तक सीमित कर दिया और वेद उनकी अपनी संपत्ति हो गए। वेदों का दर्शन ब्राह्मण वर्ग तक सीमित हो जाने की प्रतिक्रिया का यह परिणाम हुआ कि उपनिषदों की रचना प्रारम्भ हई / औपनिषदिक ऋषियों ने प्रात्मस्वातंत्र्य के द्वार जन-साधारण के लिये उदघाटित किये। उपनिषत काल में विद्या, ज्ञान साधना के क्षेत्र में क्षत्रियों का प्रवेश हुना और आत्मविद्या को प्रमुख स्थान दिया एवं यह स्पष्ट किया कि धर्म का सच्चा अर्थ आध्यात्मिक उत्कर्ष है, जिसके द्वारा व्यक्ति वहिर्मुखता को छोड़कर वासनाओं के पाश से मुक्त होकर, शुद्ध सच्चिदानन्द-धन रूप आत्म-स्वरूप की उपलब्धि के लिये अग्रसर होकर उसे प्राप्त करता है / यही यथार्थ धर्म है। Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org