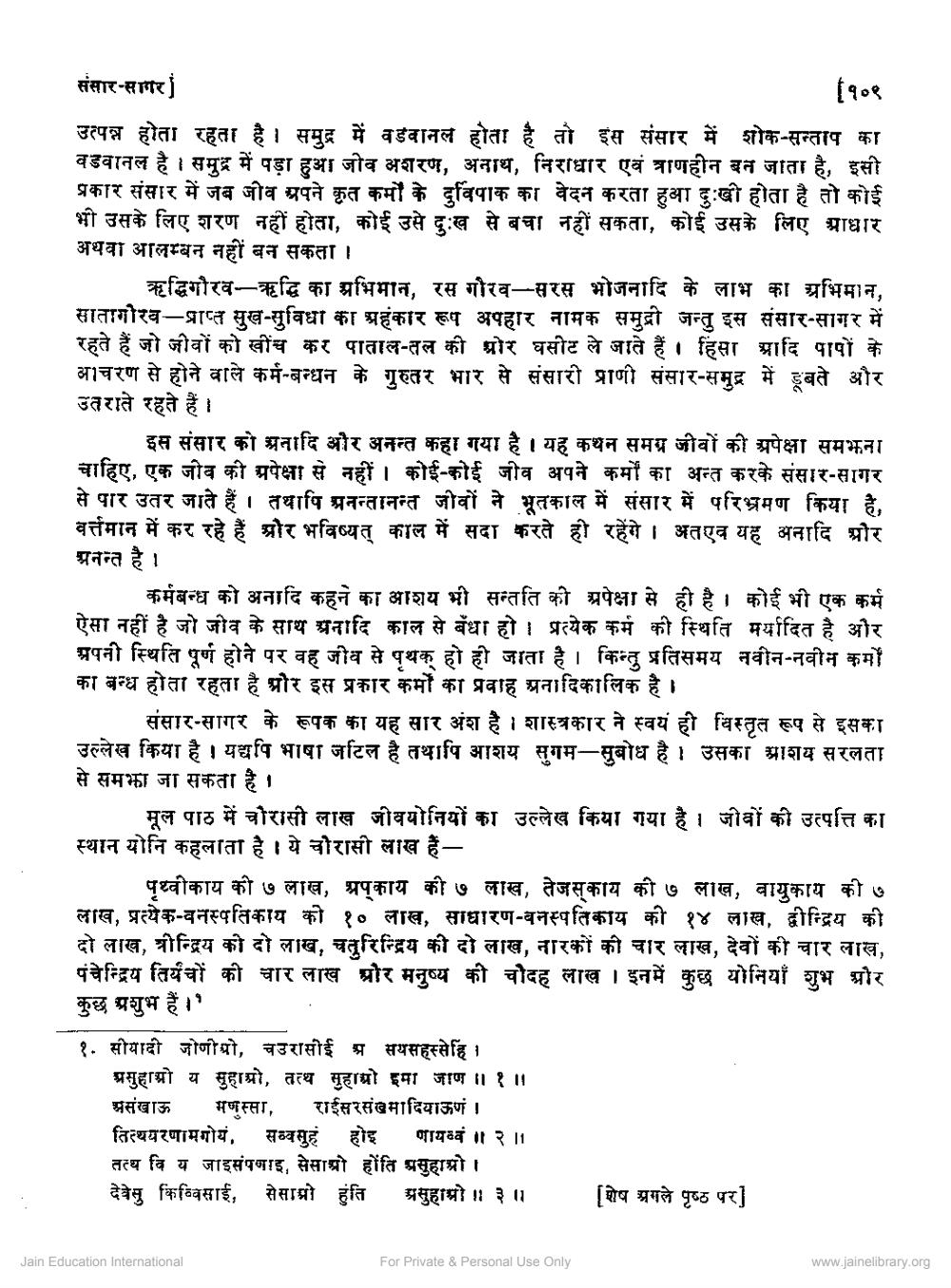________________ संसार-सागर उत्पन्न होता रहता है। समुद्र में वडवानल होता है तो इस संसार में शोक-सन्ताप का वडवानल है / समुद्र में पड़ा हुआ जीव अशरण, अनाथ, निराधार एवं त्राणहीन बन जाता है, इसी प्रकार संसार में जब जीव अपने कृत कर्मों के दुर्विपाक का वेदन करता हुआ दुःखी होता है तो कोई भी उसके लिए शरण नहीं होता, कोई उसे दुःख से बचा नहीं सकता, कोई उसके लिए आधार अथवा आलम्बन नहीं बन सकता। ऋद्धिगौरव-ऋद्धि का अभिमान, रस गौरव-सरस भोजनादि के लाभ का अभिमान, सातागौरव-प्राप्त सुख-सुविधा का अहंकार रूप अपहार नामक समुद्री जन्तु इस संसार-सागर में रहते हैं जो जीवों को खींच कर पाताल-तल की ओर घसीट ले जाते हैं। हिंसा आदि पापों के आचरण से होने वाले कर्म-बन्धन के गुरुतर भार से संसारी प्राणी संसार-समुद्र में डूबते और उतराते रहते हैं। इस संसार को अनादि और अनन्त कहा गया है / यह कथन समग्र जीवों की अपेक्षा समझना चाहिए, एक जीव की अपेक्षा से नहीं। कोई-कोई जीव अपने कर्मों का अन्त करके संसार-सागर से पार उतर जाते हैं / तथापि अनन्तानन्त जीवों ने भूतकाल में संसार में परिभ्रमण किया है, वर्तमान में कर रहे हैं और भविष्यत काल में सदा करते ही रहेंगे। अतएव यह अनादि और अनन्त है। __ कर्मबन्ध को अनादि कहने का आशय भी सन्तति की अपेक्षा से ही है। कोई भी एक कर्म ऐसा नहीं है जो जीव के साथ अनादि काल से बँधा हो। प्रत्येक कर्म की स्थिति मर्यादित है और अपनी स्थिति पूर्ण होने पर वह जीव से पृथक् हो ही जाता है। किन्तु प्रतिसमय नवीन-नवीन कर्मों का बन्ध होता रहता है और इस प्रकार कर्मों का प्रवाह अनादिकालिक है / संसार-सागर के रूपक का यह सार अंश है / शास्त्रकार ने स्वयं ही विस्तृत रूप से इसका उल्लेख किया है। यद्यपि भाषा जटिल है तथापि आशय सुगम-सुबोध है। उसका आशय सरलता से समझा जा सकता है। मूल पाठ में चौरासी लाख जीवयोनियों का उल्लेख किया गया है। जीवों की उत्पत्ति का स्थान योनि कहलाता है / ये चौरासी लाख हैं पृथ्वीकाय की 7 लाख, अपकाय की 7 लाख, तेजस्काय की 7 लाख, वायुकाय की 7 लाख, प्रत्येक-वनस्पतिकाय को 10 लाख, साधारण-वनस्पतिकाय की 14 लाख, द्वीन्द्रिय की दो लाख, त्रीन्द्रिय को दो लाख, चतुरिन्द्रिय की दो लाख, नारकों की चार लाख, देवों की चार लाख, पंचेन्द्रिय तिर्यंचों की चार लाख और मनुष्य की चौदह लाख / इनमें कुछ योनियाँ शुभ और कुछ अशुभ हैं।' 1. सीयादी जोणीयो, चउरासीई प्र सयसहस्सेहि / असुहायो य सुहायो, तत्थ सुहायो इमा जाण / / 1 / / असंखाऊ मणस्सा, राईसरसंखमादियाऊणं / तित्थयरणामगोयं, सव्वसुहं होइ णायब्वं // 2 // तत्य वि य जाइसंपणाइ, सेसाप्रो होंति असुहायो। देवेसु किदिवसाई, सेसाम्रो हंति असुहाम्रो।। 3 / / [शेष अगले पृष्ठ पर Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org