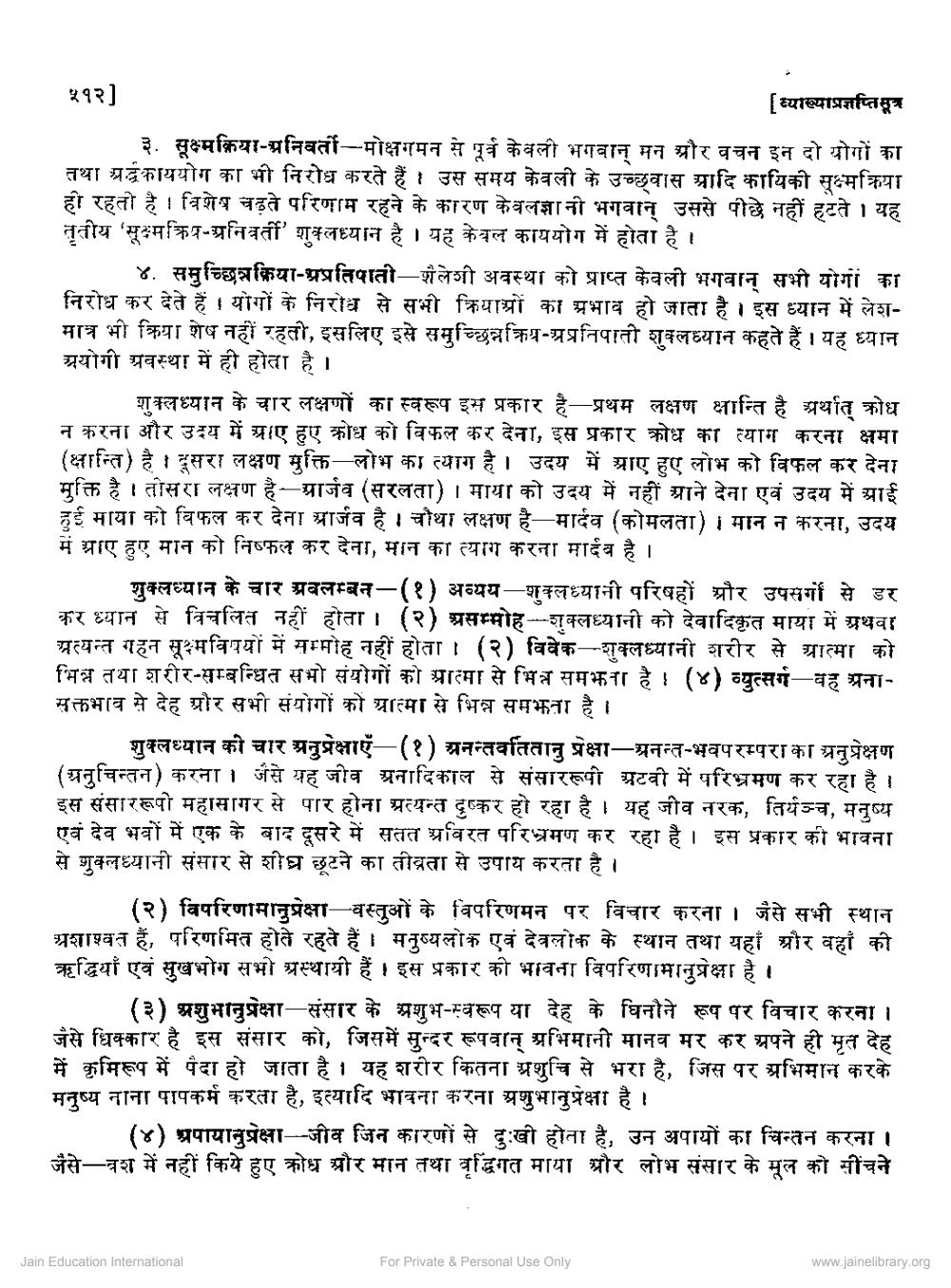________________ 512] [व्याख्याप्रज्ञप्तिसूत्र 3. सूक्ष्मनिया-अनिवर्ती--मोक्षगमन से पूर्व केवली भगवान् मन और वचन इन दो योगों का तथा अदकाययोग का भी निरोध करते हैं। उस समय केवली के उच्छ्वास आदि कायिकी सूक्ष्मक्रिया ही रहती है / विशेष चढ़ते परिणाम रहने के कारण केवलज्ञानी भगवान् उससे पीछे नहीं हटते / यह नृतीय 'सूक्ष्म क्रिष-अनिवर्ती' शुक्लध्यान है / यह केवल काययोग में होता है। 4. समुच्छिन्नक्रिया-प्रप्रतिपाती-शैलेगी अवस्था को प्राप्त केवली भगवान् सभी योगों का निरोध कर देते हैं / योगों के निरोध से सभी क्रियाओं का अभाव हो जाता है। इस ध्यान में लेशमात्र भी क्रिया शेष नहीं रहती, इसलिए इसे समुच्छिन्नक्रिय-अप्रनिपाती शुक्लध्यान कहते हैं / यह ध्यान अयोगी अवस्था में ही होता है / शुक्लध्यान के चार लक्षणों का स्वरूप इस प्रकार है-प्रथम लक्षण क्षान्ति है अर्थात् क्रोध न करना और उदय में अाए हुए क्रोध को विफल कर देना, इस प्रकार क्रोध का त्याग करना क्षमा (क्षान्ति) है। दूसरा लक्षण मुक्ति लोभ का त्याग है। उदय में पाए हुए लोभ को विफल कर देना मुक्ति है / तोसरा लक्षण है-पार्जव (सरलता)। माया को उदय में नहीं आने देना एवं उदय में आई हुई माया को विफल कर देना आर्जव है। चौथा लक्षण है—मार्दव (कोमलता)। मान न करना, उदय में लाए हुए मान को निष्फल कर देना, मान का त्याग करना मार्दव है / / शुक्लध्यान के चार अवलम्बन-(१) अव्यय-शुक्लध्यानी परिषहों और उपसर्गों से डर कर ध्यान से विचलित नहीं होता। (2) असम्मोहशुक्लध्यानी को देवादिकृत माया में अथवा अत्यन्त गहन सूक्ष्म विषयों में सम्मोह नहीं होता। (2) विवेक-शुक्लध्यानी शरीर से प्रात्मा को भिन्न तथा शरीर-सम्बन्धित सभो संयोगों को प्रात्मा से भित्र समझना है / (4) व्युत्सर्ग-वह अनासक्तभाव से देह और सभी संयोगों को प्रात्मा से भिन्न समझता है / शुक्लध्यान की चार अनुप्रेक्षाएँ—(१) अनन्ततितानु प्रेक्षा-अनन्त-भवपरम्परा का अनुप्रेक्षण (अनुचिन्तन) करना। जैसे यह जीव अनादिकाल से संसाररूपी अटवी में परिभ्रमण कर रहा है / इस संसाररूपी महासागर से पार होना अत्यन्त दुष्कर हो रहा है। यह जीव नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य एवं देव भवों में एक के बाद दूसरे में सतत अविरत परिभ्रमण कर रहा है। इस प्रकार की भावना से शुक्लध्यानी संसार से शीघ्र छूटने का तीव्रता से उपाय करता है। (2) विपरिणामानुप्रेक्षा-वस्तुओं के विपरिणमन पर विचार करना / जैसे सभी स्थान अशाश्वत हैं, परिणमित होते रहते हैं। मनुष्यलोक एवं देवलोक के स्थान तथा यहाँ और वहाँ की ऋद्धियाँ एवं सुखभोग सभी अस्थायी हैं / इस प्रकार की भावना विपरिणामानुप्रेक्षा है। (3) अशुभानुप्रेक्षा-संसार के अशुभ-स्वरूप या देह के घिनौने रूप पर विचार करना / जैसे धिक्कार है इस संसार को, जिसमें सून्दर रूपवान अभिमानी मानव मर कर अपने ही मृत देह में कृमिरूप में पैदा हो जाता है। यह शरीर कितना अशुचि से भरा है, जिस पर अभिमान करके मनुष्य नाना पापकर्म करता है, इत्यादि भावना करना अशुभानुप्रेक्षा है। (4) अपायानुप्रेक्षा--जीव जिन कारणों से दुःखी होता है, उन अपायों का चिन्तन करना / जैसे-वश में नहीं किये हुए क्रोध और मान तथा वृद्धिंगत माया और लोभ संसार के मूल को सींचने Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org