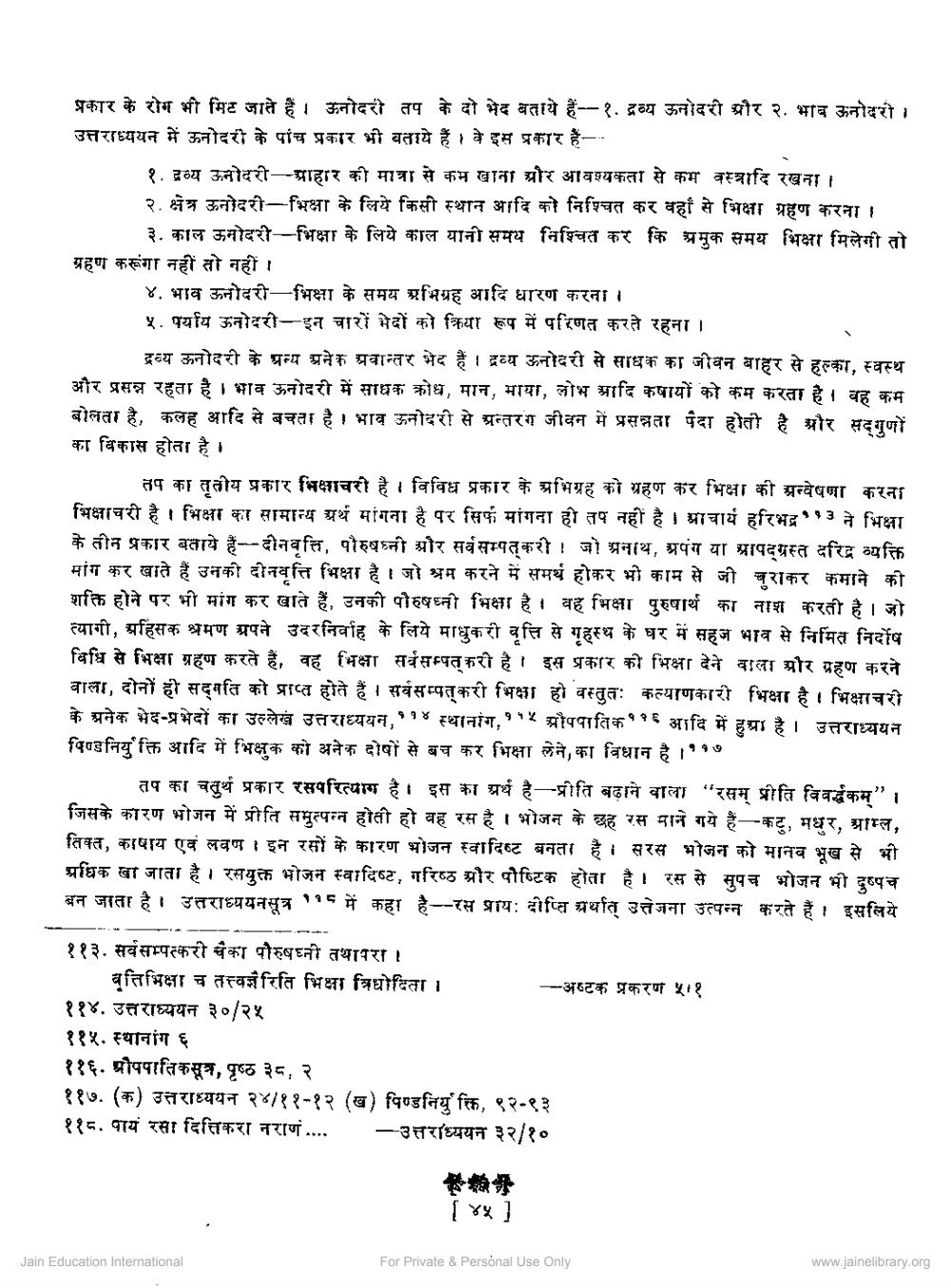________________ प्रकार के रोग भी मिट जाते हैं। ऊनोदरी तप के दो भेद बताये हैं--१. द्रव्य ऊलोदरी और 2. भाब ऊनोदरी। उत्तराध्ययन में ऊनोदरी के पांच प्रकार भी बताये हैं। वे इस प्रकार है 1. द्रव्य ऊनोदरी-माहार की मात्रा से कम खाना और आवश्यकता से कम वस्त्रादि रखना। 2. क्षेत्र ऊनोदरी-भिक्षा के लिये किसी स्थान आदि को निशिचत कर वहाँ से भिक्षा ग्रहण करना / 3. काल ऊमोदरी-भिक्षा के लिये काल यानी समय निश्चित कर कि अमुक समय भिक्षा मिलेगी तो ग्रहण करूंगा नहीं तो नहीं / 4. भाव ऊनोदरी-भिक्षा के समय अभिग्रह आदि धारण करना / 5. पर्याय ऊनोदरी-इन चारों भेदों को क्रिया रूप में परिणत करते रहना। द्रव्य ऊनोदरी के अन्य अनेक अवान्तर भेद हैं / द्रव्य ऊनोदरी से साधक का जीवन बाहर से हल्का, स्वस्थ और प्रसन्न रहता है। भाव ऊनोदरी में साधक क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषायों को कम करता है। वह कम बोलता है, कलह आदि से बचता है। भाव ऊनोदरी से अन्तरग जीवन में प्रसन्नता पैदा होती है और सदगुणों का विकास होता है। तप का ततीय प्रकार भिक्षाचरी है। विविध प्रकार के अभिग्रह को ग्रहण कर भिक्षा की अन्वेषणा करना भिक्षाचरी है / भिक्षा का सामान्य अर्थ मांगना है पर सिर्फ मांगना ही तप नहीं है / आचार्य हरिभद्र'' ने भिक्षा के तीन प्रकार बताये हैं---दोनवति, पौरुषघ्नी और सर्वसम्पत करी। जो अनाथ, अपंग या प्रापद्ग्रस्त दरिद्र व्यक्ति मांग कर खाते हैं उनकी दीनवृत्ति भिक्षा है। जो श्रम करने में समर्थ होकर भी काम से जी चुराकर कमाने की शक्ति होने पर भी मांग कर खाते हैं, उनकी पौरुषनी भिक्षा है। वह भिक्षा पुरुषार्थ का नाश करती है। जो त्यागी, अहिंसक श्रमण अपने उदरनिर्वाह के लिये माधुकरी वृत्ति से गृहस्थ के घर में सहज भाव से निर्मित निर्दोष विधि से भिक्षा ग्रहण करते हैं, वह भिक्षा सर्वसम्पत्करी है। इस प्रकार की भिक्षा देने वाला और ग्रहण करने वाला, दोनों ही सद्वति को प्राप्त होते हैं / सर्वसम्पत्करी भिक्षा हो वस्तुतः कल्याणकारी भिक्षा है। भिक्षाचरी के अनेक भेद-प्रभेदों का उल्लेख उत्तराध्ययन,' 14 स्थानांग,११५ प्रौपपातिक 116 आदि में हया है। उत्तराध्ययन पिण्डनियुक्ति आदि में भिक्षुक को अनेक दोषों से बच कर भिक्षा लेने, का विधान है / '17 तप का चतुर्थ प्रकार रसपरित्याग है। इस का अर्थ है-प्रीति बढ़ाने वाला "रसम प्रीति विवर्द्धकम"। ग भोजन में प्रीति समुत्पन्न होती हो वह रस है / भोजन के छह रस माने गये हैं-कटु, मधुर, आम्ल, तिक्त, काषाय एवं लवण / इन रसों के कारण भोजन स्वादिष्ट बनता है। सरस भोजन को मानव भूख से भी अधिक खा जाता है। रसयुक्त भोजन स्वादिष्ट, गरिष्ठ और पौष्टिक होता है। रस से सुपच भोजन भी दुष्पच बन जाता है। उत्तराध्ययनसूत्र 118 में कहा है--रस प्राय: दीप्ति अर्थात् उत्तेजना उत्पन्न करते हैं। इसलिये 113. सर्वसम्पत्करी चैका पौरुषघ्नी तथापरा / बत्तिभिक्षा च तत्त्वज्ञ रिति भिक्षा विधोदिता / --अष्टक प्रकरण 511 114. उत्तराध्ययन 30/25 115. स्थानांग 6 116. प्रौपपातिकसूत्र, पृष्ठ 38, 2 117. (क) उत्तराध्ययन 24/11-12 (ख) पिण्डनियुक्ति, 92-93 118. पायं रसा दित्तिकरा नराणं.... -उत्तराध्ययन 32/10 [45 ] www.jainelibrary.org Jain Education International For Private & Personal Use Only