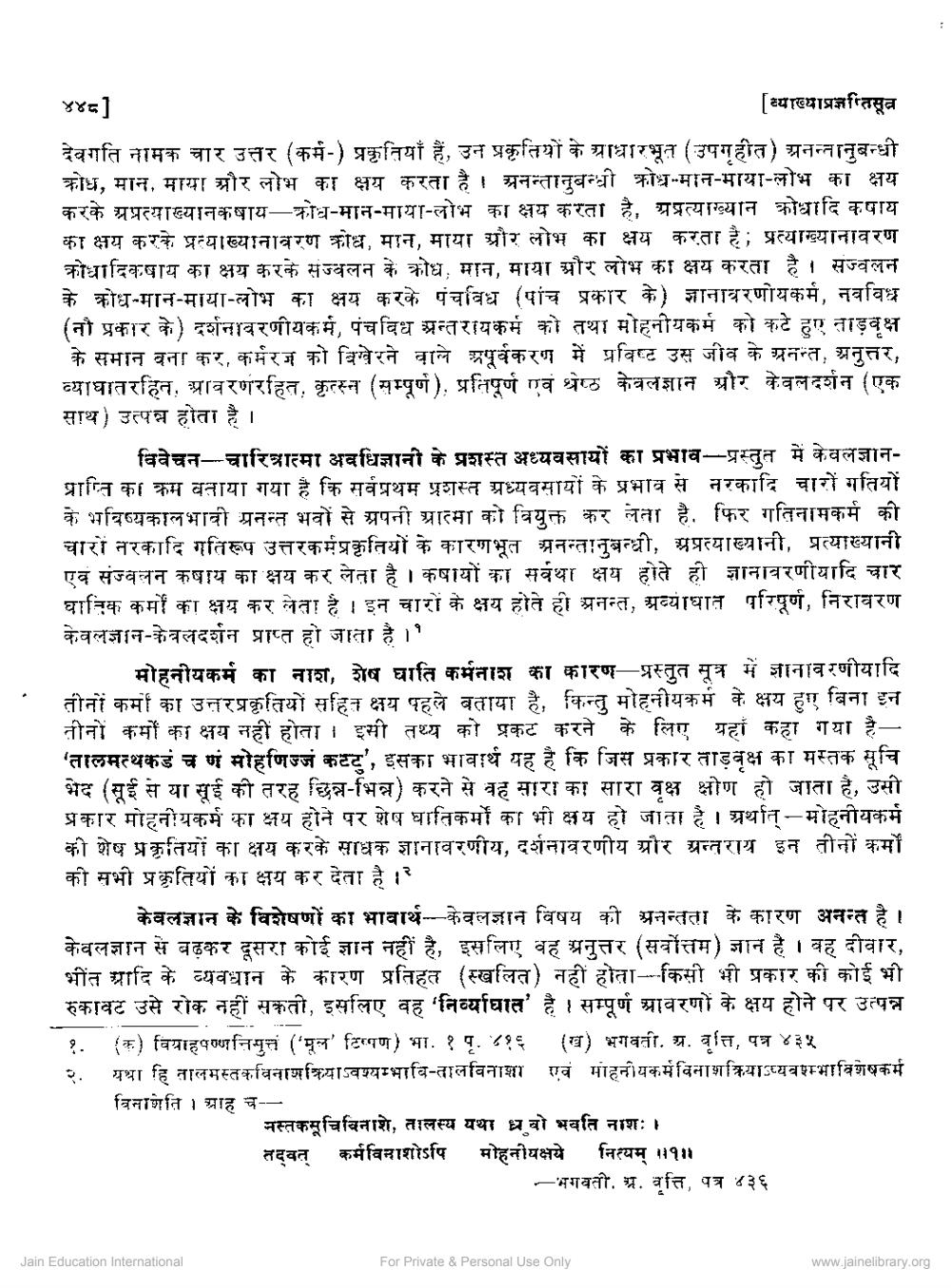________________ 448] [व्याख्याप्रज्ञप्तिसूत्र देवगति नामक चार उत्तर (कर्म-) प्रकृतियाँ हैं, उन प्रकृतियों के अाधारभूत (उपमहीत) अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ का क्षय करता है / अनन्तानुबन्धी क्रोध-मान-माया-लोभ का क्षय करके अप्रत्याख्यानकषाय-क्रोध-मान-माया-लोभ का क्षय करता है, अप्रत्याख्यान कोधादि कषाय का क्षय करके प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया और लोभ का क्षय करता है ; प्रत्याख्यानावरण क्रोधादिकषाय का क्षय करके सज्वलन के क्रोध, मान, माया और लोभ का क्षय करता है। संज्वलन के क्रोध-मान-माया-लोभ का क्षय करके पंचविध (पांच प्रकार के) ज्ञानावरणोयकर्म, नवविध (नौ प्रकार के) दर्शनावरणीयकर्म, पंचविध अन्तरायकर्म को तथा मोहनीयकर्म को कटे हुए ताइवृक्ष के समान बना कर, कर्मरज को बिखेरने वाले अपूर्वकरण में प्रविष्ट उस जीव के अनन्त, अनुत्तर, घातरहित, आवरणरहित. कृत्स्न (सम्पूर्ण), प्रतिपूर्ण एवं श्रेष्ठ केवलज्ञान और केवलदर्शन (एक साथ) उत्पन्न होता है / / विवेचन-चारित्रात्मा अवधिज्ञानी के प्रशस्त अध्यवसायों का प्रभाव-प्रस्तुत में केवलज्ञानप्राप्ति का क्रम बताया गया है कि सर्वप्रथम प्रशस्त अध्यवसायों के प्रभाव से नरकादि चारों गतियों के भविष्यकालभावी अनन्त भवों से अपनी आत्मा को वियुक्त कर लेता है. फिर गतिनामकर्म की चारों तरकादि गतिरूप उत्तरकर्मप्रकृतियों के कारणभूत अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी एवं संज्वलन कषाय का क्षय कर लेता है। कषायों का सर्वथा क्षय होते ही ज्ञानावरणीयादि चार घानिक कर्मों का क्षय कर लेता है / इन चारों के क्षय होते ही अनन्त, अव्याघात परिपूर्ण, निरावरण केवलज्ञान-केवलदर्शन प्राप्त हो जाता है।' मोहनीयकर्म का नाश, शेष घाति कर्मनाश का कारण प्रस्तुत मूत्र में ज्ञानावरणीयादि तीनों कर्मों का उत्तरप्रकुतियों सहित क्षय पहले बताया है, किन्तु मोहनीयकर्म के क्षय हुए बिना इन तीनों कों का क्षय नहीं होता। इसी तथ्य को प्रकट करने के लिए यहाँ कहा गया है'तालमत्थकडं च णं मोहणिज्जं कटटु', इसका भावार्थ यह है कि जिस प्रकार ताडवृक्ष का मस्तक सूचि भेद (सूई से या सूई की तरह छिन्न-भिन्न) करने से वह सारा का सारा वृक्ष क्षीण हो जाता है, उसी प्रकार मोहनीयकर्म का क्षय होने पर शेष घातिकर्मों का भी क्षय हो जाता है / अर्थात् –मोहनीयकर्म को शेष प्रकृतियों का क्षय करके साधक ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अन्तराय इन तीनों कर्मों को सभी प्रकृतियों का क्षय कर देता है। केवलज्ञान के विशेषणों का भावार्थ-केवलज्ञान विषय की अनन्तता के कारण अनन्त है। केवलज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए वह अनुत्तर (सर्वोत्तम) ज्ञान है / वह दीवार, भीत आदि के व्यवधान के कारण प्रतिहत (स्खलित) नहीं होता--किसी भी प्रकार की कोई भी रुकावट उसे रोक नहीं सकती, इसलिए वह 'नियाघात' है / सम्पूर्ण आवरणों के क्षय होने पर उत्पन्न 1. (क) विवाहपरणनिमुत्तं ('मूल' टिप्पण) भा. 1 पृ. 416 (ख) भगवती. अ. वृत्ति, पत्र 435 2. यथा हि तालमस्तविनाशक्रियाऽवश्यम्भावि-तालविनाशा एवं माहनीयकर्मविनाशक्रियाऽप्यवाभाविशेषकर्म विनाश नि / अाह च-- नस्तकमूचिविनाशे, तालस्य यथा ध्र वो भवति नाशः / तद्वत् कर्मविनाशोऽपि मोहनीयक्षये नित्यम् // 1 // -भगवती. अ. अत्ति, पत्र 436 Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org