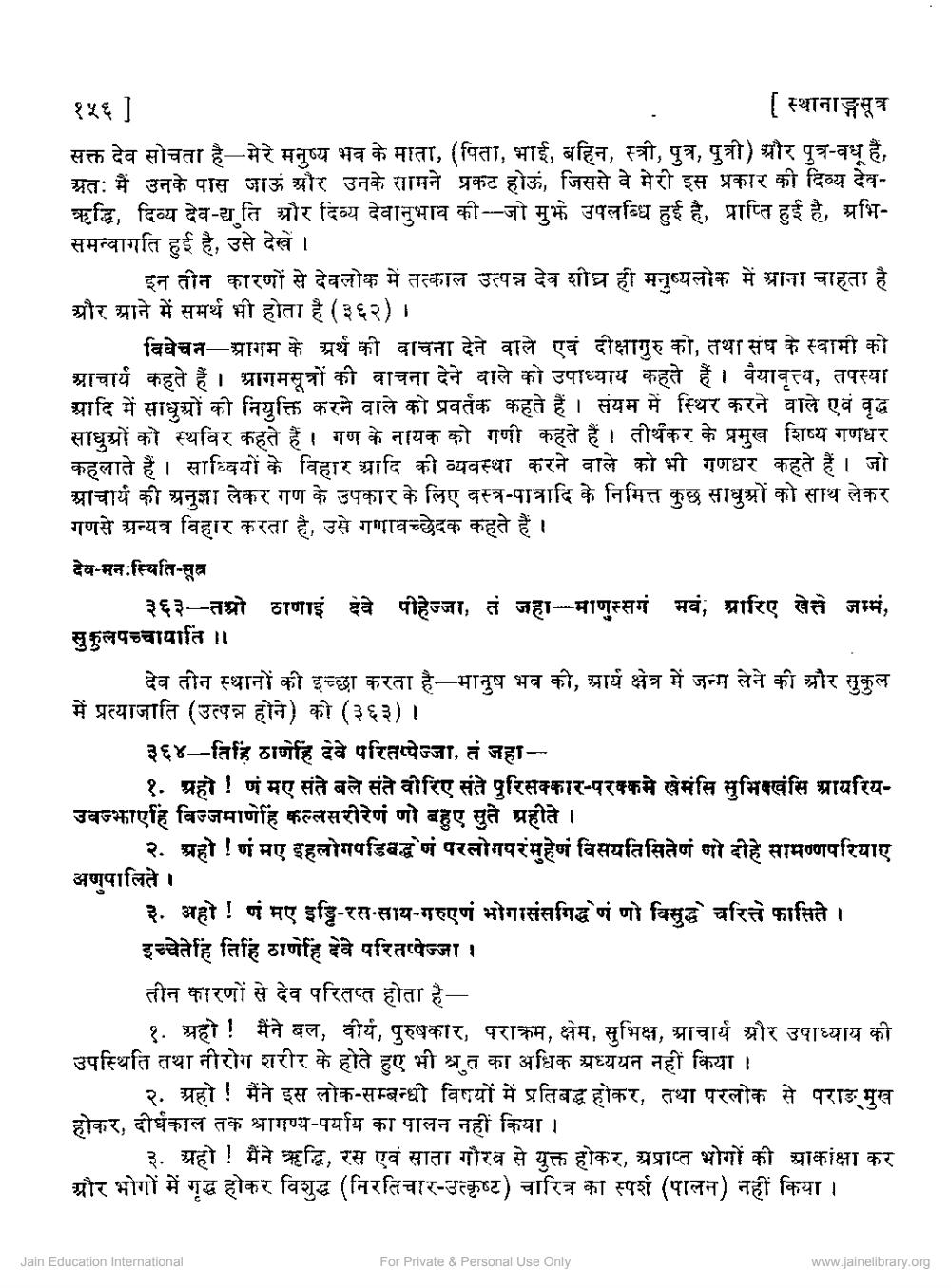________________ 156 ] [ स्थानाङ्गसूत्र सक्त देव सोचता है—मेरे मनुष्य भव के माता, (पिता, भाई, बहिन, स्त्री, पुत्र, पुत्री) और पुत्र-वधु हैं, अतः मैं उनके पास जाऊं और उनके सामने प्रकट होऊं, जिससे वे मेरी इस प्रकार की दिव्य देवऋद्धि, दिव्य देव-ध ति और दिव्य देवानुभाव की-जो मुझे उपलब्धि हुई है, प्राप्ति हुई है, अभिसमन्वागति हुई है, उसे देखें / इन तीन कारणों से देवलोक में तत्काल उत्पन्न देव शीघ्र ही मनुष्यलोक में आना चाहता है और आने में समर्थ भी होता है (362) / विवेचन—पागम के अर्थ की वाचना देने वाले एवं दीक्षागुरु को, तथा संघ के स्वामी को आचार्य कहते हैं। आगमसूत्रों की वाचना देने वाले को उपाध्याय कहते हैं। वैयावृत्त्य, तपस्या आदि में साधुओं की नियुक्ति करने वाले को प्रवर्तक कहते हैं / संयम में स्थिर करने वाले एवं वृद्ध साधुओं को स्थविर कहते हैं। गण के नायक को गणी कहते हैं। तीर्थंकर के प्रमुख शिष्य गणधर कहलाते हैं / साध्वियों के विहार आदि की व्यवस्था करने वाले को भी गणधर कहते हैं / जो आचार्य की अनुज्ञा लेकर गण के उपकार के लिए वस्त्र-पात्रादि के निमित्त कुछ साधुओं को साथ लेकर गणसे अन्यत्र विहार करता है, उसे गणावच्छेदक कहते हैं / देव-मन:स्थिति-सूत्र ३६३-तो ठाणाई देवे पोहेज्जा, तं जहा---माणुस्सगं मवं, प्रारिए खेत्ते जम्म, सुकुलपच्चायाति // देव तीन स्थानों की इच्छा करता है-मानुष भव की, आर्य क्षेत्र में जन्म लेने की और सुकुल में प्रत्याजाति (उत्पन्न होने) को (363) / ३६४--तिहि ठाणेहि देवे परितप्पेज्जा, तं जहा 1. ग्रहो ! णं मए संते बले संते वोरिए संते पुरिसक्कार-परक्कमे खेमंसि सुभिक्खंसि पायरियउवज्झाएहि विज्जमाणेहिं कल्लसरीरेणं णो बहुए सुते प्रहीते / 2. अहो ! णं मए इहलोगपडिबद्धणं परलोगपरंमुहेणं विसयतिसितेणं णो दोहे सामण्णपरियाए अणुपालिते। 3. अहो ! णं मए इडि-रस-साय-गरुएणं भोगासंसगिद्धणं णो विसुद्ध चरित्ते फासिते। इच्चेतेहि तिहि ठाणेहिं देवे परितप्पेज्जा / तीन कारणों से देव परितप्त होता है 1. अहो ! मैंने बल, वीर्य, पुरुषकार, पराक्रम, क्षेम, सुभिक्ष, आचार्य और उपाध्याय की उपस्थिति तथा नीरोग शरीर के होते हुए भी श्रुत का अधिक अध्ययन नहीं किया। 2. अहो ! मैंने इस लोक-सम्बन्धी विषयों में प्रतिबद्ध होकर, तथा परलोक से पराङ मुख होकर, दीर्घकाल तक श्रामण्य-पर्याय का पालन नहीं किया। 3. अहो ! मैंने ऋद्धि, रस एवं साता गौरव से युक्त होकर, अप्राप्त भोगों की आकांक्षा कर और भोगों में गृद्ध होकर विशुद्ध (निरतिचार-उत्कृष्ट) चारित्र का स्पर्श (पालन) नहीं किया। Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org