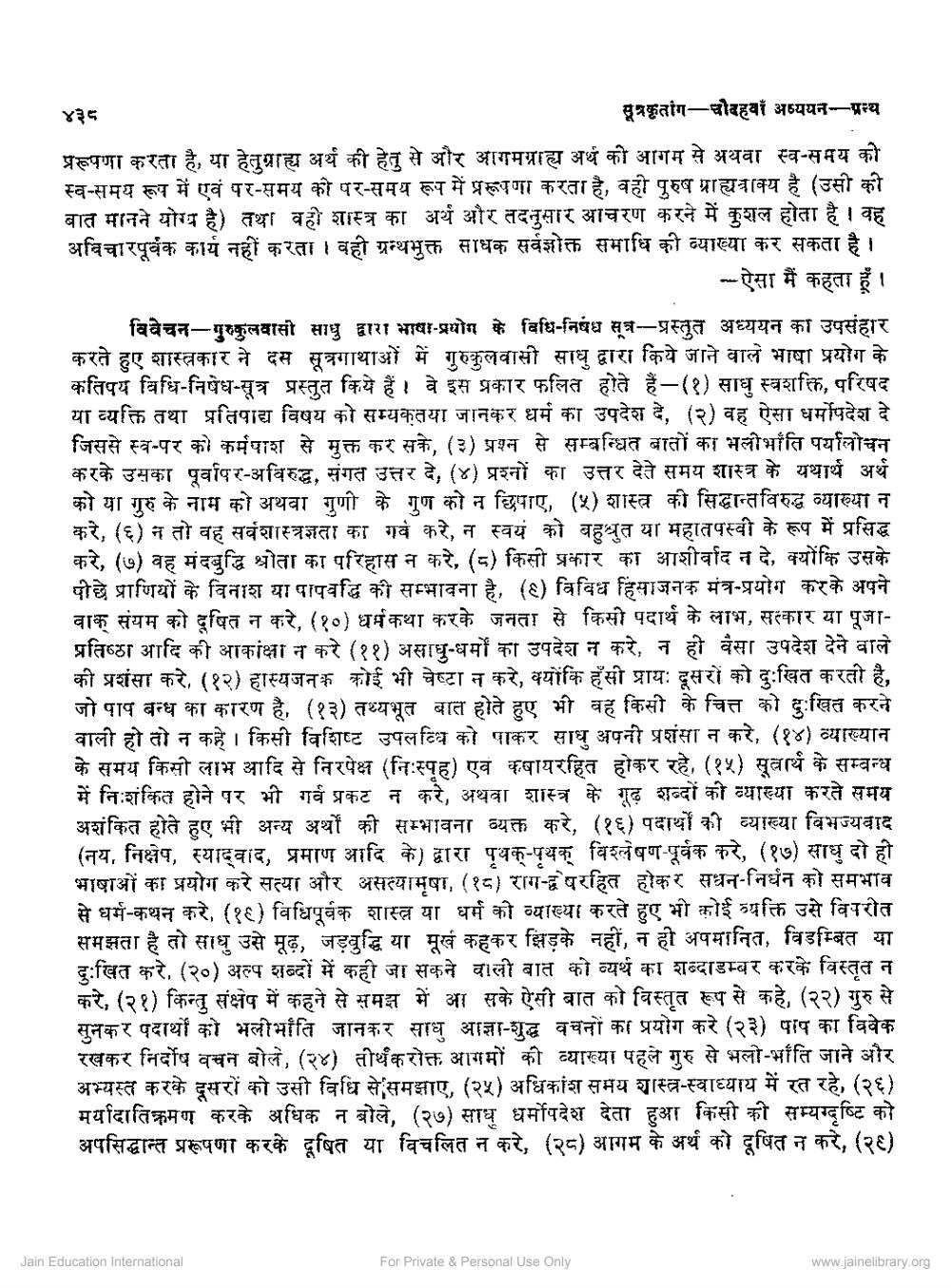________________ 438 सूत्रकृतांग-चौदहवाँ अध्ययन-प्रस्थ प्ररूपणा करता है, या हेतुग्राह्य अर्थ की हेतु से और आगमग्राह्य अर्थ को आगम से अथवा स्व-समय को स्व-समय रूप में एवं पर-समय को पर-समय रूप में प्ररूपणा करता है, वही पुरुष ग्राह्यवाक्य है (उसी की बात मानने योग्य है) तथा वही शास्त्र का अर्थ और तदनुसार आचरण करने में कुशल होता है / वह अविचारपूर्वक कार्य नहीं करता / वही ग्रन्थमुक्त साधक सर्वज्ञोक्त समाधि की व्याख्या कर सकता है। ~ऐसा मैं कहता हूँ। विवेचन-गुरुकुलवासी साधु द्वारा भाषा-प्रयोग के विधि-निबंध सूत्र-प्रस्तुत अध्ययन का उपसंहार स सूत्रगाथाओं में गुरुकुलवासी साध द्वारा किये जाने वाले कतिपय विधि-निषेध-सूत्र प्रस्तुत किये हैं। वे इस प्रकार फलित होते हैं-(१) साधु स्वशक्ति, परिषद या व्यक्ति तथा प्रतिपाद्य विषय को सम्यकतया जानकर धर्म का उपदेश दे, (2) वह ऐसा धर्मोपदेश दे जिससे स्व-पर को कर्मपाश से मुक्त कर सके, (3) प्रश्न से सम्बन्धित बातों का भलीभाँति पर्यालोचन करके उसका पूर्वापर-अविरुद्ध, संगत उत्तर दे, (4) प्रश्नों का उत्तर देते समय शास्त्र के यथार्थ अर्थ को या गुरु के नाम को अथवा गुणी के गुण को न छिपाए, (5) शास्त्र की सिद्धान्तविरुद्ध व्याख्या न , (6) न तो वह सर्वशास्त्रज्ञता का गर्व करे, न स्वयं को बहथत या महातपस्वी के रूप में प्रसिद्ध करे, (7) वह मंदबुद्धि श्रोता का परिहास न करे, (8) किसी प्रकार का आशीर्वाद न दे, क्योंकि उसके पीछे प्राणियों के विनाश या पापवद्धि की सम्भावना है, (8) विविध हिंसाजनक मंत्र प्रयोग करके अपने वाक् संयम को दुषित न करे, (10) धर्मकथा करके जनता से किसी पदार्थ के लाभ, सत्कार या पूजाप्रतिष्ठा आदि की आकांक्षा न करे (11) असाधु-धर्मों का उपदेश न करे, न ही वैसा उपदेश देने वाले की प्रशंसा करे, (12) हास्यजनक कोई भी चेष्टा न करे, क्योंकि हँसी प्रायः दूसरों को दुःखित करती है, जो पाप बन्ध का कारण है, (13) तथ्यभूत बात होते हुए भी वह किसी के चित्त को दुःखित करने वाली हो तो न कहे। किसी विशिष्ट उपलब्धि को पाकर साध अपनी प्रशंसा न करे के समय किसी लाभ आदि से निरपेक्ष (निःस्पृह) एवं कषायरहित होकर रहे, (15) सूत्रार्थ के सम्बन्ध में निःशंकित होने पर भी गर्व प्रकट न करे, अथवा शास्त्र के गूढ़ शब्दों की व्याख्या करते समय अशंकित होते हुए भी अन्य अर्थों की सम्भावना व्यक्त करे, (16) पदार्थों की व्याख्या विभज्यवाद (नय, निक्षेप, स्याद्वाद, प्रमाण आदि के) द्वारा पृथक्-पृथक् विश्लेषण-पूर्वक करे, (17) साधु दो ही भाषाओं का प्रयोग करे सत्या और असत्यामृषा, (18) राग-द्वषरहित होकर सधन-निर्धन को समभाव से धर्म-कथन करे, (16) विधिपूर्वक शास्त्र या धर्म को व्याख्या करते हुए भी कोई व्यक्ति उसे विपरीत समझता है तो साधु उसे मूढ़, जड़वुद्धि या मूर्ख कहकर झिड़के नहीं, न ही अपमानित, विडम्बित या दःखित करे, (20) अल्प शब्दों में कही जा सकने वाली बात को व्यर्थ का शब्दाडम्बर करके विस्तृत न करे, (21) किन्तु संक्षेप में कहने से समझ में आ सके ऐसी बात को विस्तृत रूप से कहे, (22) गुरु से सुनकर पदार्थों को भलीभांति जानकर साधु आज्ञा-शुद्ध वचनों का प्रयोग करे (23) पाप का विवेक रखकर निर्दोष वचन बोले. (24) तीर्थंकरोक्त आगमों की व्याख्या पहले गुरु से भली-भांति जाने और अभ्यस्त करके दूसरों को उसी विधि से समझाए, (25) अधिकांश समय शास्त्र-स्वाध्याय में रत रहे, (26) मर्यादातिक्रमण करके अधिक न बोले, (27) साधु धर्मोपदेश देता हुआ किसी की सम्यग्दृष्टि को अपसिद्धान्त प्ररूपणा करके दूषित या विचलित न करे, (28) आगम के अर्थ को दूषित न करे, (29) Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org