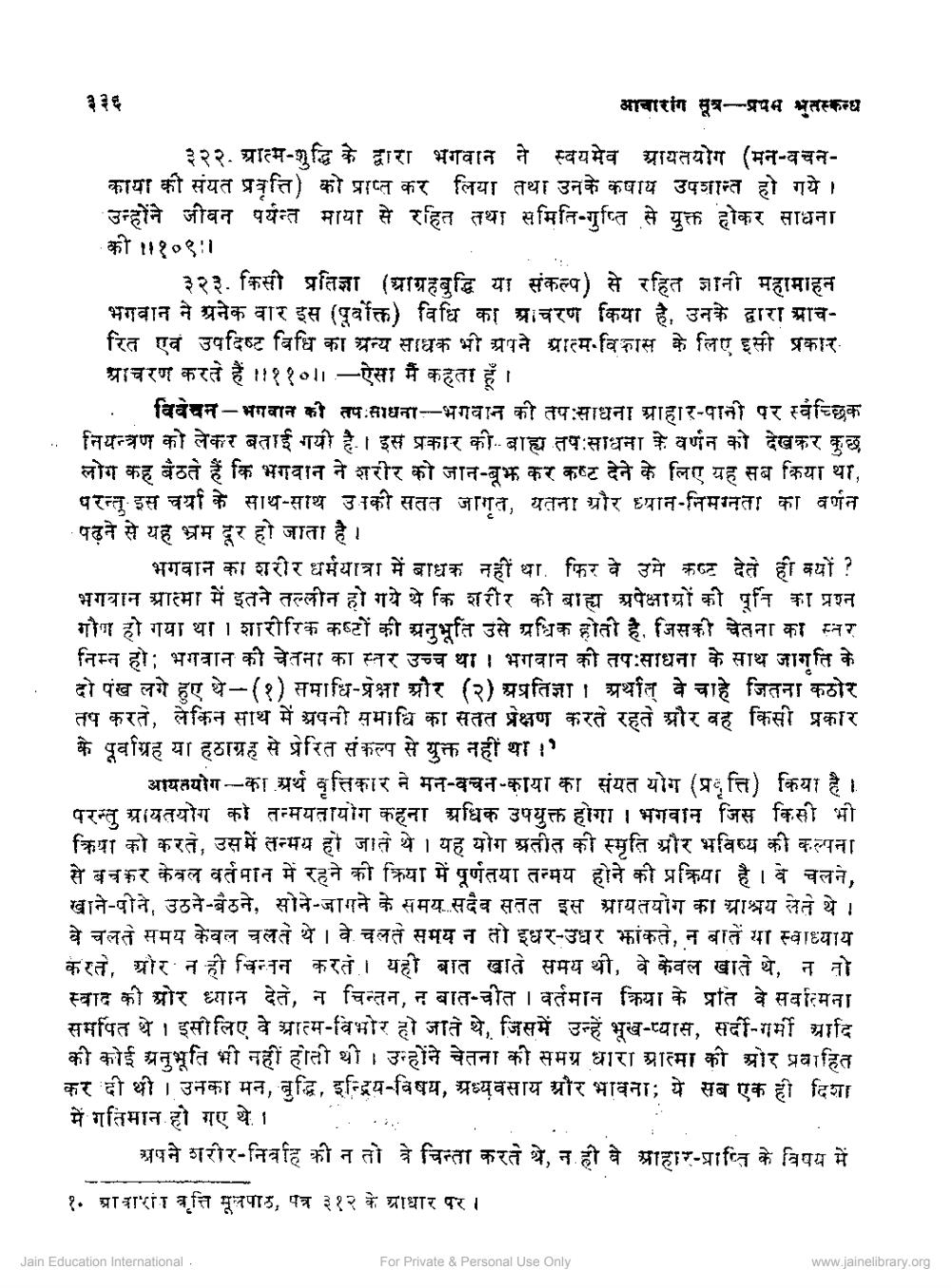________________ आचारांग सूत्र-प्रपम भुतस्कन्ध 322. प्रात्म-शुद्धि के द्वारा भगवान ने स्वयमेव आयतयोग (मन-वचनकाया की संयत प्रवृत्ति) को प्राप्त कर लिया तथा उनके कषाय उपशान्त हो गये। उन्होंने जीवन पर्यन्त माया से रहित तथा समिति-गुप्ति से युक्त होकर साधना की // 109 / 323. किसी प्रतिज्ञा (याग्रहबुद्धि या संकल्प) से रहित ज्ञानी महामाहन भगवान ने अनेक वार इस (पूर्वोक्त) विधि का प्राचरण किया है, उनके द्वारा आचरित एवं उपदिष्ट विधि का अन्य साधक भी अपने प्रात्म-विकास के लिए इसी प्रकार आचरण करते हैं / 110 / / —ऐसा मैं कहता हूँ। . विवेचन - भगवान की तपःसाधना-भगवान की तपःसाधना पाहार-पानी पर स्वैच्छिक नियन्त्रण को लेकर बताई गयी है। इस प्रकार की. बाह्य तप:साधना के वर्णन को देखकर कुछ लोग कह बैठते हैं कि भगवान ने शरीर को जान-बूझ कर कष्ट देने के लिए यह सब किया था, परन्तु इस चर्या के साथ-साथ उसकी सतत जागत, यतना और ध्यान-निमग्नता का वर्णन पढ़ने से यह भ्रम दूर हो जाता है। / भगवान का शरीर धर्मयात्रा में बाधक नहीं था. फिर वे उसे कष्ट देते ही क्यों ? भगवान आत्मा में इतने तल्लीन हो गये थे कि शरीर की बाह्य अपेक्षानों की पूर्ति का प्रश्न गौण हो गया था / शारीरिक कष्टों की अनुभूति उसे अधिक होती है, जिसकी चेतना का स्तर निम्न हो; भगवान की चेतना का स्तर उच्च था। भगवान की तपःसाधना के साथ जागति के दो पंख लगे हुए थे-(१) समाधि-प्रेना और (2) अप्रतिज्ञा / अर्थात् वे चाहे जितना कठोर तप करते, लेकिन साथ में अपनी समाधि का सतत प्रेक्षण करते रहते और वह किसी प्रकार के पूर्वाग्रह या हठाग्रह से प्रेरित संकल्प से युक्त नहीं था।' __ आयतयोग-का अर्थ वृत्तिकार ने मन-वचन-काया का संयत योग (प्रवृत्ति) किया है। परन्तु आयतयोग को तन्मयतायोग कहना अधिक उपयुक्त होगा / भगवान जिस किसी भी या को करते, उस में तन्मय हो जाते थे। यह योग अतीत की स्मति और भविष्य की कल्पना से बचकर केवल वर्तमान में रहने की क्रिया में पूर्णतया तन्मय होने की प्रक्रिया है। वे चलने, खाने-पीने, उठने-बैठने, सोने-जागने के समय सदैव सतत इस आयतयोग का ग्राश्रय लेते थे। वे चलते समय केवल चलते थे / वे चलते समय न तो इधर-उधर झांकते, न बातें या स्वाध्याय करते, ग्र , और न ही चिन्तन करते। यही बात खाते समय थी, वे केवल खाते थे, न तो स्वाद की ओर ध्यान देते, न चिन्तन, न बात-चीत / वर्तमान क्रिया के प्रति वे सर्वात्मना समर्पित थे। इसीलिए वे आत्म-विभोर हो जाते थे, जिसमें उन्हें भूख-प्यास, सर्दी-गर्मी आदि की कोई अनुभूति भी नहीं होती थी। उन्होंने चेतना की समग्र धारा प्रात्मा की ओर प्रवाहित कर दी थी। उनका मन, बुद्धि, इन्द्रिय-विषय, अध्यवसाय और भावना; ये सब एक ही दिशा में गतिमान हो गए थे / अपने शरीर-निर्वाह की न तो वे चिन्ता करते थे, न ही वे आहार-प्राप्ति के विषय में 1. प्रावासा वृत्ति मूलपाठ, पत्र 312 के आधार पर / Jain Education International . For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org