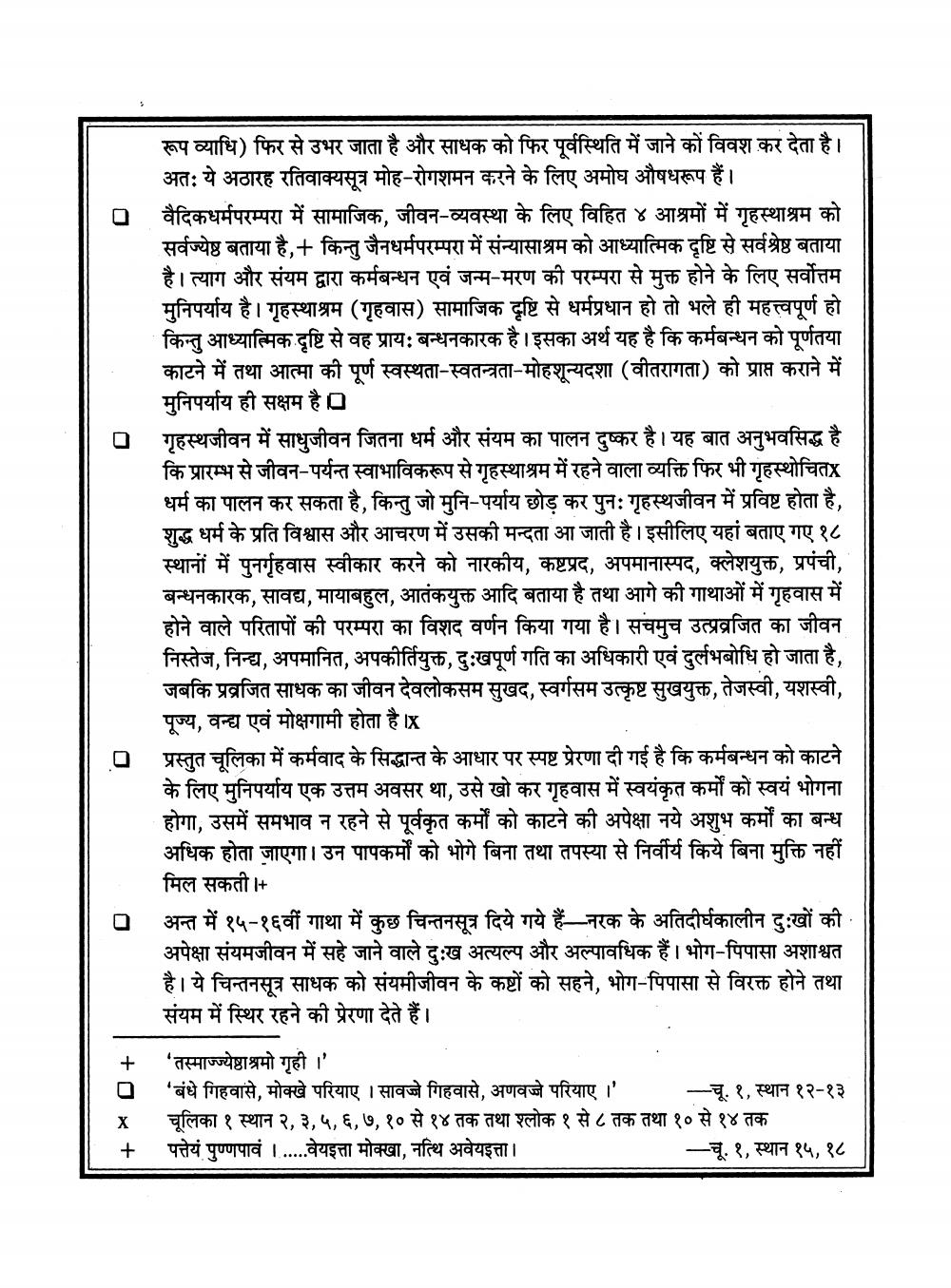________________
रूप व्याधि) फिर से उभर जाता है और साधक को फिर पूर्वस्थिति में जाने को विवश कर देता है। अतः ये अठारह रतिवाक्यसूत्र मोह-रोगशमन करने के लिए अमोघ औषधरूप हैं। वैदिकधर्मपरम्परा में सामाजिक, जीवन-व्यवस्था के लिए विहित ४ आश्रमों में गृहस्थाश्रम को सर्वज्येष्ठ बताया है, किन्तु जैनधर्मपरम्परा में संन्यासाश्रम को आध्यात्मिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ बताया है। त्याग और संयम द्वारा कर्मबन्धन एवं जन्म-मरण की परम्परा से मुक्त होने के लिए सर्वोत्तम मुनिपर्याय है। गृहस्थाश्रम (गृहवास) सामाजिक दृष्टि से धर्मप्रधान हो तो भले ही महत्त्वपूर्ण हो किन्तु आध्यात्मिक दृष्टि से वह प्रायः बन्धनकारक है। इसका अर्थ यह है कि कर्मबन्धन को पूर्णतया काटने में तथा आत्मा की पूर्ण स्वस्थता-स्वतन्त्रता-मोहशून्यदशा (वीतरागता) को प्राप्त कराने में
मुनिपर्याय ही सक्षम है। " गृहस्थजीवन में साधुजीवन जितना धर्म और संयम का पालन दुष्कर है। यह बात अनुभवसिद्ध है
कि प्रारम्भ से जीवन-पर्यन्त स्वाभाविकरूप से गृहस्थाश्रम में रहने वाला व्यक्ति फिर भी गृहस्थोचितx धर्म का पालन कर सकता है, किन्तु जो मुनि-पर्याय छोड़ कर पुनः गृहस्थजीवन में प्रविष्ट होता है, शुद्ध धर्म के प्रति विश्वास और आचरण में उसकी मन्दता आ जाती है। इसीलिए यहां बताए गए १८ स्थानों में पुनर्गृहवास स्वीकार करने को नारकीय, कष्टप्रद, अपमानास्पद, क्लेशयुक्त, प्रपंची, बन्धनकारक, सावध, मायाबहुल, आतंकयुक्त आदि बताया है तथा आगे की गाथाओं में गृहवास में होने वाले परितापों की परम्परा का विशद वर्णन किया गया है। सचमुच उत्प्रव्रजित का जीवन निस्तेज, निन्द्य, अपमानित, अपकीर्तियुक्त, दुःखपूर्ण गति का अधिकारी एवं दुर्लभबोधि हो जाता है, जबकि प्रव्रजित साधक का जीवन देवलोकसम सुखद, स्वर्गसम उत्कृष्ट सुखयुक्त, तेजस्वी, यशस्वी, पूज्य, वन्द्य एवं मोक्षगामी होता है।x प्रस्तुत चूलिका में कर्मवाद के सिद्धान्त के आधार पर स्पष्ट प्रेरणा दी गई है कि कर्मबन्धन को काटने के लिए मुनिपर्याय एक उत्तम अवसर था, उसे खो कर गृहवास में स्वयंकृत कर्मों को स्वयं भोगना होगा, उसमें समभाव न रहने से पूर्वकृत कर्मों को काटने की अपेक्षा नये अशुभ कर्मों का बन्ध अधिक होता जाएगा। उन पापकर्मों को भोगे बिना तथा तपस्या से निर्वीर्य किये बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। अन्त में १५-१६वीं गाथा में कुछ चिन्तनसूत्र दिये गये हैं—नरक के अतिदीर्घकालीन दुःखों की अपेक्षा संयमजीवन में सहे जाने वाले दुःख अत्यल्प और अल्पावधिक हैं। भोग-पिपासा अशाश्वत है। ये चिन्तनसूत्र साधक को संयमीजीवन के कष्टों को सहने, भोग-पिपासा से विरक्त होने तथा
संयम में स्थिर रहने की प्रेरणा देते हैं। + 'तस्माज्ज्येष्ठाश्रमो गृही ।' . 'बंधे गिहवासे, मोक्खे परियाए । सावजे गिहवासे, अणवज्जे परियाए।' -चू. १, स्थान १२-१३ x चूलिका १ स्थान २, ३, ५, ६, ७, १० से १४ तक तथा श्लोक १ से ८ तक तथा १० से १४ तक + पत्तेयं पुण्णपावं । .....वेयइत्ता मोक्खा, नत्थि अवेयइत्ता।
-चू. १, स्थान १५, १८