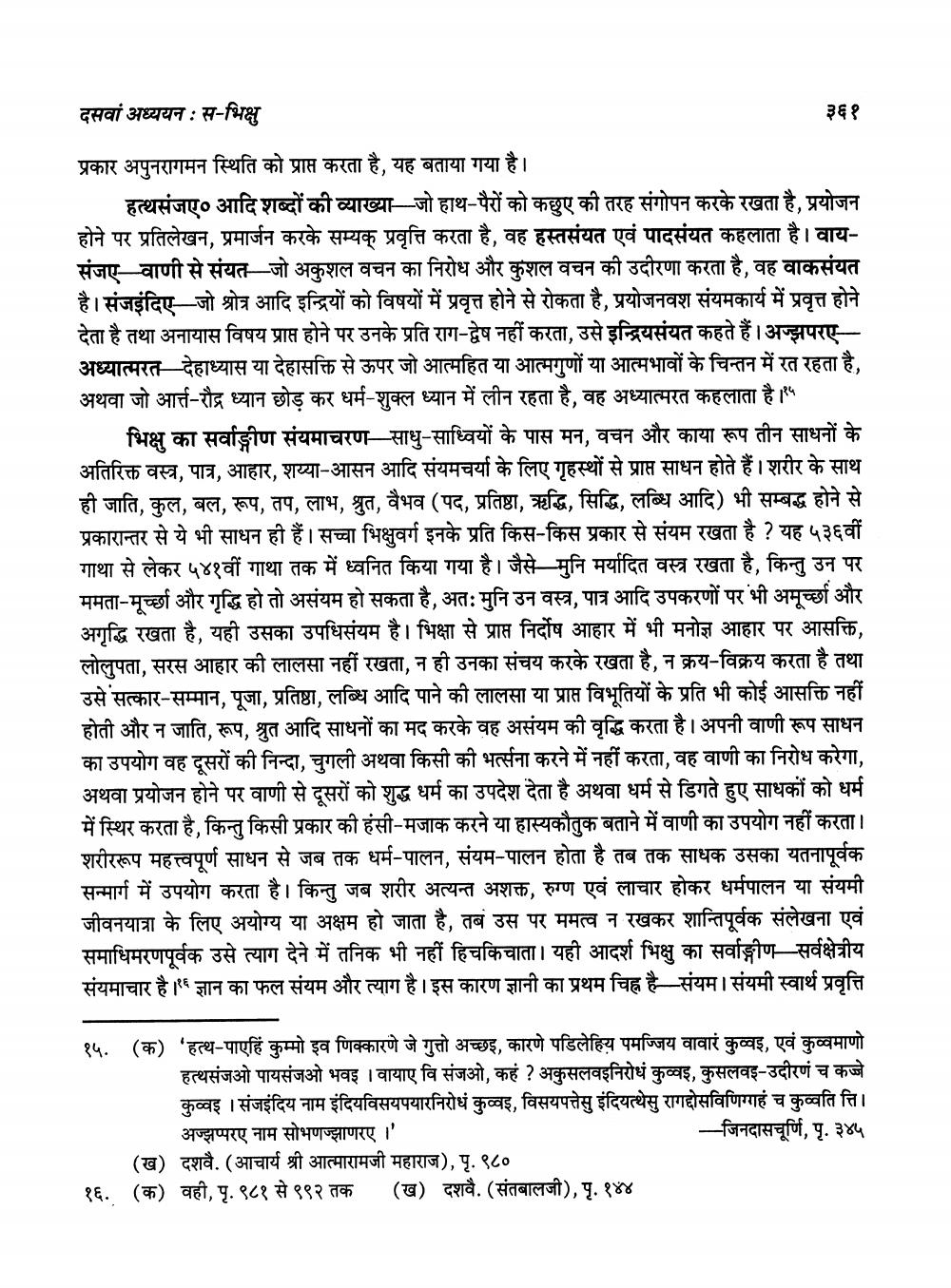________________
दसवां अध्ययन : स-भिक्षु
प्रकार अपुनरागमन स्थिति को प्राप्त करता है, यह बताया गया है।
हत्थसंजए० आदि शब्दों की व्याख्या-जो हाथ-पैरों को कछुए की तरह संगोपन करके रखता है, प्रयोजन होने पर प्रतिलेखन, प्रमार्जन करके सम्यक् प्रवृत्ति करता है, वह हस्तसंयत एवं पादसंयत कहलाता है। वायसंजवाणी से संयत — जो अकुशल वचन का निरोध और कुशल वचन की उदीरणा करता है, वह वाकसंयत है | संजइंदि— जो श्रोत्र आदि इन्द्रियों को विषयों में प्रवृत्त होने से रोकता है, प्रयोजनवश संयमकार्य में प्रवृत्त होने देता है तथा अनायास विषय प्राप्त होने पर उनके प्रति राग-द्वेष नहीं करता, उसे इन्द्रियसंयत कहते हैं। अज्झपरए— अध्यात्मरत—देहाध्यास या देहासक्ति से ऊपर जो आत्महित या आत्मगुणों या आत्मभावों के चिन्तन में रत रहता है, अथवा जो आर्त्त - रौद्र ध्यान छोड़ कर धर्म- शुक्ल ध्यान में लीन रहता है, वह अध्यात्मरत कहलाता है ।१५
भिक्षु का सर्वाङ्गीण संयमाचरण – साधु-साध्वियों के पास मन, वचन और काया रूप तीन साधनों के अतिरिक्त वस्त्र, पात्र, आहार, शय्या-आसन आदि संयमचर्या के लिए गृहस्थों से प्राप्त साधन होते हैं। शरीर के साथ ही जाति, कुल, बल, रूप, तप, लाभ, श्रुत, वैभव (पद, प्रतिष्ठा, ऋद्धि सिद्धि लब्धि आदि) भी सम्बद्ध होने से प्रकारान्तर से ये भी साधन ही हैं। सच्चा भिक्षुवर्ग इनके प्रति किस-किस प्रकार से संयम रखता है ? यह ५३६वीं गाथा से लेकर ५४१वीं गाथा तक में ध्वनित किया गया है। जैसे—मुनि मर्यादित वस्त्र रखता है, किन्तु उन पर ममता-मूर्च्छा और गृद्धि हो तो असंयम हो सकता है, अतः मुनि उन वस्त्र, पात्र आदि उपकरणों पर भी अमूर्च्छा और अगृद्धि रखता है, यही उसका उपधिसंयम है। भिक्षा से प्राप्त निर्दोष आहार में भी मनोज्ञ आहार पर आसक्ति, लोलुपता, सरस आहार की लालसा नहीं रखता, न ही उनका संचय करके रखता है, न क्रय-विक्रय करता है तथा उसे सत्कार-सम्मान, पूजा, प्रतिष्ठा, लब्धि आदि पाने की लालसा या प्राप्त विभूतियों के प्रति भी कोई आसक्ति नहीं होती और न जाति, रूप, श्रुत आदि साधनों का मद करके वह असंयम की वृद्धि करता है। अपनी वाणी रूप साधन का उपयोग वह दूसरों की निन्दा, चुगली अथवा किसी की भर्त्सना करने में नहीं करता, वह वाणी का निरोध करेगा, अथवा प्रयोजन होने पर वाणी से दूसरों को शुद्ध धर्म का उपदेश देता है अथवा धर्म से डिगते हुए साधकों को धर्म में स्थिर करता है, किन्तु किसी प्रकार की हंसी-मजाक करने या हास्यकौतुक बताने में वाणी का उपयोग नहीं करता । शरीररूप महत्त्वपूर्ण साधन से जब तक धर्म - पालन, संयम- पालन होता है तब तक साधक उसका यतनापूर्वक सन्मार्ग में उपयोग करता है। किन्तु जब शरीर अत्यन्त अशक्त, रुग्ण एवं लाचार होकर धर्मपालन या संयमी जीवनयात्रा के लिए अयोग्य या अक्षम हो जाता है, तब उस पर ममत्व न रखकर शान्तिपूर्वक संलेखना एवं समाधिमरणपूर्वक उसे त्याग देने में तनिक भी नहीं हिचकिचाता। यही आदर्श भिक्षु का सर्वाङ्गीण — सर्वक्षेत्रीय संयमाचार है । ६ ज्ञान का फल संयम और त्याग है। इस कारण ज्ञानी का प्रथम चिह्न है—संयम । संयमी स्वार्थ प्रवृत्ति
१५.
३६१
(क) 'हत्थ - पाएहिं कुम्मो इव णिक्कारणे जे गुत्तो अच्छइ, कारणे पडिलेहिय पमज्जिय वावारं कुव्वइ, एवं कुव्वमाणो हत्थसंजओ पायसंजओ भवइ । वायाए वि संजओ, कहं ? अकुसलवइनिरोधं कुव्वइ, कुसलवइ - उदीरणं च कज्जे कुव्वइ । संजइंदिय नाम इंदियविसयपयारनिरोधं कुव्वइ, विसयपत्तेसु इंदियत्थेसु रागद्दोसविणिग्गहं च कुव्वति त्ति । अज्झप्परए नाम सोभणज्झाणरए ।' — जिनदासचूर्णि, पृ. ३४५
(ख) दशवै . ( आचार्य श्री आत्मारामजी महाराज), पृ. ९८०
१६. (क) वही, पृ. ९८१ से ९९२ तक (ख) दशवै. (संतबालजी), पृ. १४४