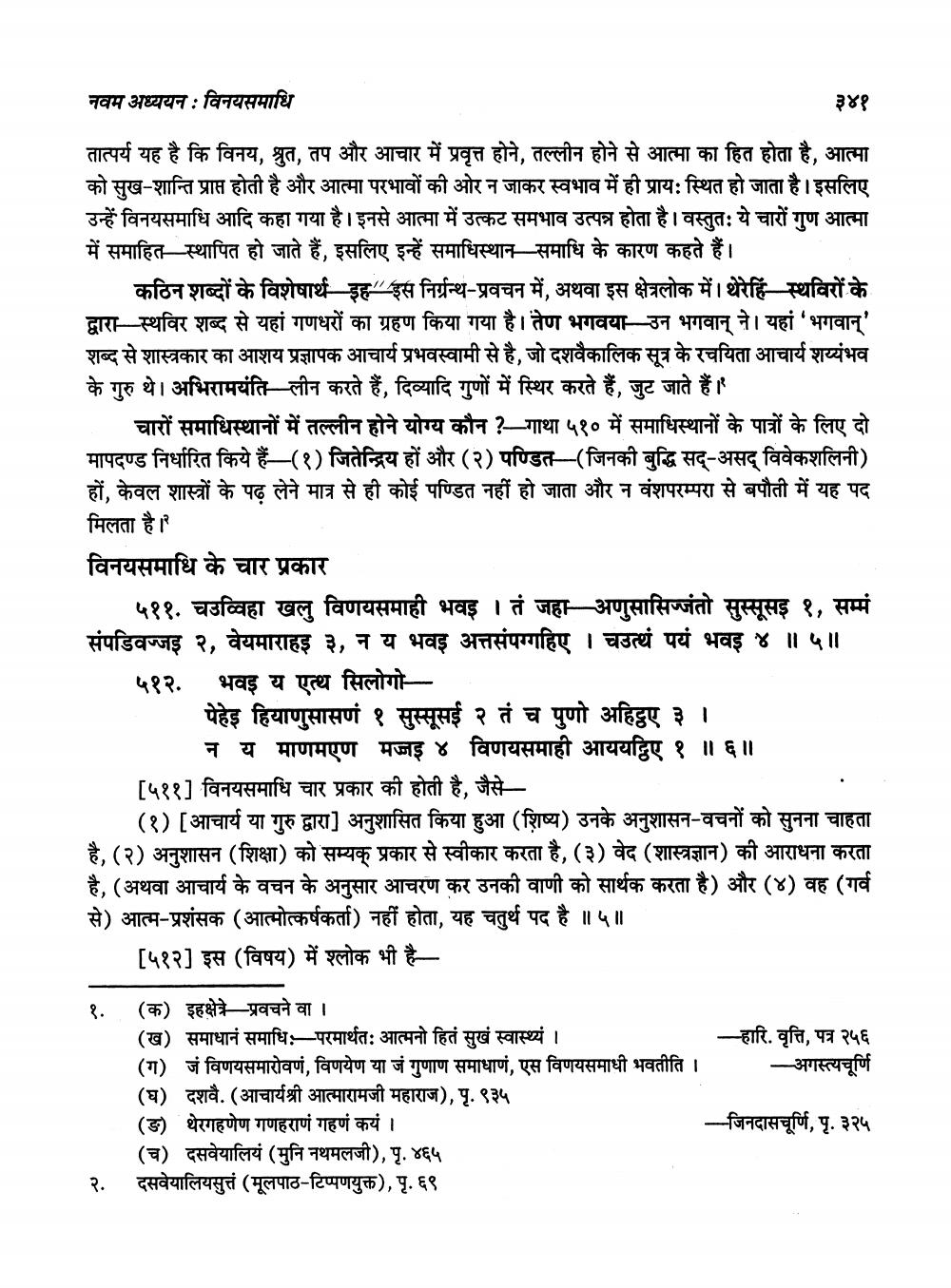________________
नवम अध्ययन : विनयसमाधि
३४१
तात्पर्य यह है कि विनय, श्रुत, तप और आचार में प्रवृत्त होने, तल्लीन होने से आत्मा का हित होता है, आत्मा को सुख-शान्ति प्राप्त होती है और आत्मा परभावों की ओर न जाकर स्वभाव में ही प्रायः स्थित हो जाता है। इसलिए उन्हें विनयसमाधि आदि कहा गया है। इनसे आत्मा में उत्कट समभाव उत्पन्न होता है। वस्तुतः ये चारों गुण आत्मा में समाहित –—–— स्थापित हो जाते हैं, इसलिए इन्हें समाधिस्थान — समाधि के कारण कहते हैं।
कठिन शब्दों के विशेषार्थ इह इस निर्ग्रन्थ- प्रवचन में, अथवा इस क्षेत्रलोक में । थेरेहिं— स्थविरों के द्वारा—स्थविर शब्द से यहां गणधरों का ग्रहण किया गया है। तेण भगवया—उन भगवान् ने । यहां 'भगवान्' शब्द से शास्त्रकार का आशय प्रज्ञापक आचार्य प्रभवस्वामी से है, जो दशवैकालिक सूत्र के रचयिता आचार्य शय्यंभव के गुरु थे। अभिरामयंति—लीन करते हैं, दिव्यादि गुणों में स्थिर करते हैं, जुट जाते हैं ।
चारों समाधिस्थानों में तल्लीन होने योग्य कौन ? – गाथा ५१० में समाधिस्थानों के पात्रों के लिए दो मापदण्ड निर्धारित किये हैं- (१) जितेन्द्रिय हों और (२) पण्डित - (जिनकी बुद्धि सद्-असद् विवेकशलिनी) हों, केवल शास्त्रों के पढ़ लेने मात्र से ही कोई पण्डित नहीं हो जाता और न वंशपरम्परा से बपौती में यह पद मिलता है।
विनयसमाधि के चार प्रकार
५११. चउव्विहा खलु विणयसमाही भवइ । तं जहा— अणुसासिज्जंतो सुस्सूसइ १, सम्मं संपडिवज्जइ २, वेयमाराहइ ३, न य भवइ अत्तसंपग्गहिए । चउत्थं पयं भवइ ४ ॥ ५ ॥
५१२.
[५११] विनयसमाधि चार प्रकार की होती है, जैसे
(१) [आचार्य या गुरु द्वारा ] अनुशासित किया हुआ (शिष्य) उनके अनुशासन - वचनों को सुनना चाहता है, (२) अनुशासन (शिक्षा) को सम्यक् प्रकार से स्वीकार करता है, (३) वेद (शास्त्रज्ञान) की आराधना करता है, (अथवा आचार्य के वचन के अनुसार आचरण कर उनकी वाणी को सार्थक करता है) और (४) वह (गर्व से) आत्म-प्रशंसक (आत्मोत्कर्षकर्ता) नहीं होता, यह चतुर्थ पद है ॥ ५ ॥
[५१२] इस (विषय) में श्लोक भी है—
१.
भवइ य एत्थ सिलोगो—
पेइ हियाणुसासणं १ सुस्सूसई २ तं च पुणो अट्ठिए ३ ।
न य माणमएण मज्जइ ४ विणयसमाही आययद्विए १ ॥ ६ ॥
२.
(क) इहक्षेत्रे प्रवचने वा ।
(ख) समाधानं समाधिः — परमार्थतः आत्मनो हितं सुखं स्वास्थ्यं ।
(ग) जं विणयसमारोवणं, विणयेण या जं गुणाण समाधाणं, एस विणयसमाधी भवतीति ।
(घ) दशवै. ( आचार्य श्री आत्मारामजी महाराज), पृ. ९३५
(ङ) थेरगहणेण गणहराणं गहणं कयं ।
(च) दसवेयालियं (मुनि नथमलजी), पृ. ४६५ दसवेयालियसुत्तं (मूलपाठ - टिप्पणयुक्त), पृ. ६९
— हारि. वृत्ति, पत्र २५६ — अगस्त्यचूर्णि
—जिनदासचूर्णि, पृ. ३२५