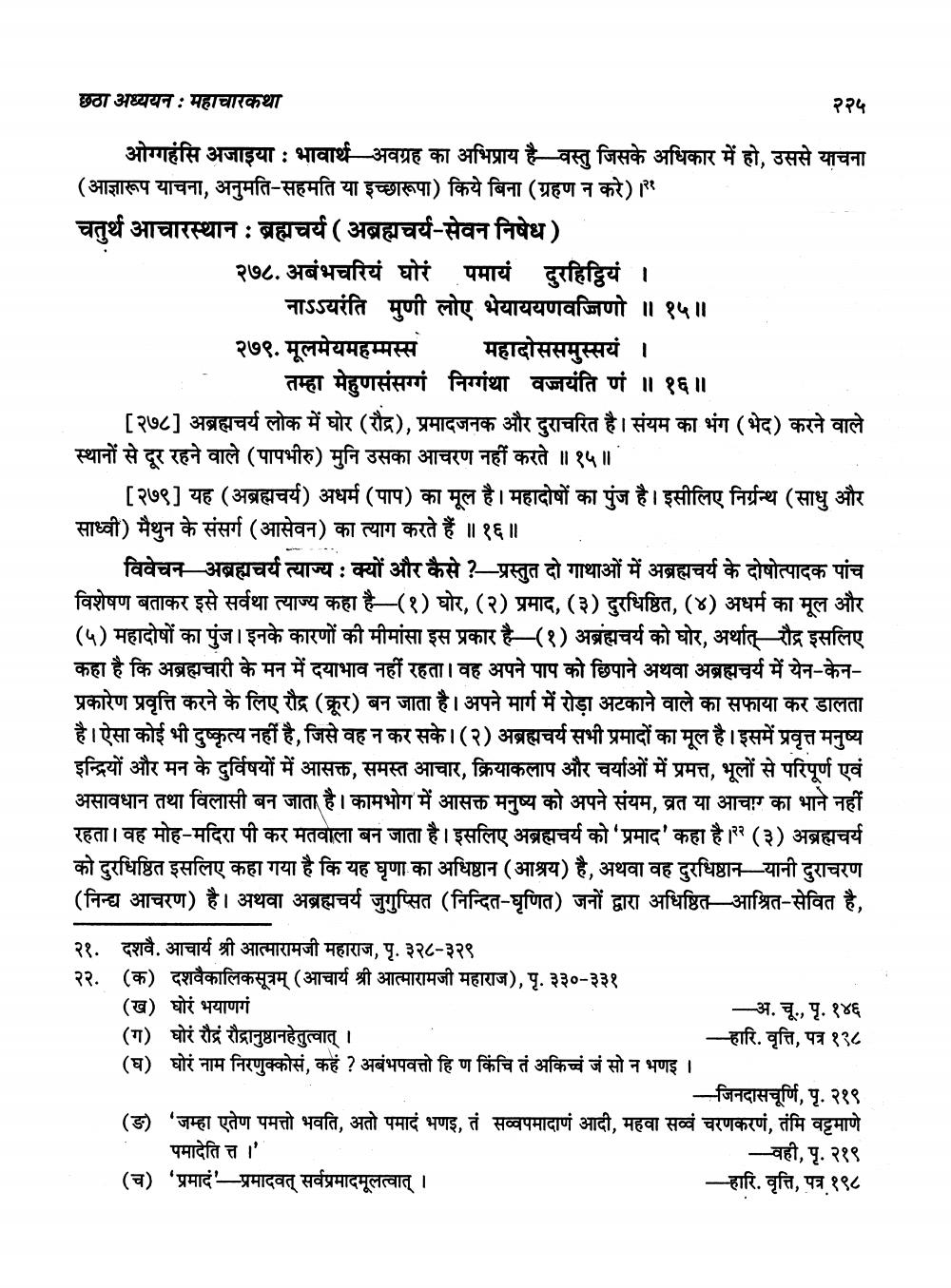________________
छठा अध्ययन: महाचारकथा
२२५
ओग्गहंसि अजाइया : भावार्थ —अवग्रह का अभिप्राय है वस्तु जिसके अधिकार में हो, उससे याचना (आज्ञारूप याचना, अनुमति-सहमति या इच्छारूपा) किये बिना (ग्रहण न करे)। चतुर्थ आचारस्थान : ब्रह्मचर्य (अब्रह्मचर्य-सेवन निषेध)
२७८. अबंभचरियं घोरं पमायं दुरहिट्ठियं ।
नाऽऽयरंति मुणी लोए भेयाययणवजिणो ॥ १५॥ २७९. मूलमेयमहम्मस्स महादोससमुस्सयं ।
तम्हा मेहुणसंसग्गं निग्गंथा वजयंति णं ॥ १६॥ [२७८] अब्रह्मचर्य लोक में घोर (रौद्र), प्रमादजनक और दुराचरित है। संयम का भंग (भेद) करने वाले स्थानों से दूर रहने वाले (पापभीरु) मुनि उसका आचरण नहीं करते ॥ १५॥
[२७९] यह (अब्रह्मचर्य) अधर्म (पाप) का मूल है। महादोषों का पुंज है। इसीलिए निर्ग्रन्थ (साधु और साध्वी) मैथुन के संसर्ग (आसेवन) का त्याग करते हैं ॥१६॥
विवेचन अब्रह्मचर्य त्याज्य : क्यों और कैसे ? प्रस्तुत दो गाथाओं में अब्रह्मचर्य के दोषोत्पादक पांच विशेषण बताकर इसे सर्वथा त्याज्य कहा है—(१) घोर, (२) प्रमाद, (३) दुरधिष्ठित, (४) अधर्म का मूल और (५) महादोषों का पुंज। इनके कारणों की मीमांसा इस प्रकार है—(१) अब्रह्मचर्य को घोर, अर्थात्रौद्र इसलिए कहा है कि अब्रह्मचारी के मन में दयाभाव नहीं रहता। वह अपने पाप को छिपाने अथवा अब्रह्मचर्य में येन-केनप्रकारेण प्रवृत्ति करने के लिए रौद्र (क्रूर) बन जाता है। अपने मार्ग में रोड़ा अटकाने वाले का सफाया कर डालता है। ऐसा कोई भी दुष्कृत्य नहीं है, जिसे वह न कर सके। (२) अब्रह्मचर्य सभी प्रमादों का मूल है। इसमें प्रवृत्त मनुष्य इन्द्रियों और मन के दुर्विषयों में आसक्त, समस्त आचार, क्रियाकलाप और चर्याओं में प्रमत्त, भूलों से परिपूर्ण एवं असावधान तथा विलासी बन जाता है। कामभोग में आसक्त मनुष्य को अपने संयम, व्रत या आचार का भाने नहीं रहता। वह मोह-मदिरा पी कर मतवाला बन जाता है। इसलिए अब्रह्मचर्य को 'प्रमाद' कहा है।२२ (३) अब्रह्मचर्य को दुरधिष्ठित इसलिए कहा गया है कि यह घृणा का अधिष्ठान (आश्रय) है, अथवा वह दुरधिष्ठान यानी दुराचरण (निन्ध आचरण) है। अथवा अब्रह्मचर्य जुगुप्सित (निन्दित-घृणित) जनों द्वारा अधिष्ठित-आश्रित-सेवित है, २१. दशवै. आचार्य श्री आत्मारामजी महाराज, पृ. ३२८-३२९ २२. (क) दशवैकालिकसूत्रम् (आचार्य श्री आत्मारामजी महाराज), पृ. ३३०-३३१ (ख) घोरं भयाणगं
-अ.चू., पृ. १४६ (ग) घोरं रौद्रं रौद्रानुष्ठानहेतुत्वात् ।
-हारि. वृत्ति, पत्र १९८ (घ) घोरं नाम निरणुक्कोसं, कहं? अबंभपवत्तो हि ण किंचि तं अकिच्चं जं सो न भणइ ।
-जिनदासचूर्णि, पृ. २१९ (ङ) 'जम्हा एतेण पमत्तो भवति, अतो पमादं भणइ, तं सव्वपमादाणं आदी, महवा सव्वं चरणकरणं, तंमि वट्टमाणे पमादेति त ।'
-वही, पृ. २१९ (च) 'प्रमादं'—प्रमादवत् सर्वप्रमादमूलत्वात् ।
–हारि. वृत्ति, पत्र १९८