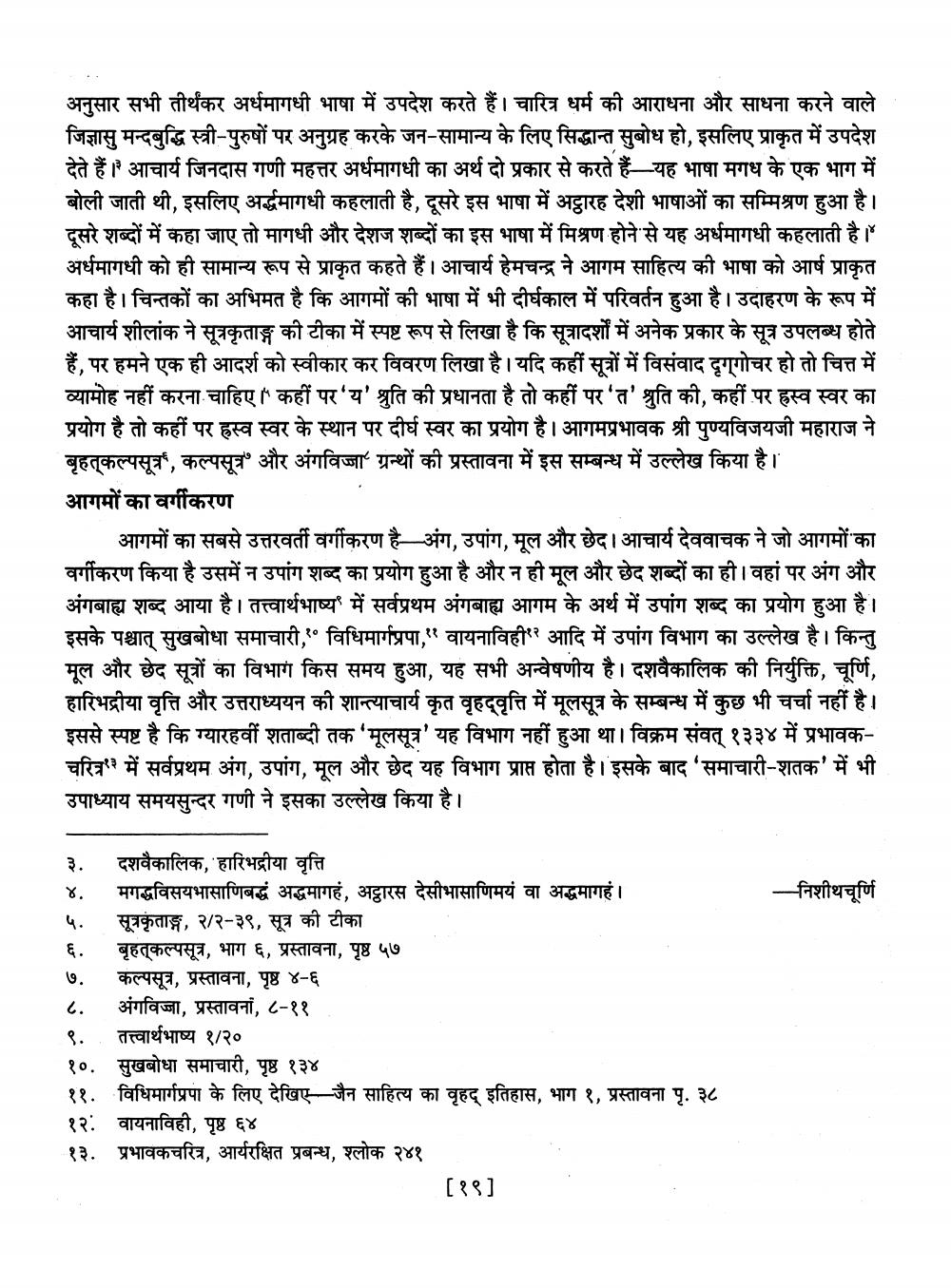________________
अनुसार सभी तीर्थंकर अर्धमागधी भाषा में उपदेश करते हैं। चारित्र धर्म की आराधना और साधना करने वाले जिज्ञासु मन्दबुद्धि स्त्री-पुरुषों पर अनुग्रह करके जन-सामान्य के लिए सिद्धान्त सुबोध हो, इसलिए प्राकृत में उपदेश देते हैं। आचार्य जिनदास गणी महत्तर अर्धमागधी का अर्थ दो प्रकार से करते हैं—यह भाषा मगध के एक भाग में बोली जाती थी, इसलिए अर्द्धमागधी कहलाती है, दूसरे इस भाषा में अट्ठारह देशी भाषाओं का सम्मिश्रण हुआ है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मागधी और देशज शब्दों का इस भाषा में मिश्रण होने से यह अर्धमागधी कहलाती है। अर्धमागधी को ही सामान्य रूप से प्राकत कहते हैं। आचार्य हेमचन्द्र ने आगम साहित्य की भाषा को आर्ष प्राकत कहा है। चिन्तकों का अभिमत है कि आगमों की भाषा में भी दीर्घकाल में परिवर्तन हुआ है। उदाहरण के रूप में आचार्य शीलांक ने सूत्रकृताङ्ग की टीका में स्पष्ट रूप से लिखा है कि सूत्रादर्शों में अनेक प्रकार के सूत्र उपलब्ध होते हैं, पर हमने एक ही आदर्श को स्वीकार कर विवरण लिखा है। यदि कहीं सूत्रों में विसंवाद दृग्गोचर हो तो चित्त में व्यामोह नहीं करना चाहिए। कहीं पर 'य' श्रुति की प्रधानता है तो कहीं पर 'त' श्रुति की, कहीं पर ह्रस्व स्वर का प्रयोग है तो कहीं पर ह्रस्व स्वर के स्थान पर दीर्घ स्वर का प्रयोग है। आगमप्रभावक श्री पुण्यविजयजी महाराज ने बृहत्कल्पसूत्र', कल्पसूत्र और अंगविजा ग्रन्थों की प्रस्तावना में इस सम्बन्ध में उल्लेख किया है। आगमों का वर्गीकरण
आगमों का सबसे उत्तरवर्ती वर्गीकरण है—अंग, उपांग, मूल और छेद । आचार्य देववाचक ने जो आगमों का वर्गीकरण किया है उसमें न उपांग शब्द का प्रयोग हुआ है और न ही मूल और छेद शब्दों का ही। वहां पर अंग और अंगबाह्य शब्द आया है। तत्त्वार्थभाष्य में सर्वप्रथम अंगबाह्य आगम के अर्थ में उपांग शब्द का प्रयोग हुआ है। इसके पश्चात् सुखबोधा समाचारी, विधिमार्गप्रपा,१ वायनाविही१२ आदि में उपांग विभाग का उल्लेख है। किन्तु मूल और छेद सूत्रों का विभाग किस समय हुआ, यह सभी अन्वेषणीय है। दशवैकालिक की नियुक्ति, चूर्णि, हारिभद्रीया वृत्ति और उत्तराध्ययन की शान्त्याचार्य कृत वृहद्वृत्ति में मूलसूत्र के सम्बन्ध में कुछ भी चर्चा नहीं है। इससे स्पष्ट है कि ग्यारहवीं शताब्दी तक 'मूलसूत्र' यह विभाग नहीं हुआ था। विक्रम संवत् १३३४ में प्रभावकचरित्र में सर्वप्रथम अंग, उपांग, मूल और छेद यह विभाग प्राप्त होता है। इसके बाद 'समाचारी-शतक' में भी उपाध्याय समयसुन्दर गणी ने इसका उल्लेख किया है।
-निशीथचूर्णि
३. दशवैकालिक, हारिभद्रीया वृत्ति
मगद्धविसयभासाणिबद्धं अद्धमागहं, अट्ठारस देसीभासाणिमयं वा अद्धमागहं। ५. सूत्रकृताङ्ग, २/२-३९, सूत्र की टीका
बृहत्कल्पसूत्र, भाग ६, प्रस्तावना, पृष्ठ ५७
कल्पसूत्र, प्रस्तावना, पृष्ठ ४-६ ८. अंगविज्जा, प्रस्तावना, ८-११ .
तत्त्वार्थभाष्य १/२० १०. सुखबोधा समाचारी, पृष्ठ १३४ ११. विधिमार्गप्रपा के लिए देखिए-जैन साहित्य का वृहद् इतिहास, भाग १, प्रस्तावना पृ. ३८ १२. वायनाविही, पृष्ठ ६४ १३. प्रभावकचरित्र, आर्यरक्षित प्रबन्ध, श्लोक २४१
[१९]