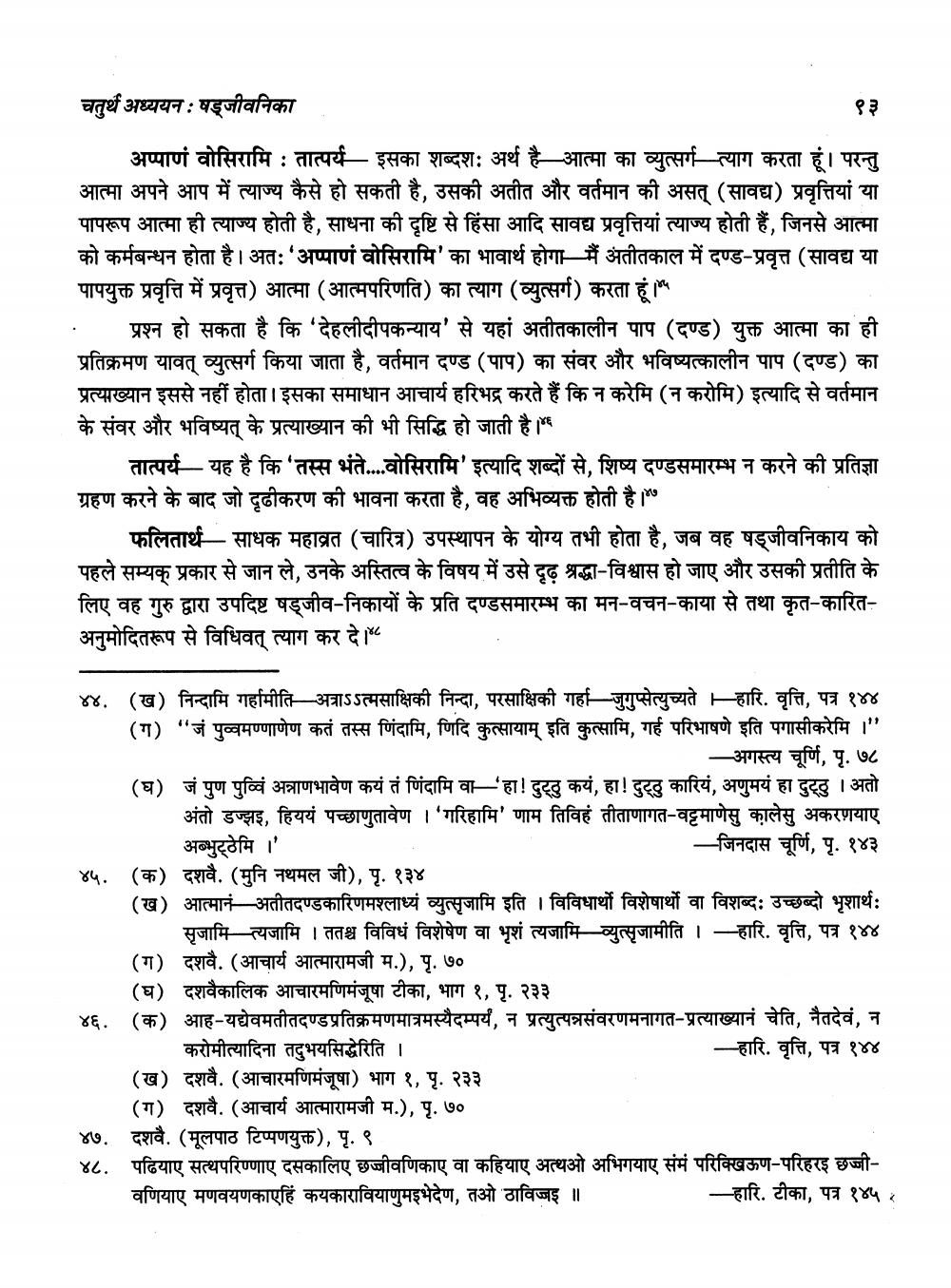________________
चतुर्थ अध्ययन : षड्जीवनिका
९३
अप्पाणं वोसिरामि : तात्पर्य इसका शब्दशः अर्थ है— आत्मा का व्युत्सर्ग— त्याग करता हूं । परन्तु आत्मा अपने आप में त्याज्य कैसे हो सकती है, उसकी अतीत और वर्तमान की असत् (सावद्य) प्रवृत्तियां या पापरूप आत्मा ही त्याज्य होती है, साधना की दृष्टि से हिंसा आदि सावध प्रवृत्तियां त्याज्य होती हैं, जिनसे आत्मा को कर्मबन्धन होता है। अतः 'अप्पाणं वोसिरामि' का भावार्थ होगा— मैं अतीतकाल में दण्ड - प्रवृत्त (सावद्य या पापयुक्त प्रवृत्ति में प्रवृत्त) आत्मा (आत्मपरिणति) का त्याग ( व्युत्सर्ग) करता हूं ।५
प्रश्न हो सकता है कि 'देहलीदीपकन्याय' से यहां अतीतकालीन पाप (दण्ड) युक्त आत्मा का ही प्रतिक्रमण यावत् व्युत्सर्ग किया जाता है, वर्तमान दण्ड (पाप) का संवर और भविष्यत्कालीन पाप (दण्ड) का प्रत्याख्यान इससे नहीं होता। इसका समाधान आचार्य हरिभद्र करते हैं कि न करेमि ( न करोमि ) इत्यादि से वर्तमान के संवर और भविष्यत् के प्रत्याख्यान की भी सिद्धि हो जाती है । ६
तात्पर्य यह है कि 'तस्स भंते....वोसिरामि' इत्यादि शब्दों से, शिष्य दण्डसमारम्भ न करने की प्रतिज्ञा ग्रहण करने के बाद जो दृढीकरण की भावना करता है, वह अभिव्यक्त होती है ।४७
फलितार्थ—–—–— साधक महाव्रत ( चारित्र) उपस्थापन के योग्य तभी होता है, जब वह षड्जीवनिकाय को पहले सम्यक् प्रकार से जान ले, उनके अस्तित्व के विषय में उसे दृढ़ श्रद्धा-विश्वास हो जाए और उसकी प्रतीति के लिए वह गुरु द्वारा उपदिष्ट षड्जीव - निकायों के प्रति दण्डसमारम्भ का मन-वचन-काया से तथा कृत- कारितअनुमोदितरूप से विधिवत् त्याग कर दे।
४४.
४५.
४६.
(ख) निन्दामि गर्हामीति — अत्राऽऽत्मसाक्षिकी निन्दा, परसाक्षिकी गर्हा— जुगुप्सेत्युच्यते । —हारि वृत्ति, पत्र १४४ (ग) "जं पुव्वमण्णाणेण कतं तस्स णिंदामि, णिदि कुत्सायाम् इति कुत्सामि, गर्ह परिभाषणे इति पगासीकरेमि । " — अगस्त्य चूर्णि, पृ. ७८
(घ)
जं पुण पुव्विं अन्नाणभावेण कयं तं जिंदामि वा—' हा ! दुट्टु कयं, हा ! दुट्टु कारियं, अणुमयं हा दुट्टु । अतो अंतो डज्झइ, हिययं पच्छाणुतावेण । 'गरिहामि' णाम तिविहं तीताणागत - वट्टमाणेसु कालेसु अकरणयाए अब्भुट्ठेमि ।' – जिनदास चूर्णि, पृ. १४३
(क) दशवै. ( मुनि नथमल जी), पृ. १३४
(ख) आत्मानं - अतीतदण्डकारिणमश्लाध्यं व्युत्सृजामि इति । विविधार्थो विशेषार्थो वा विशब्दः उच्छब्दो भृशार्थः सृजामित्यजामि । ततश्च विविधं विशेषेण वा भृशं त्यजामि — व्युत्सृजामीति । —हारि वृत्ति, पत्र १४४ (ग) दशवै. (आचार्य आत्मारामजी म.), पृ. ७०
(घ) दशवैकालिक आचारमणिमंजूषा टीका, भाग १, पृ. २३३
(क) आह-यद्येवमतीतदण्डप्रतिक्रमणमात्रमस्यैदम्पर्यं न प्रत्युत्पन्नसंवरणमनागत- प्रत्याख्यानं चेति, नैतदेवं, न करोमीत्यादिना तदुभयसिद्धेरिति । — हारि. वृत्ति, पत्र १४४
(ख) दशवै. ( आचारमणिमंजूषा ) भाग १, पृ. २३३
(ग) दशवै. (आचार्य आत्मारामजी म.), पृ. ७०
४७. दशवै. ( मूलपाठ टिप्पणयुक्त), पृ. ९
४८. पढियाए सत्थपरिण्णाए दसकालिए छज्जीवणिकाए वा कहियाए अत्थओ अभिगयाए संमं परिक्खिऊण-परिहरइ छज्जीवणिया मणवयणकाएहिं कयकारावियाणुमइभेदेण, तओ ठाविज्जइ ॥
— हारि. टीका, पत्र १४५ :