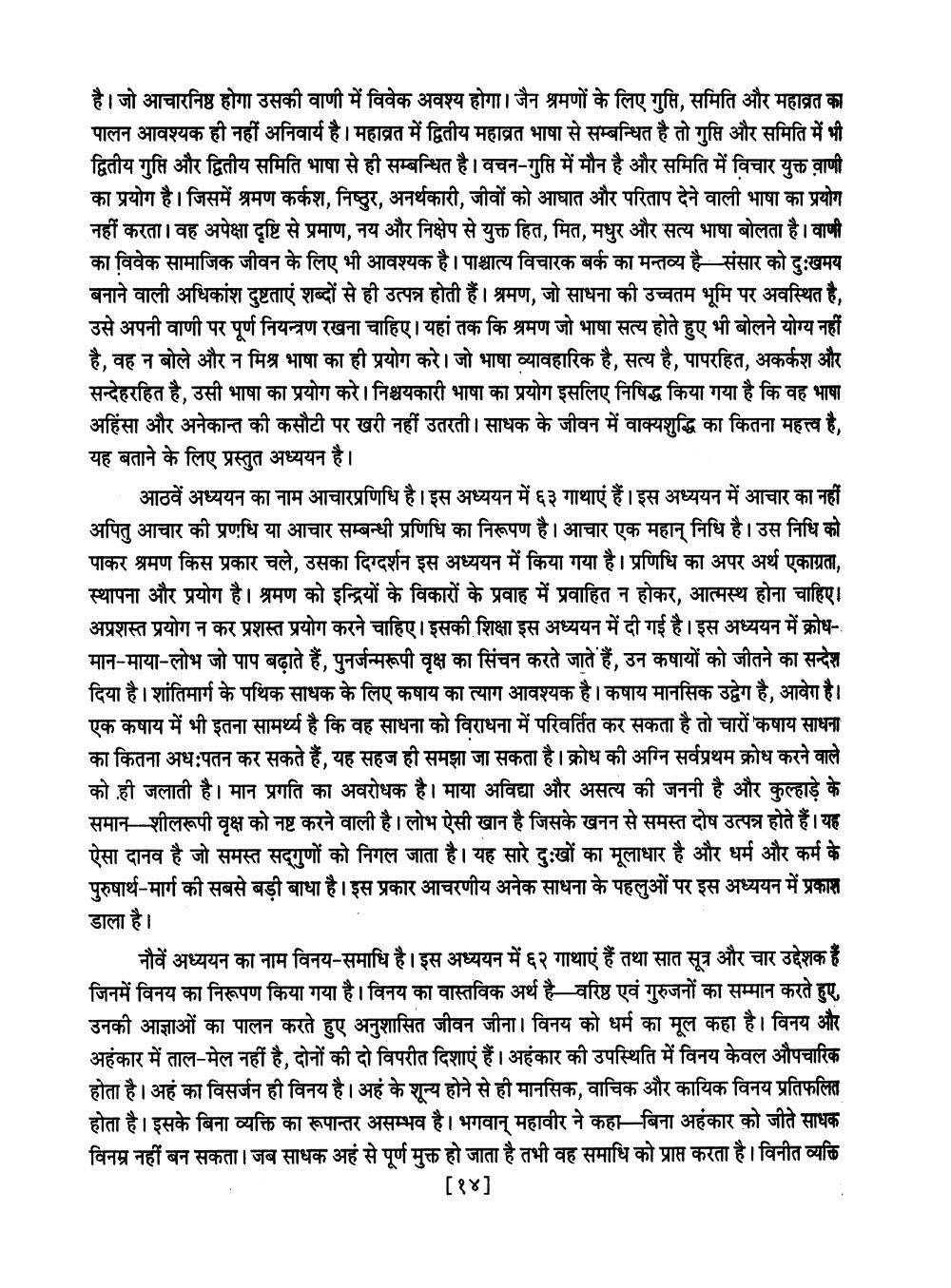________________
है। जो आचारनिष्ठ होगा उसकी वाणी में विवेक अवश्य होगा। जैन श्रमणों के लिए गुप्ति, समिति और महाव्रत का पालन आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। महाव्रत में द्वितीय महाव्रत भाषा से सम्बन्धित है तो गुप्ति और समिति में भी द्वितीय गुप्ति और द्वितीय समिति भाषा से ही सम्बन्धित है। वचन-गुप्ति में मौन है और समिति में विचार युक्त वाणी का प्रयोग है। जिसमें श्रमण कर्कश, निष्ठुर, अनर्थकारी, जीवों को आघात और परिताप देने वाली भाषा का प्रयोग नहीं करता। वह अपेक्षा दृष्टि से प्रमाण, नय और निक्षेप से युक्त हित, मित, मधुर और सत्य भाषा बोलता है। वाणी का विवेक सामाजिक जीवन के लिए भी आवश्यक है। पाश्चात्य विचारक बर्क का मन्तव्य है संसार को दुःखमय बनाने वाली अधिकांश दुष्टताएं शब्दों से ही उत्पन्न होती हैं। श्रमण, जो साधना की उच्चतम भूमि पर अवस्थित है, उसे अपनी वाणी पर पूर्ण नियन्त्रण रखना चाहिए। यहां तक कि श्रमण जो भाषा सत्य होते हए भी बोलने योग्य नहीं है, वह न बोले और न मिश्र भाषा का ही प्रयोग करे। जो भाषा व्यावहारिक है, सत्य है, पापरहित, अकर्कश और सन्देहरहित है, उसी भाषा का प्रयोग करे। निश्चयकारी भाषा का प्रयोग इसलिए निषिद्ध किया गया है कि वह भाषा अहिंसा और अनेकान्त की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। साधक के जीवन में वाक्यशुद्धि का कितना महत्त्व है, यह बताने के लिए प्रस्तुत अध्ययन है।
आठवें अध्ययन का नाम आचारप्रणिधि है। इस अध्ययन में ६३ गाथाएं हैं। इस अध्ययन में आचार का नहीं अपितु आचार की प्रणधि या आचार सम्बन्धी प्रणिधि का निरूपण है। आचार एक महान् निधि है। उस निधि को पाकर श्रमण किस प्रकार चले, उसका दिग्दर्शन इस अध्ययन में किया गया है। प्रणिधि का अपर अर्थ एकाग्रता, स्थापना और प्रयोग है। श्रमण को इन्द्रियों के विकारों के प्रवाह में प्रवाहित न होकर, आत्मस्थ होना चाहिए। अप्रशस्त प्रयोग न कर प्रशस्त प्रयोग करने चाहिए। इसकी शिक्षा इस अध्ययन में दी गई है। इस अध्ययन में क्रोधमान-माया-लोभ जो पाप बढ़ाते हैं, पुनर्जन्मरूपी वृक्ष का सिंचन करते जाते हैं, उन कषायों को जीतने का सन्देश
है। शांतिमार्ग के पथिक साधक के लिए कषाय का त्याग आवश्यक है। कषाय मानसिक उद्वेग है. आवेग है। एक कषाय में भी इतना सामर्थ्य है कि वह साधना को विराधना में परिवर्तित कर सकता है तो चारों कषाय साधना का कितना अधःपतन कर सकते हैं, यह सहज ही समझा जा सकता है। क्रोध की अग्नि सर्वप्रथम क्रोध करने वाले को ही जलाती है। मान प्रगति का अवरोधक है। माया अविद्या और असत्य की जननी है और कुल्हाड़े के समान–शीलरूपी वृक्ष को नष्ट करने वाली है। लोभ ऐसी खान है जिसके खनन से समस्त दोष उत्पन्न होते हैं। यह ऐसा दानव है जो समस्त सद्गुणों को निगल जाता है। यह सारे दुःखों का मूलाधार है और धर्म और कर्म के पुरुषार्थ-मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। इस प्रकार आचरणीय अनेक साधना के पहलुओं पर इस अध्ययन में प्रकाश डाला है।
नौवें अध्ययन का नाम विनय-समाधि है। इस अध्ययन में ६२ गाथाएं हैं तथा सात सूत्र और चार उद्देशक हैं जिनमें विनय का निरूपण किया गया है। विनय का वास्तविक अर्थ है वरिष्ठ एवं गुरुजनों का सम्मान करते हुए, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए अनुशासित जीवन जीना। विनय को धर्म का मूल कहा है। विनय और अहंकार में ताल-मेल नहीं है, दोनों की दो विपरीत दिशाएं हैं। अहंकार की उपस्थिति में विनय केवल औपचारिक होता है। अहं का विसर्जन ही विनय है। अहं के शून्य होने से ही मानसिक, वाचिक और कायिक विनय प्रतिफलित होता है। इसके बिना व्यक्ति का रूपान्तर असम्भव है। भगवान् महावीर ने कहा—बिना अहंकार को जीते साधक विनम्र नहीं बन सकता। जब साधक अहं से पूर्ण मुक्त हो जाता है तभी वह समाधि को प्राप्त करता है। विनीत व्यक्ति
[१४]