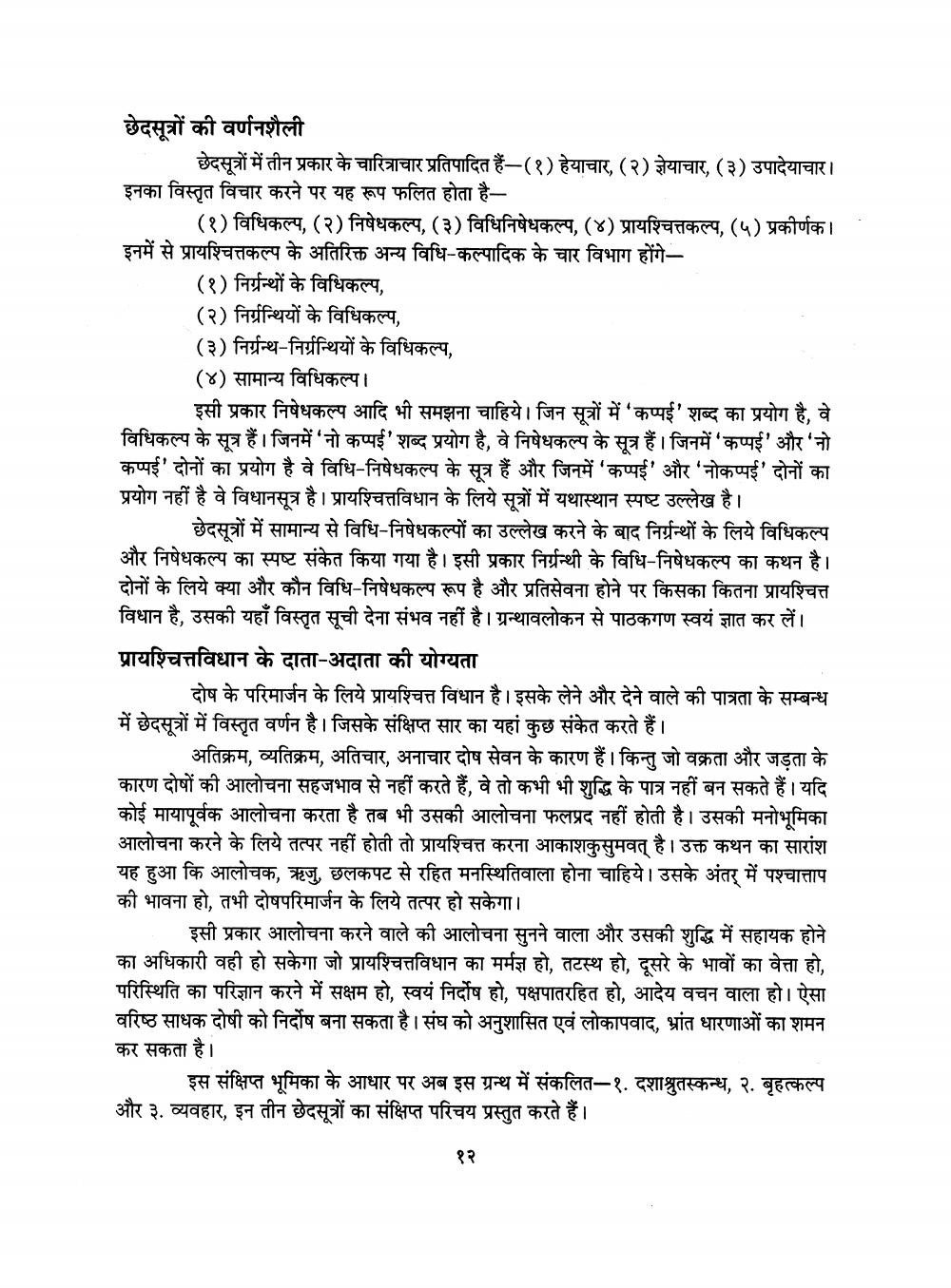________________
छेदसूत्रों की वर्णनशैली
छेदसूत्रों में तीन प्रकार के चारित्राचार प्रतिपादित हैं - (१) हेयाचार, (२) ज्ञेयाचार, (३) उपादेयाचार । इनका विस्तृत विचार करने पर यह रूप फलित होता है
(१) विधिकल्प, (२) निषेधकल्प, (३) विधिनिषेधकल्प, (४) प्रायश्चित्तकल्प, (५) प्रकीर्णक । इनमें से प्रायश्चित्तकल्प के अतिरिक्त अन्य विधि-कल्पादिक के चार विभाग होंगे
(१) निर्ग्रन्थों के विधिकल्प,
(२) निर्ग्रन्थियों के विधिकल्प,
(३) निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों के विधिकल्प,
(४) सामान्य विधिकल्प |
इसी प्रकार निषेधकल्प आदि भी समझना चाहिये। जिन सूत्रों में 'कप्पई' शब्द का प्रयोग है, वे विधिकल्प के सूत्र हैं। जिनमें 'नो कप्पई' शब्द प्रयोग है, वे निषेधकल्प के सूत्र हैं। जिनमें 'कप्पई' और 'नो कप्पई' दोनों का प्रयोग है वे विधि-निषेधकल्प के सूत्र हैं और जिनमें 'कप्पई' और 'नोकप्पई' दोनों का प्रयोग नहीं है वे विधानसूत्र है । प्रायश्चित्तविधान के लिये सूत्रों में यथास्थान स्पष्ट उल्लेख है।
छेदसूत्रों में सामान्य से विधि-निषेधकल्पों का उल्लेख करने के बाद निर्ग्रन्थों के लिये विधिकल्प और निषेधकल्प का स्पष्ट संकेत किया गया है। इसी प्रकार निर्ग्रन्थी के विधि - निषेधकल्प का कथन है । दोनों के लिये क्या और कौन विधि - निषेधकल्प रूप है और प्रतिसेवना होने पर किसका कितना प्रायश्चित्त विधान है, उसकी यहाँ विस्तृत सूची देना संभव नहीं है। ग्रन्थावलोकन से पाठकगण स्वयं ज्ञात कर लें । प्रायश्चित्तविधान के दाता अदाता की योग्यता
दोष के परिमार्जन के लिये प्रायश्चित्त विधान है। इसके लेने और देने वाले की पात्रता के सम्बन्ध में छेदसूत्रों में विस्तृत वर्णन है। जिसके संक्षिप्त सार का यहां कुछ संकेत करते हैं।
अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार दोष सेवन के कारण हैं। किन्तु जो वक्रता और जड़ता के कारण दोषों की आलोचना सहजभाव से नहीं करते हैं, वे तो कभी भी शुद्धि के पात्र नहीं बन सकते हैं। यदि कोई मायापूर्वक आलोचना करता है तब भी उसकी आलोचना फलप्रद नहीं होती है। उसकी मनोभूमिका आलोचना करने के लिये तत्पर नहीं होती तो प्रायश्चित्त करना आकाशकुसुमवत् है। उक्त कथन का सारांश यह हुआ कि आलोचक, ऋजु, छलकपट से रहित मनस्थितिवाला होना चाहिये। उसके अंतर् में पश्चात्ताप की भावना हो, तभी दोषपरिमार्जन के लिये तत्पर हो सकेगा।
इसी प्रकार आलोचना करने वाले की आलोचना सुनने वाला और उसकी शुद्धि में सहायक होने का अधिकारी वही हो सकेगा जो प्रायश्चित्तविधान का मर्मज्ञ हो, तटस्थ हो, दूसरे के भावों का वेत्ता हो, परिस्थिति का परिज्ञान करने में सक्षम हो, स्वयं निर्दोष हो, पक्षपातरहित हो, आदेय वचन वाला हो। ऐसा वरिष्ठ साधक दोषी को निर्दोष बना सकता है। संघ को अनुशासित एवं लोकापवाद, भ्रांत धारणाओं का शमन कर सकता है।
इस संक्षिप्त भूमिका के आधार पर अब इस ग्रन्थ में संकलित - १. दशाश्रुतस्कन्ध, २. बृहत्कल्प और ३. व्यवहार, इन तीन छेदसूत्रों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करते हैं ।
१२