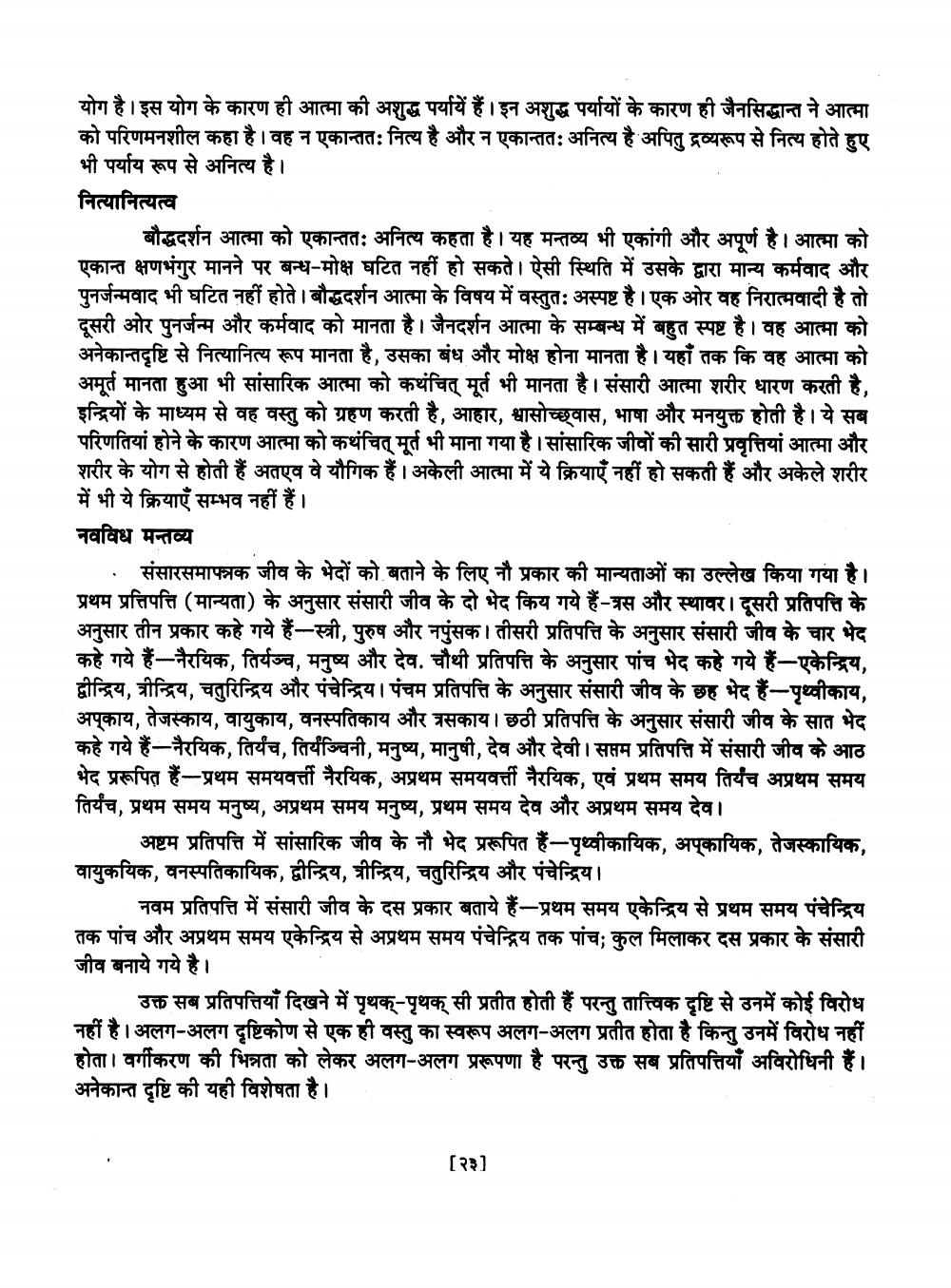________________
योग है। इस योग के कारण ही आत्मा की अशुद्ध पर्यायें हैं। इन अशुद्ध पर्यायों के कारण ही जैनसिद्धान्त ने आत्मा को परिणमनशील कहा है। वह न एकान्ततः नित्य है और न एकान्ततः अनित्य है अपितु द्रव्यरूप से नित्य होते हुए भी पर्याय रूप से अनित्य है। नित्यानित्यत्व
बौद्धदर्शन आत्मा को एकान्ततः अनित्य कहता है। यह मन्तव्य भी एकांगी और अपूर्ण है। आत्मा को एकान्त क्षणभंगुर मानने पर बन्ध-मोक्ष घटित नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा मान्य कर्मवाद और पुनर्जन्मवाद भी घटित नहीं होते। बौद्धदर्शन आत्मा के विषय में वस्तुतः अस्पष्ट है । एक ओर वह निरात्मवादी है तो दूसरी ओर पुनर्जन्म और कर्मवाद को मानता है। जैनदर्शन आत्मा के सम्बन्ध में बहुत स्पष्ट है। वह आत्मा को अनेकान्तदृष्टि से नित्यानित्य रूप मानता है, उसका बंध और मोक्ष होना मानता है। यहाँ तक कि वह आत्मा को अमूर्त मानता हुआ भी सांसारिक आत्मा को कथंचित् मूर्त भी मानता है। संसारी आत्मा शरीर धारण करती है, इन्द्रियों के माध्यम से वह वस्तु को ग्रहण करती है, आहार, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मनयुक्त होती है। ये सब परिणतियां होने के कारण आत्मा को कथंचित् मूर्त भी माना गया है। सांसारिक जीवों की सारी प्रवृत्तियां आत्मा और शरीर के योग से होती हैं अतएव वे यौगिक हैं। अकेली आत्मा में ये क्रियाएँ नहीं हो सकती हैं और अकेले शरीर में भी ये क्रियाएँ सम्भव नहीं हैं। नवविध मन्तव्य __. संसारसमापनक जीव के भेदों को बताने के लिए नौ प्रकार की मान्यताओं का उल्लेख किया गया है। प्रथम प्रत्तिपत्ति (मान्यता) के अनुसार संसारी जीव के दो भेद किय गये हैं-त्रस और स्थावर। दूसरी प्रतिपत्ति के अनुसार तीन प्रकार कहे गये हैं-स्त्री, पुरुष और नपुंसक। तीसरी प्रतिपत्ति के अनुसार संसारी जीव के चार भेद कहे गये हैं-नैरयिक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देव. चौथी प्रतिपत्ति के अनुसार पांच भेद कहे गये हैं-एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय । पंचम प्रतिपत्ति के अनुसार संसारी जीव के छह भेद हैं-पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय। छठी प्रतिपत्ति के अनुसार संसारी जीव के सात भेद कहे गये हैं-नैरयिक, तिर्यंच, तिर्यञ्चिनी, मनुष्य, मानुषी, देव और देवी। सप्तम प्रतिपत्ति में संसारी जीव के आठ भेद प्ररूपित हैं-प्रथम समयवर्ती नैरयिक, अप्रथम समयवर्ती नैरयिक, एवं प्रथम समय तिर्यंच अप्रथम समय तिर्यंच, प्रथम समय मनुष्य, अप्रथम समय मनुष्य, प्रथम समय देव और अप्रथम समय देव।
अष्टम प्रतिपत्ति में सांसारिक जीव के नौ भेद प्ररूपित हैं-पृथ्वीकायिक, अपकायिक, तेजस्कायिक, वायुकयिक, वनस्पतिकायिक, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय।
___ नवम प्रतिपत्ति में संसारी जीव के दस प्रकार बताये हैं-प्रथम समय एकेन्द्रिय से प्रथम समय पंचेन्द्रिय तक पांच और अप्रथम समय एकेन्द्रिय से अप्रथम समय पंचेन्द्रिय तक पांच; कुल मिलाकर दस प्रकार के संसारी जीव बनाये गये है।
___ उक्त सब प्रतिपत्तियाँ दिखने में पृथक्-पृथक् सी प्रतीत होती हैं परन्तु तात्त्विक दृष्टि से उनमें कोई विरोध नहीं है। अलग-अलग दृष्टिकोण से एक ही वस्तु का स्वरूप अलग-अलग प्रतीत होता है किन्तु उनमें विरोध नहीं होता। वर्गीकरण की भिन्नता को लेकर अलग-अलग प्ररूपणा है परन्तु उक्त सब प्रतिपत्तियाँ अविरोधिनी हैं। अनेकान्त दृष्टि की यही विशेषता है।
[२३]