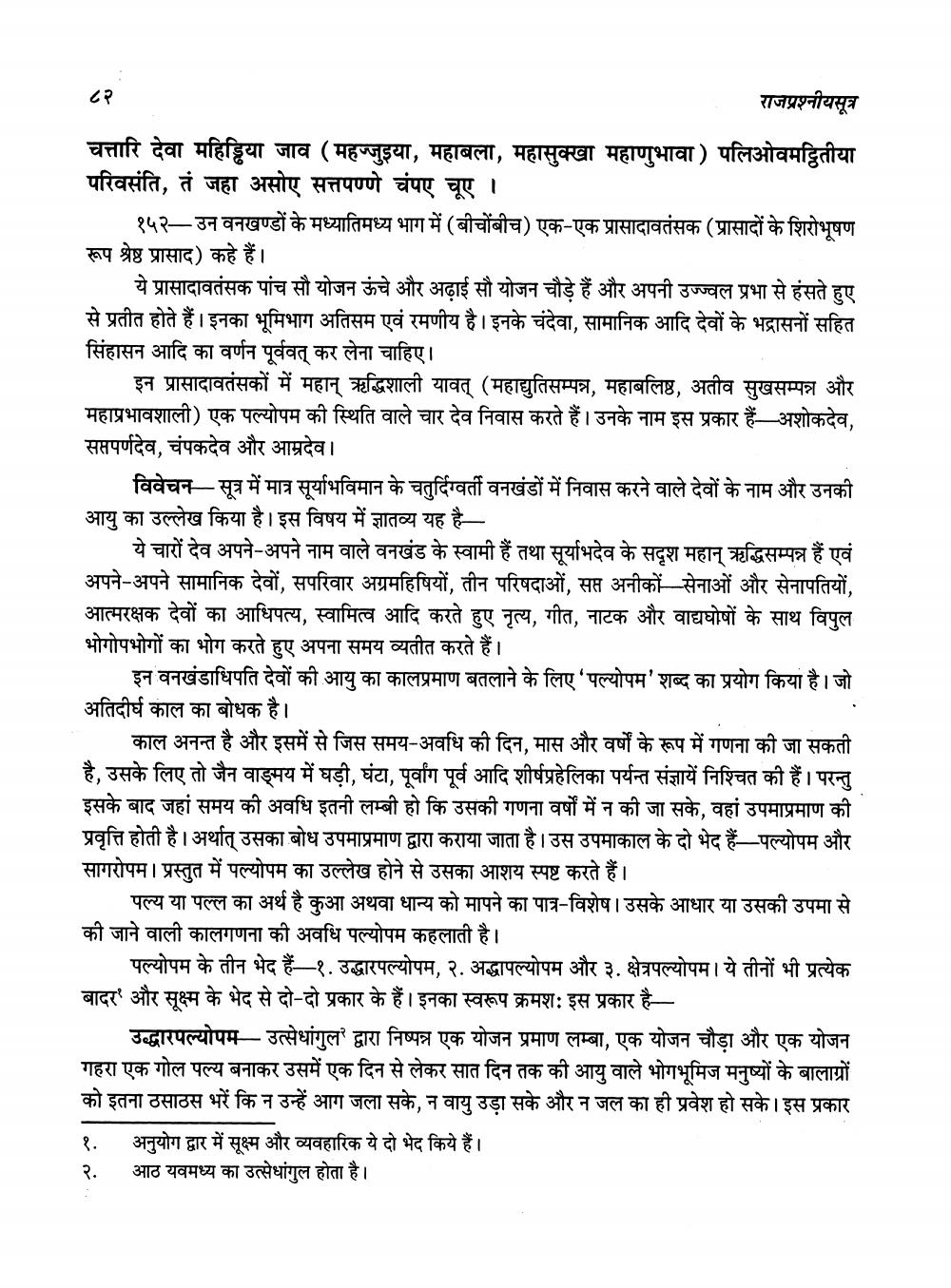________________
राजप्रश्नीयसूत्र
चत्तारि देवा महिड्डिया जाव ( महज्जुइया, महाबला, महासुक्खा महाणुभावा) पलिओवमद्वितीया परिवसंति, तं जहा असोए सत्तपणे चंपए चूए ।
८२
१५२ – उन वनखण्डों के मध्यातिमध्य भाग में (बीचोंबीच ) एक-एक प्रासादावतंसक (प्रासादों के शिरोभूषण रूप श्रेष्ठ प्रासाद) कहे हैं ।
ये प्रासादावतंसक पांच सौ योजन ऊंचे और अढ़ाई सौ योजन चौड़े हैं और अपनी उज्ज्वल प्रभा से हंसते हुए प्रतीत होते हैं। इनका भूमिभाग अतिसम एवं रमणीय है। इनके चंदेवा, सामानिक आदि देवों के भद्रासनों सहित सिंहासन आदि का वर्णन पूर्ववत् कर लेना चाहिए ।
इन प्रासादावतंसकों में महान् ऋद्धिशाली यावत् (महाद्युतिसम्पन्न, महाबलिष्ठ, अतीव सुखसम्पन्न और महाप्रभावशाली) एक पल्योपम की स्थिति वाले चार देव निवास करते हैं । उनके नाम इस प्रकार हैं— अशोकदेव, सप्तपर्णदेव, चंपकदेव और आम्रदेव ।
विवेचन — सूत्र में मात्र सूर्याभविमान के चतुर्दिग्वर्ती वनखंडों में निवास करने वाले देवों के नाम और उनकी आयु का उल्लेख किया है। इस विषय में ज्ञातव्य यह है—
ये चारों देव अपने-अपने नाम वाले वनखंड के स्वामी हैं तथा सूर्याभदेव के सदृश महान् ऋद्धिसम्पन्न हैं एवं अपने-अपने सामानिक देवों, सपरिवार अग्रमहिषियों, तीन परिषदाओं, सप्त अनीकों सेनाओं और सेनापतियों, आत्मरक्षक देवों का आधिपत्य, स्वामित्व आदि करते हुए नृत्य, गीत, नाटक और वाद्यघोषों के साथ विपुल भोगोपभोगों का भोग करते हुए अपना समय व्यतीत करते हैं।
इन वनखंडाधिपति देवों की आयु का कालप्रमाण बतलाने के लिए 'पल्योपम' शब्द का प्रयोग किया है। जो अतिदीर्घ काल का बोधक है।
काल अनन्त है और इसमें से जिस समय अवधि की दिन, मास और वर्षों के रूप में गणना की जा सकती है, उसके लिए तो जैन वाड्मय में घड़ी, घंटा, पूर्वांग पूर्व आदि शीर्षप्रहेलिका पर्यन्त संज्ञायें निश्चित की हैं। परन्तु इसके बाद जहां समय की अवधि इतनी लम्बी हो कि उसकी गणना वर्षों में न की जा सके, वहां उपमाप्रमाण की प्रवृत्ति होती है। अर्थात् उसका बोध उपमाप्रमाण द्वारा कराया जाता है। उस उपमाकाल के दो भेद हैं—पल्योपम और सागरोपम। प्रस्तुत में पल्योपम का उल्लेख होने से उसका आशय स्पष्ट करते हैं।
पल् या पल्ल का अर्थ है कुआ अथवा धान्य को मापने का पात्र - विशेष। उसके आधार या उसकी उपमा से की जाने वाली कालगणना की अवधि पल्योपम कहलाती है ।
पल्योपम के तीन भेद हैं- १. उद्धारपल्योपम, २. अद्धापल्योपम और ३ क्षेत्रपल्योपम। ये तीनों भी प्रत्येक बादर' और सूक्ष्म के भेद से दो-दो प्रकार के हैं। इनका स्वरूप क्रमश: इस प्रकार है-—
उद्धारपल्योपम—- उत्सेधांगुल' द्वारा निष्पन्न एक योजन प्रमाण लम्बा, एक योजन चौड़ा और एक योजन गहरा एक गोल पल्य बनाकर उसमें एक दिन से लेकर सात दिन तक की आयु वाले भोगभूमिज मनुष्यों के बालाग्रों को इतना ठसाठस भरें कि न उन्हें आग जला सके, न वायु उड़ा सके और न जल का ही प्रवेश हो सके। इस प्रकार
१.
२.
अनुयोगद्वार में सूक्ष्म और व्यवहारिक ये दो भेद किये हैं।
आठ यवमध्य का उत्सेधांगुल होता है।