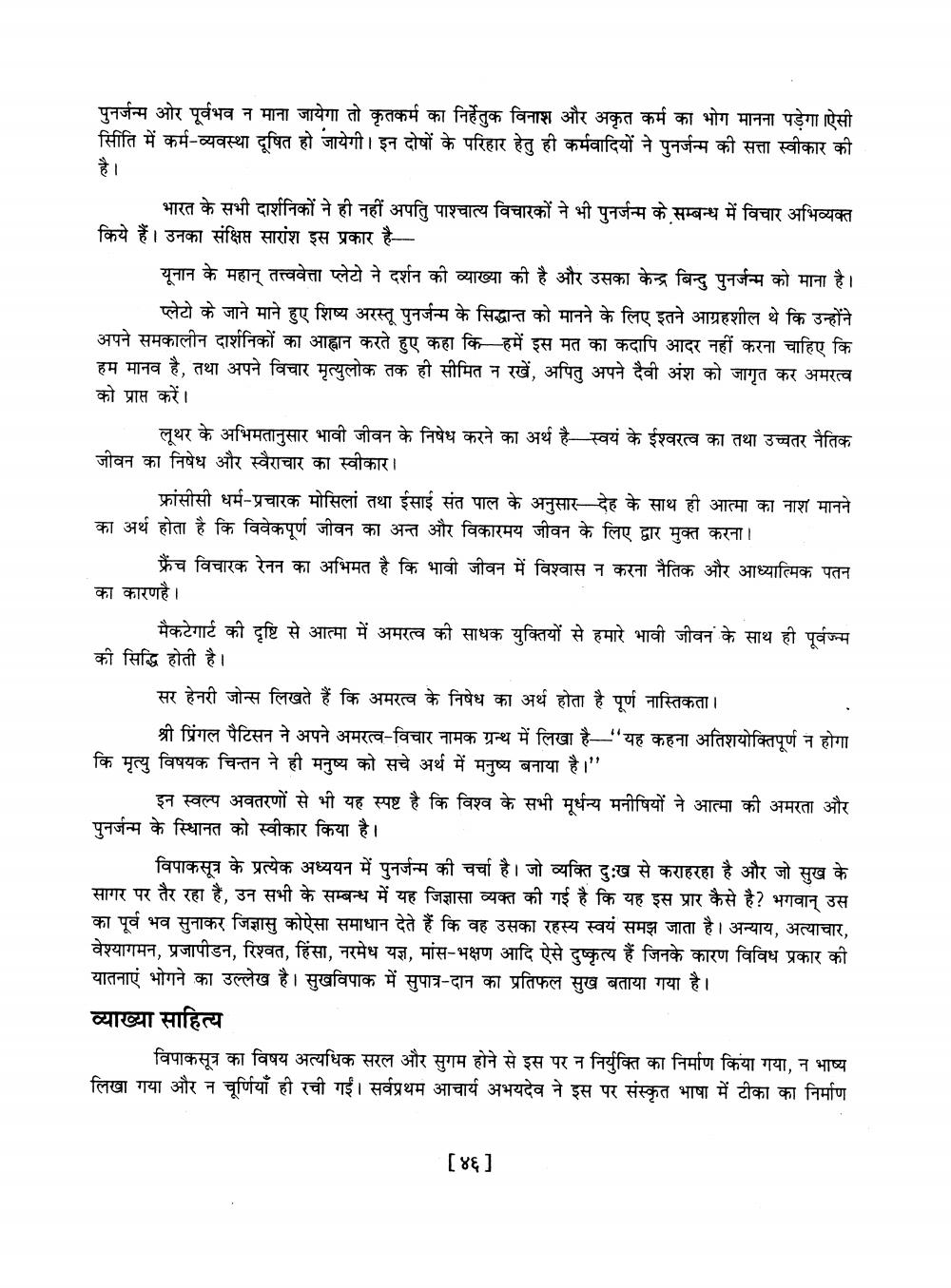________________
पुनर्जन्म ओर पूर्वभव न माना जायेगा तो कृतकर्म का निर्हेतुक विनाश और अकृत कर्म का भोग मानना पड़ेगा ऐसी सिीति में कर्म-व्यवस्था दूषित हो जायेगी। इन दोषों के परिहार हेतु ही कर्मवादियों ने पुनर्जन्म की सत्ता स्वीकार की
है।
भारत के सभी दार्शनिकों ने ही नहीं अपतुि पाश्चात्य विचारकों ने भी पुनर्जन्म के सम्बन्ध में विचार अभिव्यक्त किये हैं। उनका संक्षिप्त सारांश इस प्रकार है
यूनान के महान् तत्त्ववेत्ता प्लेटो ने दर्शन की व्याख्या की है और उसका केन्द्र बिन्दु पुनर्जन्म को माना है।
प्लेटो के जाने माने हुए शिष्य अरस्तू पुनर्जन्म के सिद्धान्त को मानने के लिए इतने आग्रहशील थे कि उन्होंने अपने समकालीन दार्शनिकों का आह्वान करते हुए कहा कि हमें इस मत का कदापि आदर नहीं करना चाहिए कि हम मानव है, तथा अपने विचार मृत्युलोक तक ही सीमित न रखें, अपितु अपने दैवी अंश को जागृत कर अमरत्व को प्राप्त करें।
लूथर के अभिमतानुसार भावी जीवन के निषेध करने का अर्थ है स्वयं के ईश्वरत्व का तथा उच्चतर नैतिक जीवन का निषेध और स्वैराचार का स्वीकार।
फ्रांसीसी धर्म-प्रचारक मोसिलां तथा ईसाई संत पाल के अनुसार-देह के साथ ही आत्मा का नाश मानने का अर्थ होता है कि विवेकपूर्ण जीवन का अन्त और विकारमय जीवन के लिए द्वार मुक्त करना।
फ्रैंच विचारक रेनन का अभिमत है कि भावी जीवन में विश्वास न करना नैतिक और आध्यात्मिक पतन का कारणहै।
मैकटेगार्ट की दृष्टि से आत्मा में अमरत्व की साधक युक्तियों से हमारे भावी जीवन के साथ ही पूर्वज्म की सिद्धि होती है।
सर हेनरी जोन्स लिखते हैं कि अमरत्व के निषेध का अर्थ होता है पूर्ण नास्तिकता।
श्री प्रिंगल पैटिसन ने अपने अमरत्व-विचार नामक ग्रन्थ में लिखा है-"यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा कि मृत्यु विषयक चिन्तन ने ही मनुष्य को सचे अर्थ में मनुष्य बनाया है।"
इन स्वल्प अवतरणों से भी यह स्पष्ट है कि विश्व के सभी मूर्धन्य मनीषियों ने आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म के स्धिानत को स्वीकार किया है।
विपाकसूत्र के प्रत्येक अध्ययन में पुनर्जन्म की चर्चा है। जो व्यक्ति दु:ख से कराहरहा है और जो सुख के सागर पर तैर रहा है, उन सभी के सम्बन्ध में यह जिज्ञासा व्यक्त की गई है कि यह इस प्रार कैसे है? भगवान् उस का पूर्व भव सुनाकर जिज्ञासु कोऐसा समाधान देते हैं कि वह उसका रहस्य स्वयं समझ जाता है। अन्याय, अत्याचार, वेश्यागमन, प्रजापीडन, रिश्वत, हिंसा, नरमेध यज्ञ, मांस-भक्षण आदि ऐसे दुष्कृत्य हैं जिनके कारण विविध प्रकार की यातनाएं भोगने का उल्लेख है। सुखविपाक में सुपात्र-दान का प्रतिफल सुख बताया गया है। व्याख्या साहित्य
विपाकसूत्र का विषय अत्यधिक सरल और सुगम होने से इस पर न नियुक्ति का निर्माण किया गया, न भाष्य लिखा गया और न चूर्णियाँ ही रची गईं। सर्वप्रथम आचार्य अभयदेव ने इस पर संस्कृत भाषा में टीका का निर्माण
[४६]