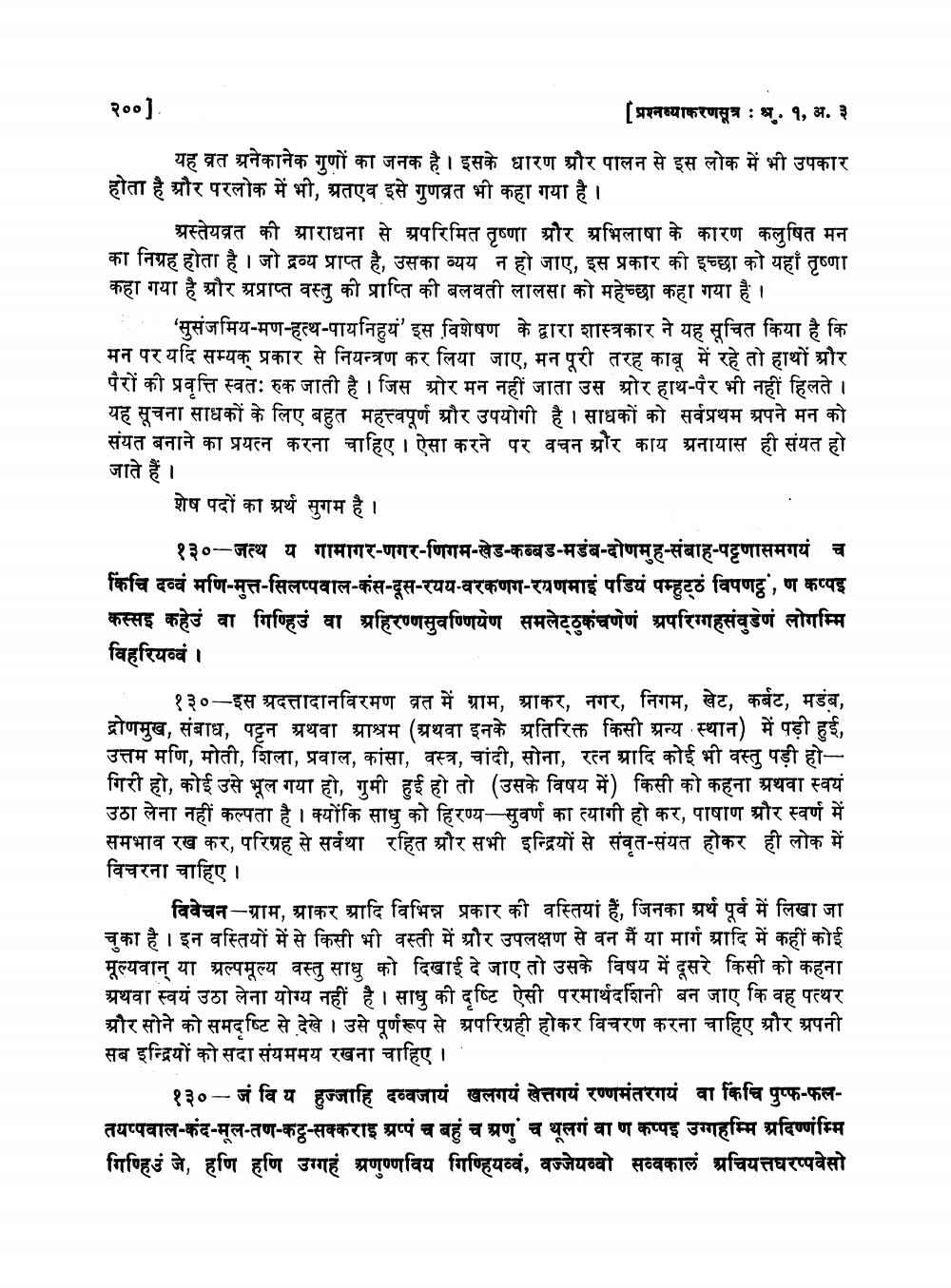________________
२००]
[प्रश्नव्याकरणसूत्र : शु. १, अ. ३
ATT तरह
यह व्रत अनेकानेक गुणों का जनक है। इसके धारण और पालन से इस लोक में भी उपकार होता है और परलोक में भी, अतएव इसे गुणव्रत भी कहा गया है ।
अस्तेयव्रत की आराधना से अपरिमित तृष्णा और अभिलाषा के कारण कलुषित मन का निग्रह होता है । जो द्रव्य प्राप्त है, उसका व्यय न हो जाए, इस प्रकार की इच्छा को यहाँ तृष्णा कहा गया है और अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति की बलवती लालसा को महेच्छा कहा गया है।
'सुसंजमिय-मण-हत्थ-पायनियं' इस विशेषण के द्वारा शास्त्रकार ने यह सूचित किया है कि मन पर यदि सम्यक प्रकार से नियन्त्रण कर लिया जाए,
हाथों और पैरों की प्रवृत्ति स्वतः रुक जाती है । जिस ओर मन नहीं जाता उस ओर हाथ-पैर भी नहीं हिलते । यह सूचना साधकों के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण और उपयोगी है। साधकों को सर्वप्रथम अपने मन को संयत बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा करने पर वचन और काय अनायास ही संयत हो जाते हैं।
शेष पदों का अर्थ सुगम है।
१३०-जत्थ य गामागर-णगर-णिगम-खेड-कब्बड-मडंब-दोणमुह-संबाह-पट्टणासमगयं च किंचि दव्वं मणि-मुत्त-सिलप्पवाल-कंस-दूस-रयय-वरकणग-रयणमाइं पडियं पम्हुठें विपणट्ठ', ण कप्पइ कस्सइ कहेउं वा गिहिउँ वा अहिरण्णसुवण्णियेण समलेठुकंचणेणं अपरिग्गहसंवुडेणं लोगम्मि विहरियव्वं ।
१३०–इस अदत्तादानविरमण व्रत में ग्राम, प्राकर, नगर, निगम, खेट, कर्बट, मडंब, द्रोणमुख, संबाध, पट्टन अथवा आश्रम (अथवा इनके अतिरिक्त किसी अन्य स्थान) में पड़ी हुई, उत्तम मणि, मोती, शिला, प्रवाल, कांसा, वस्त्र, चांदी, सोना, रत्न आदि कोई भी वस्तु पड़ी होगिरी हो, कोई उसे भूल गया हो, गुमी हुई हो तो (उसके विषय में) किसी को कहना अथवा स्वयं उठा लेना नहीं कल्पता है। क्योंकि साधु को हिरण्य-सूवर्ण का त्यागी हो कर, पाषाण और स्वर्ण में समभाव रख कर, परिग्रह से सर्वथा रहित और सभी इन्द्रियों से संवृत-संयत होकर ही लोक में विचरना चाहिए।
विवेचन-ग्राम, आकर आदि विभिन्न प्रकार की वस्तियां हैं, जिनका अर्थ पूर्व में लिखा जा चुका है । इन वस्तियों में से किसी भी वस्ती में और उपलक्षण से वन मैं या मार्ग आदि में कहीं कोई मूल्यवान् या अल्पमूल्य वस्तु साधु को दिखाई दे जाए तो उसके विषय में दूसरे किसी को कहना अथवा स्वयं उठा लेना योग्य नहीं है। साधु की दृष्टि ऐसी परमार्थदर्शिनी बन जाए कि वह पत्थर और सोने को समदृष्टि से देखे । उसे पूर्णरूप से अपरिग्रही होकर विचरण करना चाहिए और अपनी सब इन्द्रियों को सदा संयममय रखना चाहिए।
१३० - जं वि य हुन्जाहि दव्वजायं खलगयं खेत्तगयं रण्णमंतरगयं वा किंचि पुप्फ-फलतयप्पवाल-कंद-मूल-तण-कट्ठ-सक्कराइ अप्पं च बहुं च अणुच थूलगं वा ण कप्पइ उग्गहम्मि अदिण्णंम्मि गिहिउं जे, हणि हणि उग्गहं अणुण्णविय गिहियव्वं, वज्जेयव्वो सव्वकालं अचियत्तघरप्पवेसो