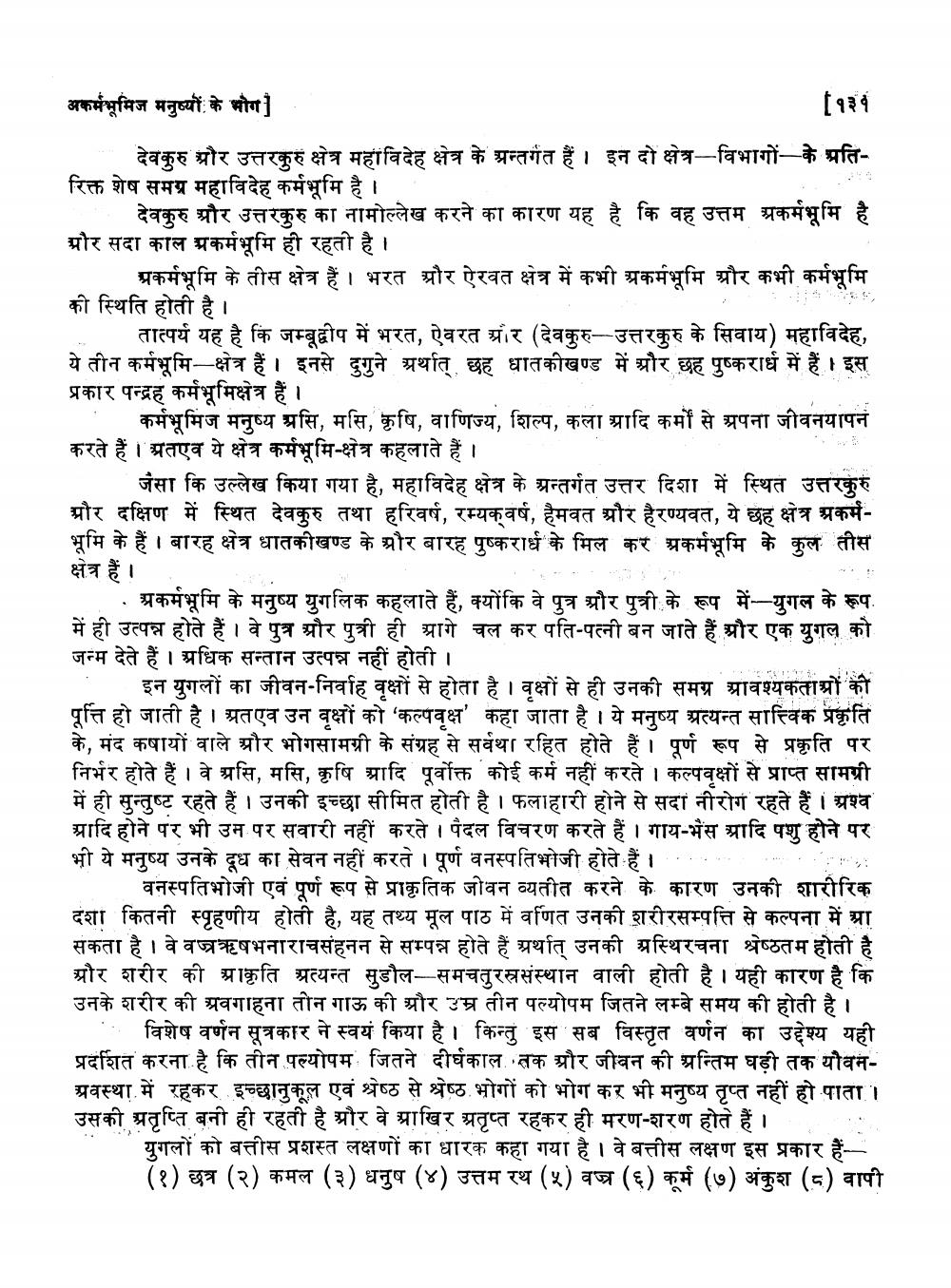________________
अकर्मभूमिज मनुष्यों के भोग]
[१३१ देवकुरु और उत्तरकुरु क्षेत्र महाविदेह क्षेत्र के अन्तर्गत हैं। इन दो क्षेत्र-विभागों के अतिरिक्त शेष समग्र महाविदेह कर्मभूमि है ।
देवकुरु और उत्तरकुरु का नामोल्लेख करने का कारण यह है कि वह उत्तम अकर्मभूमि है और सदा काल अकर्मभूमि ही रहती है।
___ प्रकर्मभूमि के तीस क्षेत्र हैं। भरत और ऐरवत क्षेत्र में कभी अकर्मभूमि और कभी कर्मभूमि की स्थिति होती है। ... तात्पर्य यह है कि जम्बूद्वीप में भरत, ऐवरत और (देवकुरु-उत्तरकुरु के सिवाय) महाविदेह, ये तीन कर्मभूमि-क्षेत्र हैं। इनसे दुगुने अर्थात् छह धातकीखण्ड में और छह पुष्करार्ध में हैं । इस प्रकार पन्द्रह कर्मभूमिक्षेत्र हैं।
- कर्मभूमिज मनुष्य असि, मसि, कृषि, वाणिज्य, शिल्प, कला आदि कर्मों से अपना जीवनयापन करते हैं । अतएव ये क्षेत्र कर्मभूमि-क्षेत्र कहलाते हैं ।
जैसा कि उल्लेख किया गया है, महाविदेह क्षेत्र के अन्तर्गत उत्तर दिशा में स्थित उत्तरकुरु और दक्षिण में स्थित देवकुरु तथा हरिवर्ष, रम्यक्वर्ष, हैमवत और हैरण्यवत, ये छह क्षेत्र अकर्मभूमि के हैं । बारह क्षेत्र धातकीखण्ड के और बारह पुष्करार्ध के मिल कर अकर्मभूमि के कुल तीस क्षेत्र हैं। __. अकर्मभूमि के मनुष्य युगलिक कहलाते हैं, क्योंकि वे पुत्र और पुत्री के रूप में-युगल के रूप में ही उत्पन्न होते हैं । वे पुत्र और पुत्री ही आगे चल कर पति-पत्नी बन जाते हैं और एक युगल को जन्म देते हैं। अधिक सन्तान उत्पन्न नहीं होती।
इन युगलों का जीवन-निर्वाह वृक्षों से होता है । वृक्षों से ही उनकी समग्र आवश्यकताओं को पूत्ति हो जाती है । अतएव उन वृक्षों को 'कल्पवृक्ष' कहा जाता है । ये मनुष्य अत्यन्त सात्त्विक प्रकृति के, मंद कषायों वाले और भोगसामग्री के संग्रह से सर्वथा रहित होते हैं। पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर होते हैं । वे असि, मसि, कृषि आदि पूर्वोक्त कोई कर्म नहीं करते । कल्पवृक्षों से प्राप्त सामग्री में ही सुन्तुष्ट रहते हैं । उनकी इच्छा सीमित होती है । फलाहारी होने से सदा नीरोग रहते हैं । अश्व आदि होने पर भी उन पर सवारी नहीं करते । पैदल विचरण करते हैं । गाय-भैंस आदि पशु होने पर भी ये मनुष्य उनके दूध का सेवन नहीं करते । पूर्ण वनस्पतिभोजी होते हैं। . . . .
वनस्पतिभोजी एवं पूर्ण रूप से प्राकृतिक जीवन व्यतीत करने के कारण उनकी शारीरिक दशा कितनी स्पृहणीय होती है, यह तथ्य मूल पाठ में वणित उनकी शरीरसम्पत्ति से कल्पना में आ सकता है । वे वज्रऋषभनाराचसंहनन से सम्पन्न होते हैं अर्थात् उनकी अस्थिरचना श्रेष्ठतम होती है और शरीर की प्राकृति अत्यन्त सुडौल-समचतुरस्रसंस्थान वाली होती है। यही कारण है कि उनके शरीर की अवगाहना तीन गाऊ की और उम्र तीन पल्योपम जितने लम्बे समय की होती है।
- विशेष वर्णन सूत्रकार ने स्वयं किया है। किन्तु इस सब विस्तृत वर्णन का उद्देश्य यही प्रदर्शित करना है कि तीन पल्योपम जितने दीर्घकाल तक और जीवन की अन्तिम घड़ी तक यौवनअवस्था में रहकर इच्छानुकूल एवं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भोगों को भोग कर भी मनुष्य तृप्त नहीं हो पाता। उसकी अतृप्ति बनी ही रहती है और वे आखिर अतृप्त रहकर ही मरण-शरण होते हैं।
यगलों को बत्तीस प्रशस्त लक्षणों का धारक कहा गया है। वे बत्तीस लक्षण इस प्रकार हैं(१) छत्र (२) कमल (३) धनुष (४) उत्तम रथ (५) वज्र (६) कूर्म (७) अंकुश (८) वापी