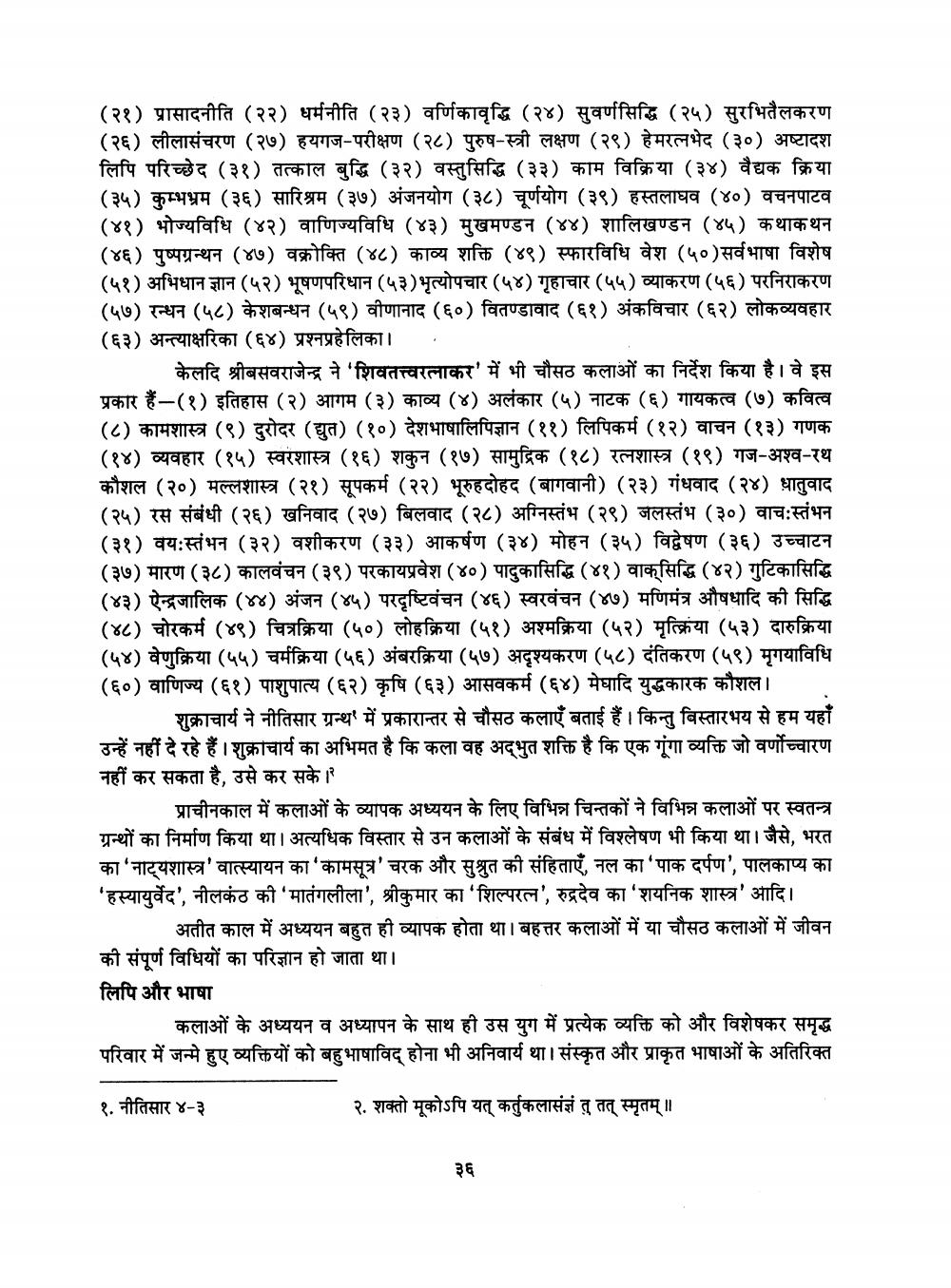________________
(२१) प्रासादनीति (२२) धर्मनीति (२३) वर्णिकावृद्धि (२४) सुवर्णसिद्धि (२५) सुरभितैलकरण (२६) लीलासंचरण (२७) हयगज-परीक्षण (२८) पुरुष-स्त्री लक्षण (२९) हेमरत्नभेद (३०) अष्टादश लिपि परिच्छेद (३१) तत्काल बुद्धि (३२) वस्तुसिद्धि (३३) काम विक्रि या (३४) वैद्यक क्रिया (३५) कुम्भभ्रम (३६) सारिश्रम (३७) अंजनयोग (३८) चूर्णयोग (३९) हस्तलाघव (४०) वचनपाटव (४१) भोज्यविधि (४२) वाणिज्यविधि (४३) मुखमण्डन (४४) शालिखण्डन (४५) कथाकथन (४६) पुष्पग्रन्थन (४७) वक्रोक्ति (४८) काव्य शक्ति (४९) स्फारविधि वेश (५०)सर्वभाषा विशेष (५१) अभिधान ज्ञान (५२) भूषणपरिधान (५३)भृत्योपचार (५४) गृहाचार (५५) व्याकरण (५६) परनिराकरण (५७) रन्धन (५८) केशबन्धन (५९) वीणानाद (६०) वितण्डावाद (६१) अंकविचार (६२) लोकव्यवहार (६३) अन्त्याक्षरिका (६४) प्रश्नप्रहेलिका।
केलदि श्रीबसवराजेन्द्र ने 'शिवतत्त्वरत्नाकर' में भी चौसठ कलाओं का निर्देश किया है। वे इस प्रकार हैं-(१) इतिहास (२) आगम (३) काव्य (४) अलंकार (५) नाटक (६) गायकत्व (७) कवित्व (८) कामशास्त्र (९) दुरोदर (द्युत) (१०) देशभाषालिपिज्ञान (११) लिपिकर्म (१२) वाचन (१३) गणक (१४) व्यवहार (१५) स्वरशास्त्र (१६) शकुन (१७) सामुद्रिक (१८) रत्नशास्त्र (१९) गज-अश्व-रथ कौशल (२०) मल्लशास्त्र (२१) सूपकर्म (२२) भूरुहदोहद (बागवानी) (२३) गंधवाद (२४) धातुवाद (२५) रस संबंधी (२६) खनिवाद (२७) बिलवाद (२८) अग्निस्तंभ (२९) जलस्तंभ (३०) वाचःस्तंभन (३१) वयःस्तंभन (३२) वशीकरण (३३) आकर्षण (३४) मोहन (३५) विद्वेषण (३६) उच्चाटन (३७) मारण (३८) कालवंचन (३९) परकायप्रवेश (४०) पादुकासिद्धि (४१) वाक्सिद्धि (४२) गुटिकासिद्धि (४३) ऐन्द्रजालिक (४४) अंजन (४५) परदष्टिवंचन (४६) स्वरवंचन (४७) मणिमंत्र औषधादि की सिद्धि (४८) चोरकर्म (४९) चित्रक्रिया (५०) लोहक्रिया (५१) अश्मक्रिया (५२) मृत्क्रिया (५३) दारुक्रिया (५४) वेणुक्रिया (५५) चर्मक्रिया (५६) अंबरक्रिया (५७) अदृश्यकरण (५८) दंतिकरण (५९) मृगयाविधि (६०) वाणिज्य (६१) पाशुपात्य (६२) कृषि (६३) आसवकर्म (६४) मेघादि युद्धकारक कौशल।
शुक्राचार्य ने नीतिसार ग्रन्थ' में प्रकारान्तर से चौसठ कलाएं बताई हैं । किन्तु विस्तारभय से हम यहाँ उन्हें नहीं दे रहे हैं। शुक्राचार्य का अभिमत है कि कला वह अद्भुत शक्ति है कि एक गूंगा व्यक्ति जो वर्णोच्चारण नहीं कर सकता है, उसे कर सके।
प्राचीनकाल में कलाओं के व्यापक अध्ययन के लिए विभिन्न चिन्तकों ने विभिन्न कलाओं पर स्वतन्त्र ग्रन्थों का निर्माण किया था। अत्यधिक विस्तार से उन कलाओं के संबंध में विश्लेषण भी किया था। जैसे, भरत का 'नाट्यशास्त्र' वात्स्यायन का 'कामसूत्र' चरक और सुश्रुत की संहिताएँ, नल का 'पाक दर्पण', पालकाप्य का 'हस्यायुर्वेद', नीलकंठ की 'मातंगलीला', श्रीकुमार का 'शिल्परल', रुद्रदेव का 'शयनिक शास्त्र' आदि।
अतीत काल में अध्ययन बहुत ही व्यापक होता था। बहत्तर कलाओं में या चौसठ कलाओं में जीवन की संपूर्ण विधियों का परिज्ञान हो जाता था। लिपि और भाषा
कलाओं के अध्ययन व अध्यापन के साथ ही उस युग में प्रत्येक व्यक्ति को और विशेषकर समृद्ध परिवार में जन्मे हुए व्यक्तियों को बहुभाषाविद् होना भी अनिवार्य था। संस्कृत और प्राकृत भाषाओं के अतिरिक्त
१. नीतिसार ४-३
२. शक्तो मूकोऽपि यत् कर्तुकलासंज्ञं तु तत् स्मृतम्॥
३६