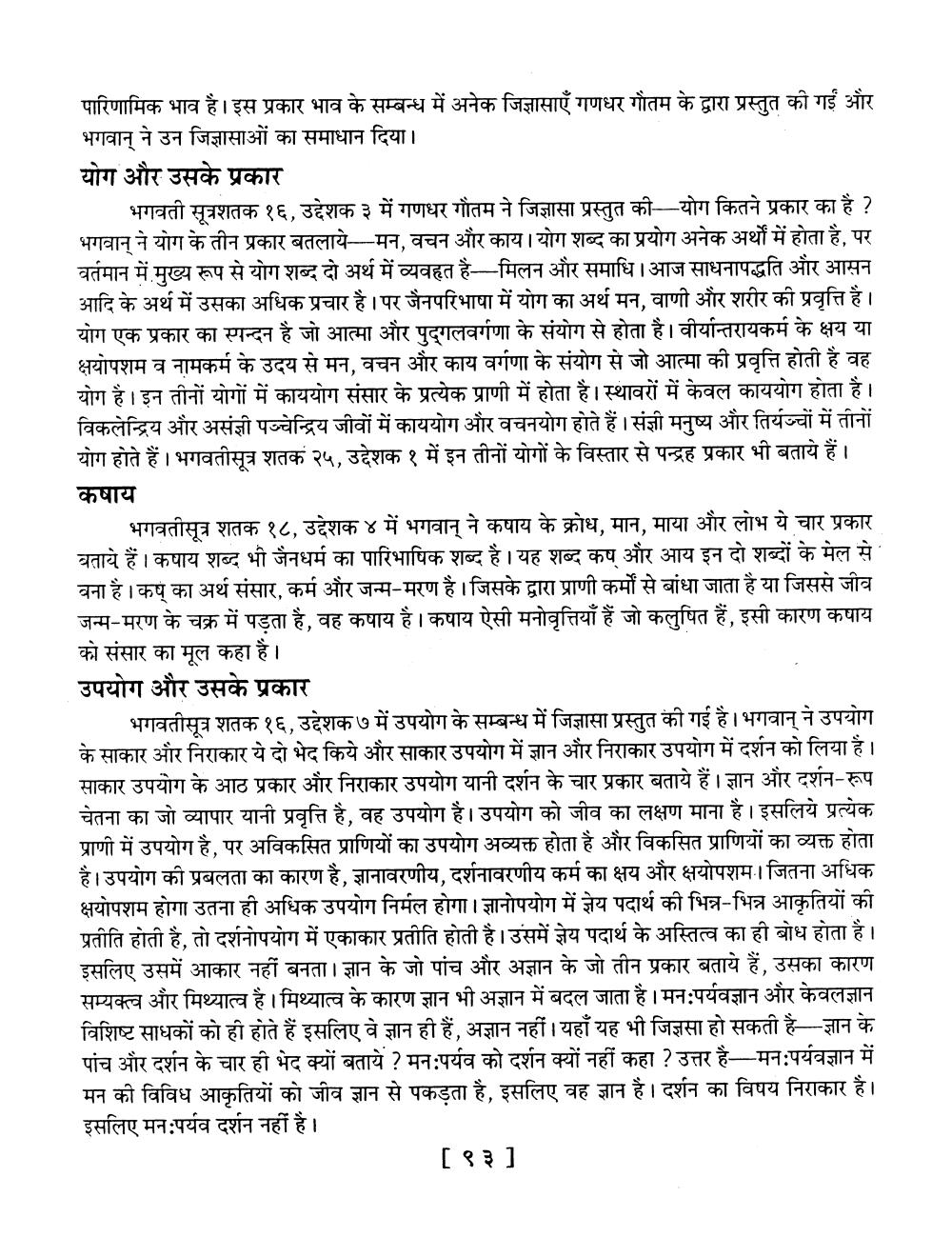________________
पारिणामिक भाव है। इस प्रकार भाव के सम्बन्ध में अनेक जिज्ञासाएँ गणधर गौतम के द्वारा प्रस्तुत की गईं और भगवान् ने उन जिज्ञासाओं का समाधान दिया ।
योग और उसके प्रकार
भगवती सूत्रशतक १६, उद्देशक ३ में गणधर गौतम ने जिज्ञासा प्रस्तुत की—योग कितने प्रकार का है ? भगवान् ने योग के तीन प्रकार बतलाये मन, वचन और काय । योग शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में होता है, पर वर्तमान में मुख्य रूप से योग शब्द दो अर्थ में व्यवहृत है— मिलन और समाधि । आज साधनापद्धति और आसन आदि के अर्थ में उसका अधिक प्रचार है। पर जैनपरिभाषा में योग का अर्थ मन, वाणी और शरीर की प्रवृत्ति है । योग एक प्रकार का स्पन्दन है जो आत्मा और पुद्गलवर्गणा के संयोग से होता है । वीर्यान्तरायकर्म के क्षय या क्षयोपशम व नामकर्म के उदय से मन, वचन और काय वर्गणा के संयोग से जो आत्मा की प्रवृत्ति होती है वह योग है। इन तीनों योगों में काययोग संसार के प्रत्येक प्राणी में होता है । स्थावरों में केवल काययोग होता है । विकलेन्द्रिय और असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीवों में काययोग और वचनयोग होते हैं। संज्ञी मनुष्य और तिर्यञ्चों में तीनों योग होते हैं । भगवतीसूत्र शतकं २५, उद्देशक १ में इन तीनों योगों के विस्तार से पन्द्रह प्रकार भी बताये हैं । कषाय
भगवतीसूत्र शतक १८, उद्देशक ४ में भगवान् ने कषाय के क्रोध, मान, माया और लोभ ये चार प्रकार बताये हैं । कषाय शब्द भी जैनधर्म का पारिभाषिक शब्द है । यह शब्द कष और आय इन दो शब्दों के मेल से बना है। कं का अर्थ संसार, कर्म और जन्म-मरण है। जिसके द्वारा प्राणी कर्मों से बांधा जाता है या जिससे जीव जन्म-मरण के चक्र में पड़ता है, वह कषाय । कषाय ऐसी मनोवृत्तियाँ हैं जो कलुषित हैं, इसी कारण कषाय को संसार का मूल कहा है ।
उपयोग और उसके प्रकार
भगवतीसूत्र शतक १६, उद्देशक ७ में उपयोग के सम्बन्ध में जिज्ञासा प्रस्तुत की गई है। भगवान् ने उपयोग के साकार और निराकार ये दो भेद किये और साकार उपयोग में ज्ञान और निराकार उपयोग में दर्शन को लिया है। साकार उपयोग के आठ प्रकार और निराकार उपयोग यानी दर्शन के चार प्रकार बताये हैं। ज्ञान और दर्शन - रूप चेतना का जो व्यापार यानी प्रवृत्ति है, वह उपयोग है। उपयोग को जीव का लक्षण माना है। इसलिये प्रत्येक प्राणी में उपयोग है, पर अविकसित प्राणियों का उपयोग अव्यक्त होता है और विकसित प्राणियों का व्यक्त होता
। उपयोग की प्रबलता का कारण है, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय कर्म का क्षय और क्षयोपशम । जितना अधिक क्षयोपशम होगा उतना ही अधिक उपयोग निर्मल होगा। ज्ञानोपयोग में ज्ञेय पदार्थ की भिन्न-भिन्न आकृतियों की प्रतीति होती है, तो दर्शनोपयोग में एकाकार प्रतीति होती है। उसमें ज्ञेय पदार्थ के अस्तित्व का ही बोध होता है । इसलिए उसमें आकार नहीं बनता । ज्ञान के जो पांच और अज्ञान के जो तीन प्रकार बताये हैं, उसका कारण सम्यक्त्व और मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के कारण ज्ञान भी अज्ञान में बदल जाता है। मनः पर्यवज्ञान और केवलज्ञान विशिष्ट साधकों को ही होते हैं इसलिए वे ज्ञान ही हैं, अज्ञान नहीं। यहाँ यह भी जिज्ञसा हो सकती है— ज्ञान के पांच और दर्शन के चार ही भेद क्यों बतायें ? मनः पर्यव को दर्शन क्यों नहीं कहा ? उत्तर है— मनः पर्यवज्ञान में मन की विविध आकृतियों को जीव ज्ञान से पकड़ता है, इसलिए वह ज्ञान है। दर्शन का विषय निराकार है । इसलिए मनः पर्यव दर्शन नहीं हैं।
[ ९३ ]