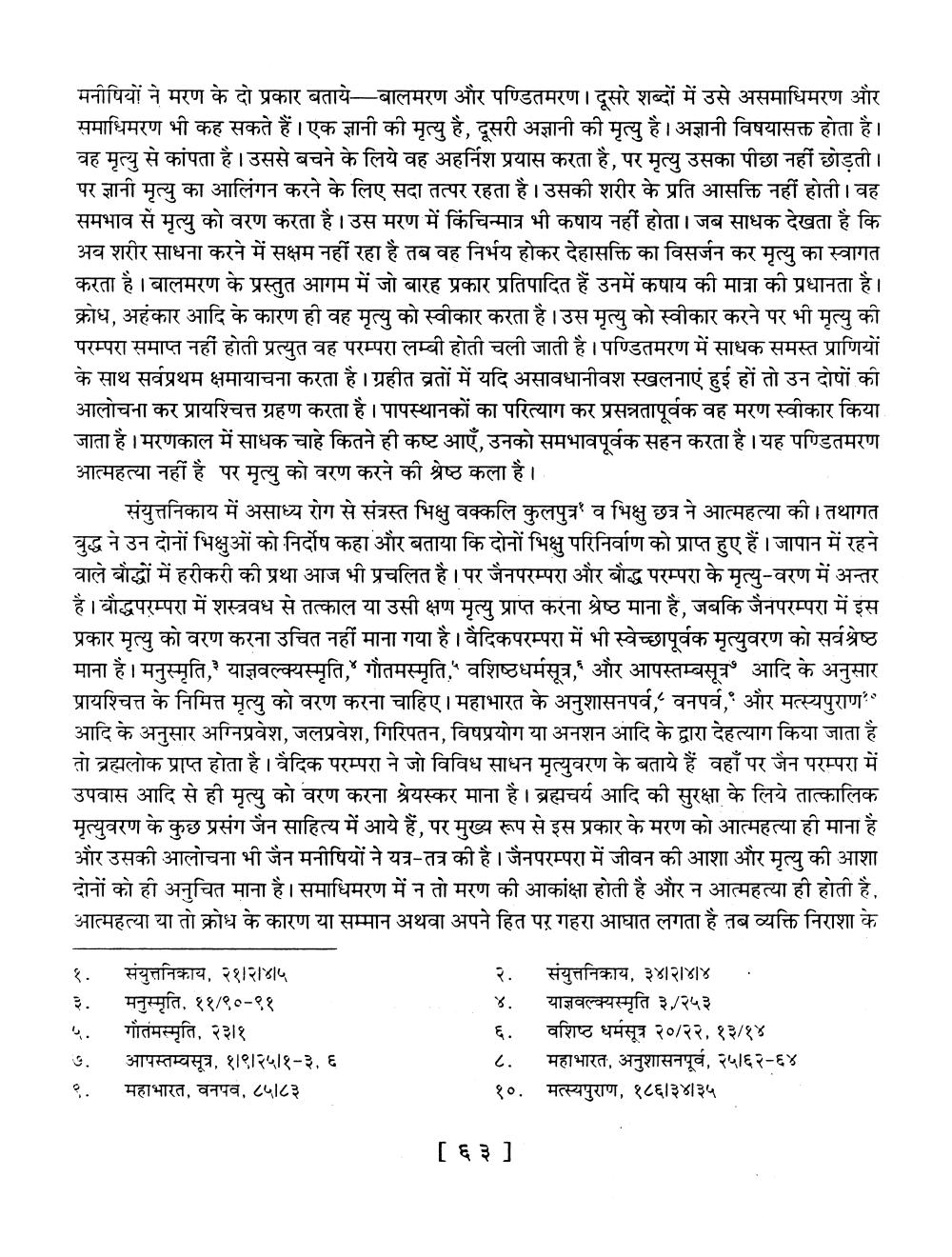________________
मनीषियों ने मरण के दो प्रकार बताये - बालमरण और पण्डितमरण । दूसरे शब्दों में उसे असमाधिमरण और समाधिमरण भी कह सकते हैं। एक ज्ञानी की मृत्यु है, दूसरी अज्ञानी की मृत्यु है । अज्ञानी विषयासक्त होता है। वह मृत्यु से कांपता है । उससे बचने के लिये वह अहर्निश प्रयास करता है, पर मृत्यु उसका पीछा नहीं छोड़ती। पर ज्ञानी मृत्यु का आलिंगन करने के लिए सदा तत्पर रहता है। उसकी शरीर के प्रति आसक्ति नहीं होती । वह समभाव से मृत्यु को वरण करता है । उस मरण में किंचिन्मात्र भी कषाय नहीं होता । जब साधक देखता है अव शरीर साधना करने में सक्षम नहीं रहा है तब वह निर्भय होकर देहासक्ति का विसर्जन कर मृत्यु का स्वागत करता है । बालमरण के प्रस्तुत आगम में जो बारह प्रकार प्रतिपादित हैं उनमें कषाय की मात्रा की प्रधानता है । क्रोध, अहंकार आदि के कारण ही वह मृत्यु को स्वीकार करता है। उस मृत्यु को स्वीकार करने पर भी मृत्यु की परम्परा समाप्त नहीं होती प्रत्युत वह परम्परा लम्बी होती चली जाती है। पण्डितमरण में साधक समस्त प्राणियों के साथ सर्वप्रथम क्षमायाचना करता है । ग्रहीत व्रतों में यदि असावधानीवश स्खलनाएं हुई हों तो उन दोषों की आलोचना कर प्रायश्चित्त ग्रहण करता है । पापस्थानकों का परित्याग कर प्रसन्नतापूर्वक वह मरण स्वीकार किया जाता है । मरणकाल में साधक चाहे कितने ही कष्ट आएँ, उनको समभावपूर्वक सहन करता है । यह पण्डितमरण आत्महत्या नहीं है पर मृत्यु को वरण करने की श्रेष्ठ कला है।
संयुत्तनिकाय में असाध्य रोग से संत्रस्त भिक्षु वक्कलि कुलपुत्र' व भिक्षु छत्र ने आत्महत्या की । तथागत बुद्ध ने उन दोनों भिक्षुओं को निर्दोष कहा और बताया कि दोनों भिक्षु परिनिर्वाण को प्राप्त हुए हैं। जापान में रहने वाले बौद्धों में हरीकरी की प्रथा आज भी प्रचलित है। पर जैनपरम्परा और बौद्ध परम्परा के मृत्यु-वरण में अन्तर है। बौद्धपरम्परा में शस्त्रवध से तत्काल या उसी क्षण मृत्यु प्राप्त करना श्रेष्ठ माना है, जबकि जैनपरम्परा में इस प्रकार मृत्यु को वरण करना उचित नहीं माना गया है। वैदिकपरम्परा में भी स्वेच्छापूर्वक मृत्युवरण को सर्वश्रेष्ठ माना है। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्यस्मृति, गौतमस्मृति' वशिष्ठधर्मसूत्र, और आपस्तम्बसूत्र' आदि के अनुसार प्रायश्चित्त के निमित्त मृत्यु को वरण करना चाहिए । महाभारत के अनुशासनपर्व, वनपर्व, और मत्स्यपुराण?" आदि के अनुसार अग्निप्रवेश, जलप्रवेश, गिरिपतन, विषप्रयोग या अनशन आदि के द्वारा देहत्याग किया जाता है तो ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। वैदिक परम्परा ने जो विविध साधन मृत्युवरण के बताये हैं वहाँ पर जैन परम्परा में उपवास आदि से ही मृत्यु को वरण करना श्रेयस्कर माना है। ब्रह्मचर्य आदि की सुरक्षा के लिये तात्कालिक मृत्युवरण के कुछ प्रसंग जैन साहित्य में आये हैं, पर मुख्य रूप से इस प्रकार के मरण को आत्महत्या ही माना है। और उसकी आलोचना भी जैन मनीषियों ने यत्र-तत्र की है। जैनपरम्परा में जीवन की आशा और मृत्यु की आशा दोनों को ही अनुचित माना है। समाधिमरण में न तो मरण की आकांक्षा होती है और न आत्महत्या ही होती है, आत्महत्या या तो क्रोध के कारण या सम्मान अथवा अपने हित पर गहरा आघात लगता है तब व्यक्ति निराशा के
१.
३.
५.
७.
९.
संयुत्तनिकाय, २१/२/४५
मनुस्मृति, ११/९०-९१
गौतमस्मृति, २३|१
आपस्तम्वसूत्र, ११९/२५/१-३, ६
महाभारत, वनपव, ८५ ८३
२.
४.
६.
८.
संयुत्तनिकाय, ३४ |२|४|४ याज्ञवल्क्यस्मृति ३/२५३
[ ६३ ]
वशिष्ठ धर्मसूत्र २०/२२, १३/१४
महाभारत, अनुशासनपूर्व २५/६२-६४
१०. मत्स्यपुराण, १८६ | ३४ / ३५