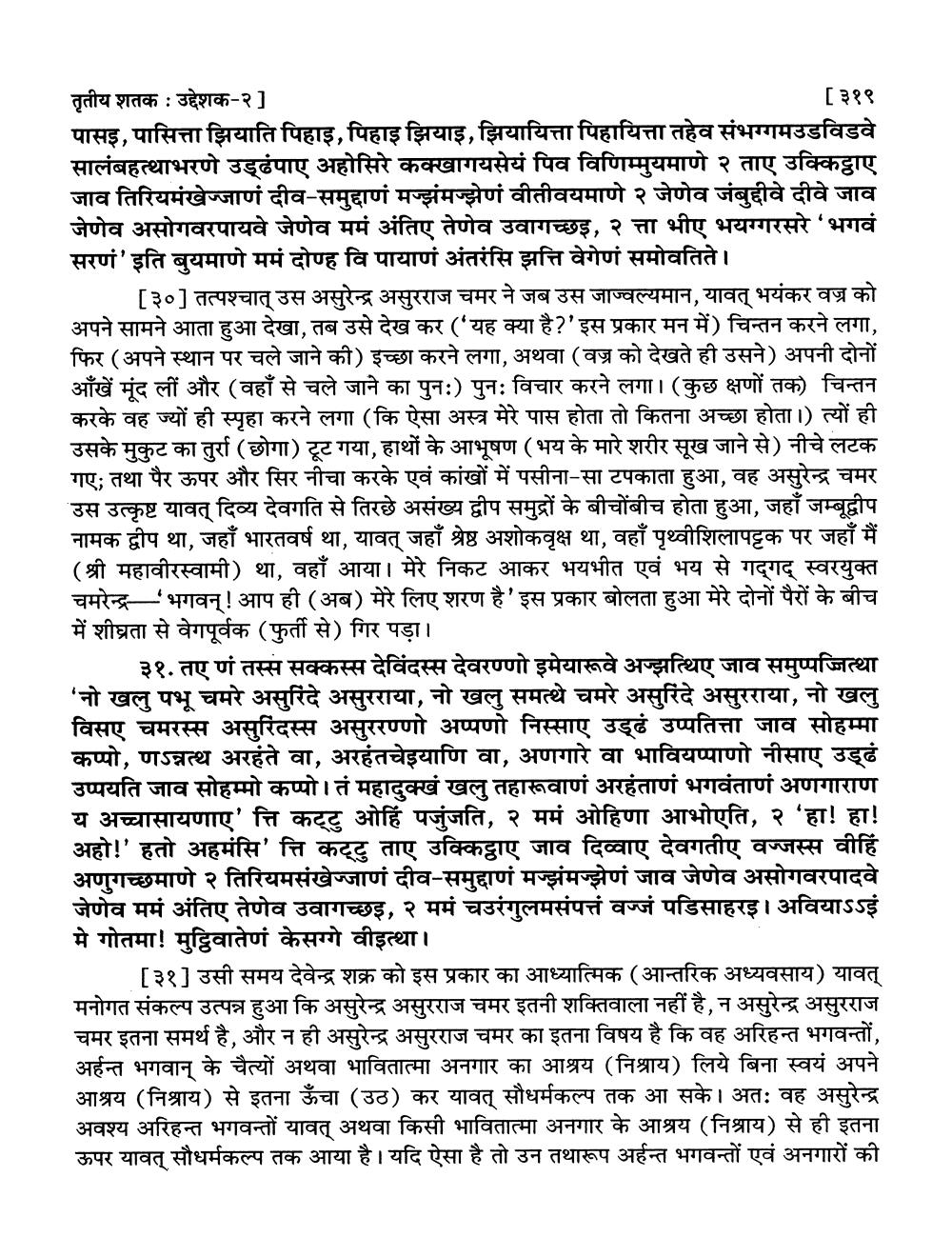________________
तृतीय शतक : उद्देशक - २]
[ ३१९
पासइ, पासित्ता झियाति पिहाड़, पिहाड़ झियाइ, झियायित्ता पिहायित्ता तहेव संभग्गमउडविडवे सालंबहत्थाभरणे उड्ढपाए अहोसिरे कक्खागयसेयं पिव विणिम्मुयमाणे २ ताए उक्किट्ठाए जव तिरियमंखेज्जाणं दीव-समुद्दाणं मज्झमज्झेणं वीतीवयमाणे २ जेणेव जंबुद्दीवे दीवे जाव जेणेव असोगवरपायवे जेणेव ममं अंतिए तेणेव उवागच्छइ, २ त्ता भीए भयग्गरसरे 'भगवं सरणं' इति बुयमाणे ममं दोण्ह वि पायाणं अंतरंसि झत्ति वेगेणं समोवतिते ।
[३०] तत्पश्चात् उस असुरेन्द्र असुरराज चमर ने जब उस जाज्वल्यमान, यावत् भयंकर वज्र को अपने सामने आता हुआ देखा, तब उसे देख कर ('यह क्या है ? ' इस प्रकार मन में) चिन्तन करने लगा, फिर (अपने स्थान पर चले जाने की) इच्छा करने लगा, अथवा (वज्र को देखते ही उसने) अपनी दोनों आँखें मूंद लीं और ( वहाँ से चले जाने का पुन:) पुन: विचार करने लगा। (कुछ क्षणों तक) चिन्तन करके वह ज्यों ही स्पृहा करने लगा (कि ऐसा अस्त्र मेरे पास होता तो कितना अच्छा होता ।) त्यों ही उसके मुकुट का तुर्रा (छोगा) टूट गया, हाथों के आभूषण (भय के मारे शरीर सूख जाने से) नीचे लटक गए; तथा पैर ऊपर और सिर नीचा करके एवं कांखों में पसीना - सा टपकाता हुआ, वह असुरेन्द्र चमर उस उत्कृष्ट यावत् दिव्य देवगति से तिरछे असंख्य द्वीप समुद्रों के बीचोंबीच होता हुआ, जहाँ जम्बूद्वीप नामक द्वीप था, जहाँ भारतवर्ष था, यावत् जहाँ श्रेष्ठ अशोकवृक्ष था, वहाँ पृथ्वीशिलापट्टक पर जहाँ मैं (श्री महावीरस्वामी) था, वहाँ आया । मेरे निकट आकर भयभीत एवं भय से गद्गद् स्वरयुक्त चमरेन्द्र — 'भगवन् ! आप ही (अब) मेरे लिए शरण है' इस प्रकार बोलता हुआ मेरे दोनों पैरों के बीच में शीघ्रता से वेगपूर्वक (फुर्ती से) गिर पड़ा।
३१. तए णं तस्स सक्कस्स देविंदस्स देवरण्णो इमेयारूवे अज्झत्थिए जाव समुप्पज्जित्था 'नो खलु पभू चमरे असुरिंदे असुरराया, नो खलु समत्थे चमरे असुरिंदे असुरराया, नो खलु विसए चमरस्स असुरिंदस्स असुररण्णो अप्पणो निस्साए उड्ढं उप्पतित्ता जाव सोहम्मा कप्पो, णन्नत्थ अरहंते वा, अरहंतचेइयाणि वा, अणगारे वा भावियप्पाणो नीसाए उड्ढ उप्पयति जाव सोहम्मो कप्पो । तं महादुक्खं खलु तहारूवाणं अरहंताणं भगवंताणं अणगाराण य अच्चासायणाए' त्ति कट्टु ओहिं पजुंजति, २ ममं ओहिणा आभोएति, २ 'हा! हा! अहो !' हतो अहमंसि' त्ति कट्टु ताए उक्किट्ठाए जाव दिव्वाए देवगतीए वज्जस्स वीहिं अणुगच्छमाणे २ तिरियमसंखेज्जाणं दीव - समुद्दाणं मज्झमज्झेणं जाव जेणेव असोगवरपादवे जेणेव ममं अंतिए तेणेव उवागच्छइ, २ ममं चउरंगुलमसंपत्तं वज्जं पडिसाहरइ । अवियाऽऽइं मे गोतमा! मुट्ठिवाणं केसग्गे वीइत्था ।
[३१] उसी समय देवेन्द्र शक्र को इस प्रकार का आध्यात्मिक ( आन्तरिक अध्यवसाय) यावत् मनोगत संकल्प उत्पन्न हुआ कि असुरेन्द्र असुरराज चमर इतनी शक्तिवाला नहीं है, न असुरेन्द्र असुरराज चमर इतना समर्थ है, और न ही असुरेन्द्र असुरराज चमर का इतना विषय है कि वह अरिहन्त भगवन्तों, अर्हन्त भगवान् के चैत्यों अथवा भावितात्मा अनगार का आश्रय (निश्राय) लिये बिना स्वयं अपने आश्रय (निश्राय) से इतना ऊँचा (उठ) कर यावत् सौधर्मकल्प तक आ सके । अतः वह असुरेन्द्र अवश्य अरिहन्त भगवन्तों यावत् अथवा किसी भावितात्मा अनगार के आश्रय (निश्राय) से ही इतना ऊपर यावत् सौधर्मकल्प तक आया है । यदि ऐसा है तो उन तथारूप अर्हन्त भगवन्तों एवं अनगारों की