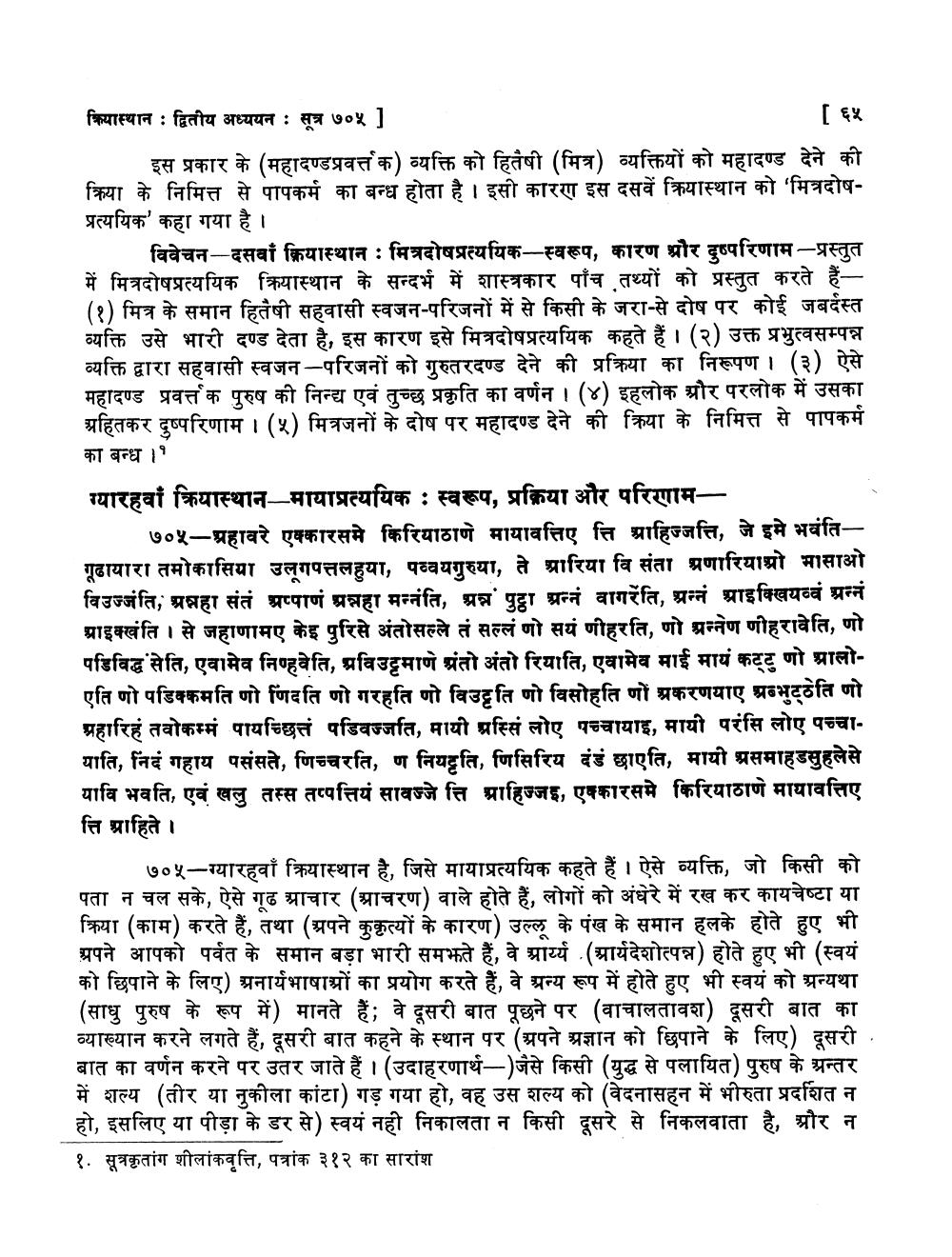________________
क्रियास्थान : द्वितीय अध्ययन : सूत्र ७०५ ]
[६५ इस प्रकार के (महादण्डप्रवर्तक) व्यक्ति को हितैषी (मित्र) व्यक्तियों को महादण्ड देने की क्रिया के निमित्त से पापकर्म का बन्ध होता है । इसी कारण इस दसवें क्रियास्थान को 'मित्रदोषप्रत्ययिक' कहा गया है।
विवेचन-दसवां क्रियास्थान : मित्रदोषप्रत्ययिक-स्वरूप, कारण और दुष्परिणाम-प्रस्तुत में मित्रदोषप्रत्ययिक क्रियास्थान के सन्दर्भ में शास्त्रकार पाँच तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं(१) मित्र के समान हितैषी सहवासी स्वजन-परिजनों में से किसी के जरा-से दोष पर कोई जबर्दस्त व्यक्ति उसे भारी दण्ड देता है, इस कारण इसे मित्रदोषप्रत्ययिक कहते हैं । (२) उक्त प्रभुत्वसम्पन्न व्यक्ति द्वारा सहवासी स्वजन-परिजनों को गुरुतरदण्ड देने की प्रक्रिया का निरूपण । (३) ऐसे महादण्ड प्रवर्तक पुरुष की निन्द्य एवं तुच्छ प्रकृति का वर्णन । (४) इहलोक और परलोक में उसका अहितकर दुष्परिणाम । (५) मित्रजनों के दोष पर महादण्ड देने की क्रिया के निमित्त से पापकर्म का बन्ध।' ग्यारहवां क्रियास्थान-मायाप्रत्ययिक : स्वरूप, प्रक्रिया और परिणाम
७०५-प्रहावरे एक्कारसमे किरियाठाणे मायावत्तिए त्ति पाहिज्जत्ति, जे इमे भवंतिगूढायारा तमोकासिया उलगपत्तलहुया, पव्वयगुरुया, ते प्रारिया वि संता प्रणारियाप्रो भासाओ विउज्जति, अन्नहा संतं अप्पाणं अन्नहा मन्नंति, अन्नपुट्ठा अन्नं वागरेंति, अन्नं प्राइक्खियव्वं अन्नं प्राइक्खंति । से जहाणामए केइ पुरिसे अंतोसल्ले तं सल्लं णो सयं णीहरति, णो अन्नेण णीहरावेति, णो पडिविद्ध सेति, एवामेव निण्हवेति, प्रविउट्टमाणे अंतो अंतो रियाति, एवामेव माई मायं कटु णो पालोएति णो पडिक्कमति णो णिदति णो गरहति णो विउदृति णो विसोहति णों प्रकरणयाए अन्भुट्ठति णो प्रहारिहं तवोकम्मं पायच्छित्तं पडिवज्जति, मायी प्रस्सिं लोए पच्चायाइ, मायी परंसि लोए पच्चा. याति, निदं गहाय पसंसते, णिच्चरति, ण नियट्टति, णिसिरिय दंडं छाएति, मायो असमाहडसुहलेसे यावि भवति, एवं खलु तस्स तप्पत्तियं सावज्जे त्ति पाहिज्जइ, एक्कारसमे किरियाठाणे मायावत्तिए त्ति प्राहिते।
७०५-ग्यारहवाँ क्रियास्थान है, जिसे मायाप्रत्ययिक कहते हैं । ऐसे व्यक्ति, जो किसी को पता न चल सके, ऐसे गूढ आचार (आचरण) वाले होते हैं, लोगों को अंधेरे में रख कर कायचेष्टा या क्रिया (काम) करते हैं, तथा (अपने कुकृत्यों के कारण) उल्लू के पंख के समान हलके होते हुए भी अपने आपको पर्वत के समान बड़ा भारी समझते हैं, वे आर्य .(आर्यदेशोत्पन्न होते हुए भी (स्वयं को छिपाने के लिए) अनार्यभाषाओं का प्रयोग करते हैं, वे अन्य रूप में होते हुए भी स्वयं को अन्यथा (साधु पुरुष के रूप में) मानते हैं; वे दूसरी बात पूछने पर (वाचालतावश) दूसरी बात का व्याख्यान करने लगते हैं, दूसरी बात कहने के स्थान पर (अपने अज्ञान को छिपाने के लिए) दूसरी . बात का वर्णन करने पर उतर जाते हैं । (उदाहरणार्थ-)जैसे किसी (युद्ध से पलायित) पुरुष के अन्तर में शल्य (तीर या नुकीला कांटा) गड़ गया हो, वह उस शल्य को (वेदनासहन में भीरुता प्रदर्शित न हो, इसलिए या पीड़ा के डर से) स्वयं नही निकालता न किसी दूसरे से निकलवाता है, और न १. सूत्रकृतांग शीलांकवृत्ति, पत्रांक ३१२ का सारांश