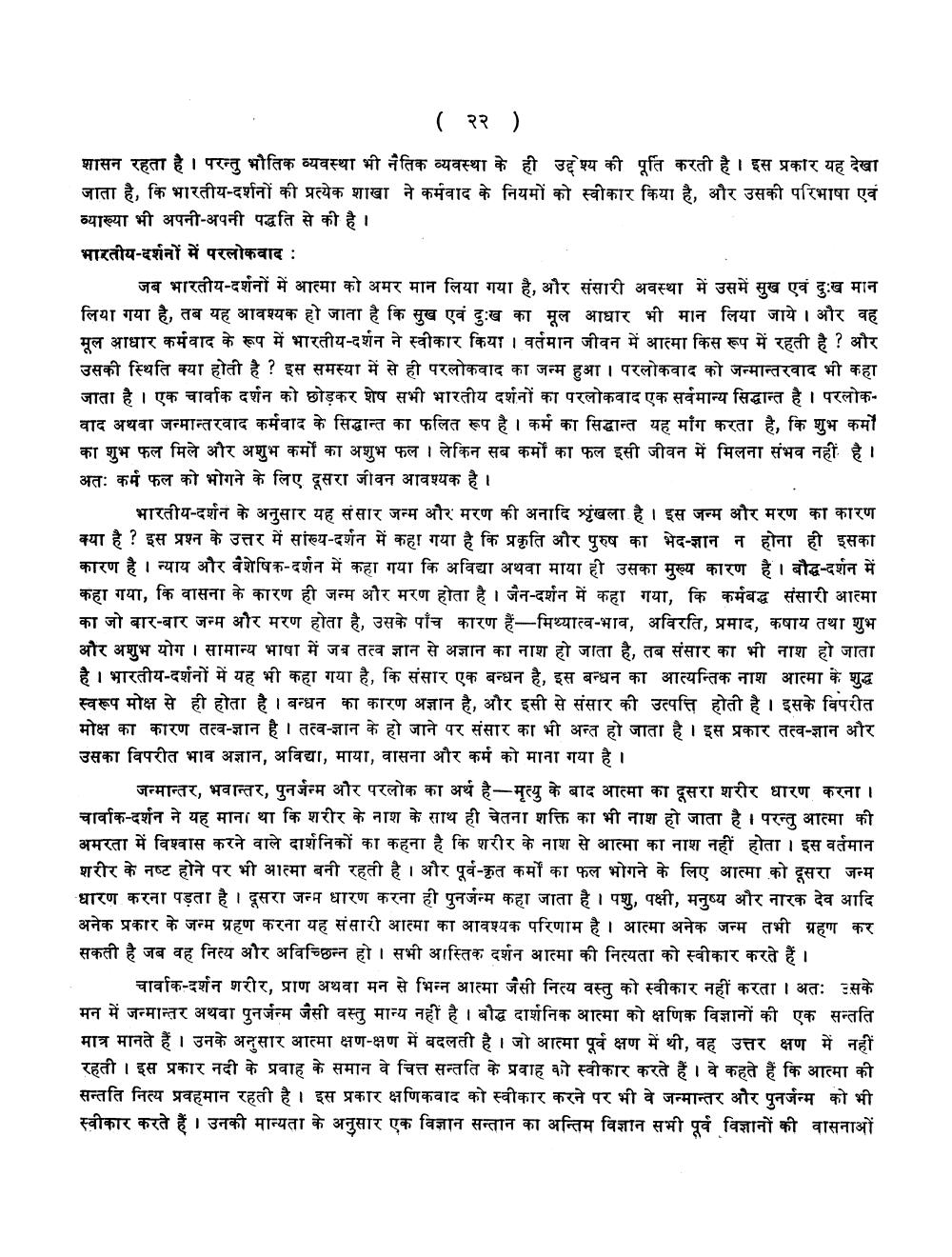________________
( २२ )
शासन रहता है । परन्तु भौतिक व्यवस्था भी नैतिक व्यवस्था के ही उद्देश्य की पूर्ति करती है । इस प्रकार यह देखा जाता है, कि भारतीय-दर्शनों की प्रत्येक शाखा ने कर्मवाद के नियमों को स्वीकार किया है, और उसकी परिभाषा एवं व्याख्या भी अपनी-अपनी पद्धति से की है। भारतीय-दर्शनों में परलोकवाद :
जब भारतीय-दर्शनों में आत्मा को अमर मान लिया गया है, और संसारी अवस्था में उसमें सुख एवं दुःख मान लिया गया है, तब यह आवश्यक हो जाता है कि सुख एवं दुःख का मूल आधार भी मान लिया जाये । और वह
द के रूप में भारतीय-दर्शन ने स्वीकार किया। वर्तमान जीवन में आत्मा किस रूप में रहती है ? और उसकी स्थिति क्या होती है ? इस समस्या में से ही परलोकवाद का जन्म हुआ। परलोकवाद को जन्मान्तरवाद भी कहा जाता है। एक चार्वाक दर्शन को छोड़कर शेष सभी भारतीय दर्शनों का परलोकवाद एक सर्वमान्य सिद्धान्त है। परलोकवाद अथवा जन्मान्तरवाद कर्मवाद के सिद्धान्त का फलित रूप है। कर्म का सिद्धान्त यह मांग करता है, कि शुभ कर्मों का शुभ फल मिले और अशुभ कर्मों का अशुभ फल । लेकिन सब कर्मों का फल इसी जीवन में मिलना संभव नहीं है। अतः कर्म फल को भोगने के लिए दूसरा जीवन आवश्यक है। भारतीय-दर्शन के अनुसार यह संसार जन्म और मरण की अनादि शृंखला है। इस जन्म और मरण का कारण
के उत्तर में सांख्य-दर्शन में कहा गया है कि प्रकृति और पुरुष का भेद-ज्ञान न होना ही इसका कारण है । न्याय और वैशेषिक-दर्शन में कहा गया कि अविद्या अथवा माया ही उसका मुख्य कारण है । बौद्ध-दर्शन में कहा गया, कि वासना के कारण ही जन्म और मरण होता है । जैन-दर्शन में कहा गया, कि कर्मबद्ध संसारी आत्मा का जो बार-बार जन्म और मरण होता है, उसके पाँच कारण हैं-मिथ्यात्व-भाव, अविरति, प्रमाद, कषाय तथा शुभ और अशुभ योग । सामान्य भाषा में जब तत्व ज्ञान से अज्ञान का नाश हो जाता है, तब संसार का भी नाश हो जाता है। भारतीय-दर्शनों में यह भी कहा गया है, कि संसार एक बन्धन है, इस बन्धन का आत्यन्तिक नाश आत्मा के शुद्ध स्वरूप मोक्ष से ही होता है । बन्धन का कारण अज्ञान है, और इसी से संसार की उत्पत्ति होती है। इसके विपरीत मोक्ष का कारण तत्व-ज्ञान है । तत्व-ज्ञान के हो जाने पर संसार का भी अन्त हो जाता है । इस प्रकार तत्व-ज्ञान और उसका विपरीत भाव अज्ञान, अविद्या, माया, वासना और कर्म को माना गया है।
जन्मान्तर, भवान्तर, पुनर्जन्म और परलोक का अर्थ है-मृत्यु के बाद आत्मा का दूसरा शरीर धारण करना । चार्वाक-दर्शन ने यह माना था कि शरीर के नाश के साथ ही चेतना शक्ति का भी नाश हो जाता है। परन्तु आत्मा की अमरता में विश्वास करने वाले दार्शनिकों का कहना है कि शरीर के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता। इस वर्तमान शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा बनी रहती है । और पूर्व-कृत कर्मों का फल भोगने के लिए आत्मा को दूसरा जन्म धारण करना पड़ता है । दूसरा जन्म धारण करना ही पुनर्जन्म कहा जाता है। पशु, पक्षी, मनुष्य और नारक देव आदि अनेक प्रकार के जन्म ग्रहण करना यह संसारी आत्मा का आवश्यक परिणाम है। आत्मा अनेक जन्म तभी ग्रहण कर सकती है जब वह नित्य और अविच्छिन्न हो । सभी आस्तिक दर्शन आत्मा की नित्यता को स्वीकार करते हैं।
चार्वाक-दर्शन शरीर, प्राण अथवा मन से भिन्न आत्मा जैसी नित्य वस्तु को स्वीकार नहीं करता । अतः उसके मन में जन्मान्तर अथवा पुनर्जन्म जैसी वस्तु मान्य नहीं है । बौद्ध दार्शनिक आत्मा को क्षणिक विज्ञानों की एक सन्तति मात्र मानते हैं । उनके अनुसार आत्मा क्षण-क्षण में बदलती है । जो आत्मा पूर्व क्षण में थी, वह उत्तर क्षण में नहीं रहती । इस प्रकार नदी के प्रवाह के समान वे चित्त सन्तति के प्रवाह को स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा की सन्तति नित्य प्रवहमान रहती है। इस प्रकार क्षणिकवाद को स्वीकार करने पर भी वे जन्मान्तर और पुनर्जन्म को भी स्वीकार करते हैं। उनकी मान्यता के अनुसार एक विज्ञान सन्तान का अन्तिम विज्ञान सभी पूर्व विज्ञानों की वासनाओं