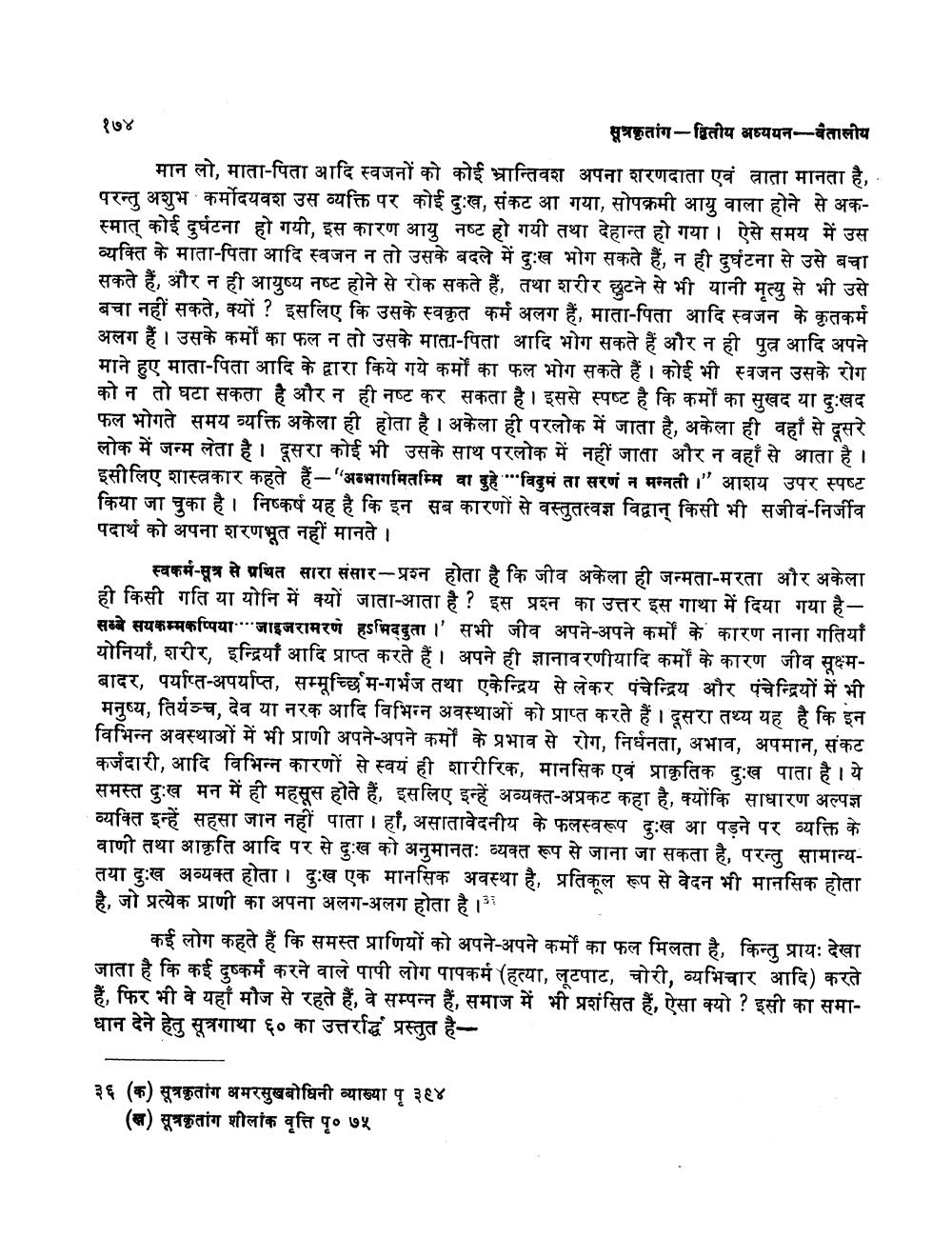________________
१७४
सूत्रकृतांग-द्वितीय अध्ययन-बैतालीय
__ मान लो, माता-पिता आदि स्वजनों को कोई भ्रान्तिवश अपना शरणदाता एवं त्राता मानता है, परन्तु अशुभ कर्मोदयवश उस व्यक्ति पर कोई दुःख, संकट आ गया, सोपक्रमी आयु वाला होने से अकस्मात् कोई दुर्घटना हो गयी, इस कारण आयु नष्ट हो गयी तथा देहान्त हो गया। ऐसे समय में उस व्यक्ति के माता-पिता आदि स्वजन न तो उसके बदले में दुःख भोग सकते हैं, न ही दुर्घटना से उसे बचा सकते हैं, और न ही आयुष्य नष्ट होने से रोक सकते हैं, तथा शरीर छुटने से भी यानी मृत्यु से भी उसे बचा नहीं सकते, क्यों? इसलिए कि उसके स्वकृत कर्म अलग हैं, माता-पिता आदि स्वजन के कृतकर्म अलग हैं। उसके कर्मों का फल न तो उसके माता-पिता आदि भोग सकते हैं और न ही पुत्र आदि अपने माने हए माता-पिता आदि के द्वारा किये गये कर्मों का फल भोग सकते हैं। कोई भी स्वजन उसके रोग को न तो घटा सकता है और न ही नष्ट कर सकता है। इससे स्पष्ट है कि कर्मों का सुखद या दुःखद फल भोगते समय व्यक्ति अकेला ही होता है । अकेला ही परलोक में जाता है, अकेला ही वहाँ से दूसरे लोक में जन्म लेता है। दूसरा कोई भी उसके साथ परलोक में नहीं जाता और न वहाँ से आता है। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं- "अब्भागमितम्मि वा दुहे "विदुमं ता सरणं न मन्नती।" आशय उपर स्पष्ट किया जा चुका है। निष्कर्ष यह है कि इन सब कारणों से वस्तुतत्वज्ञ विद्वान् किसी भी सजीव-निर्जीव पदार्थ को अपना शरणभूत नहीं मानते।
स्वकर्म-सूत्र से प्रथित सारा संसार-प्रश्न होता है कि जीव अकेला ही जन्मता-मरता और अकेला ही किसी गति या योनि में क्यों जाता-आता है ? इस प्रश्न का उत्तर इस गाथा में दिय सम्बे सयकम्मकप्पिया."जाइजरामरणे हऽभिदता ।' सभी जीव अपने-अपने कर्मों के कारण नाना गतियाँ योनियाँ, शरीर, इन्द्रियाँ आदि प्राप्त करते हैं। अपने ही ज्ञानावरणीयादि कर्मों के कारण जीव सूक्ष्मबादर, पर्याप्त-अपर्याप्त, सम्मूर्छिम-गर्भज तथा एकेन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रियों में भी मनुष्य, तिर्यञ्च, देव या नरक आदि विभिन्न अवस्थाओं को प्राप्त करते हैं। दूसरा तथ्य यह है कि इन विभिन्न अवस्थाओं में भी प्राणी अपने-अपने कर्मों के प्रभाव से रोग, निर्धनता, अभाव, अपमान, संकट कर्जदारी, आदि विभिन्न कारणों से स्वयं ही शारीरिक, मानसिक एवं प्राकृतिक दु:ख पाता है। ये समस्त दुःख मन में ही महसूस होते हैं, इसलिए इन्हें अव्यक्त-अप्रकट कहा है, क्योंकि साधारण अल्पज्ञ व्यक्ति इन्हें सहसा जान नहीं पाता। हाँ, असातावेदनीय के फलस्वरूप दुःख आ पड़ने पर व्यक्ति के वाणी तथा आकृति आदि पर से दुःख को अनुमानतः व्यक्त रूप से जाना जा सकता है, परन्तु सामान्यतया दुःख अव्यक्त होता। दुःख एक मानसिक अवस्था है, प्रतिकूल रूप से वेदन भी मानसिक होता है, जो प्रत्येक प्राणी का अपना अलग-अलग होता है।
कई लोग कहते हैं कि समस्त प्राणियों को अपने-अपने कर्मों का फल मिलता है, किन्तु प्रायः देखा जाता है कि कई दुष्कर्म करने वाले पापी लोग पापकर्म (हत्या, लूटपाट, चोरी, व्यभिचार आदि) करते हैं, फिर भी वे यहाँ मौज से रहते हैं, वे सम्पन्न हैं, समाज में भी प्रशंसित हैं, ऐसा क्यो ? इसी का समाधान देने हेतु सूत्रगाथा ६० का उत्तर्राद्ध प्रस्तुत है
३६ (क) सूत्रकृतांग अमरसुखबोधिनी व्याख्या पृ ३६४
(ख) सूत्रकृतांग शीलांक वृत्ति पृ० ७५