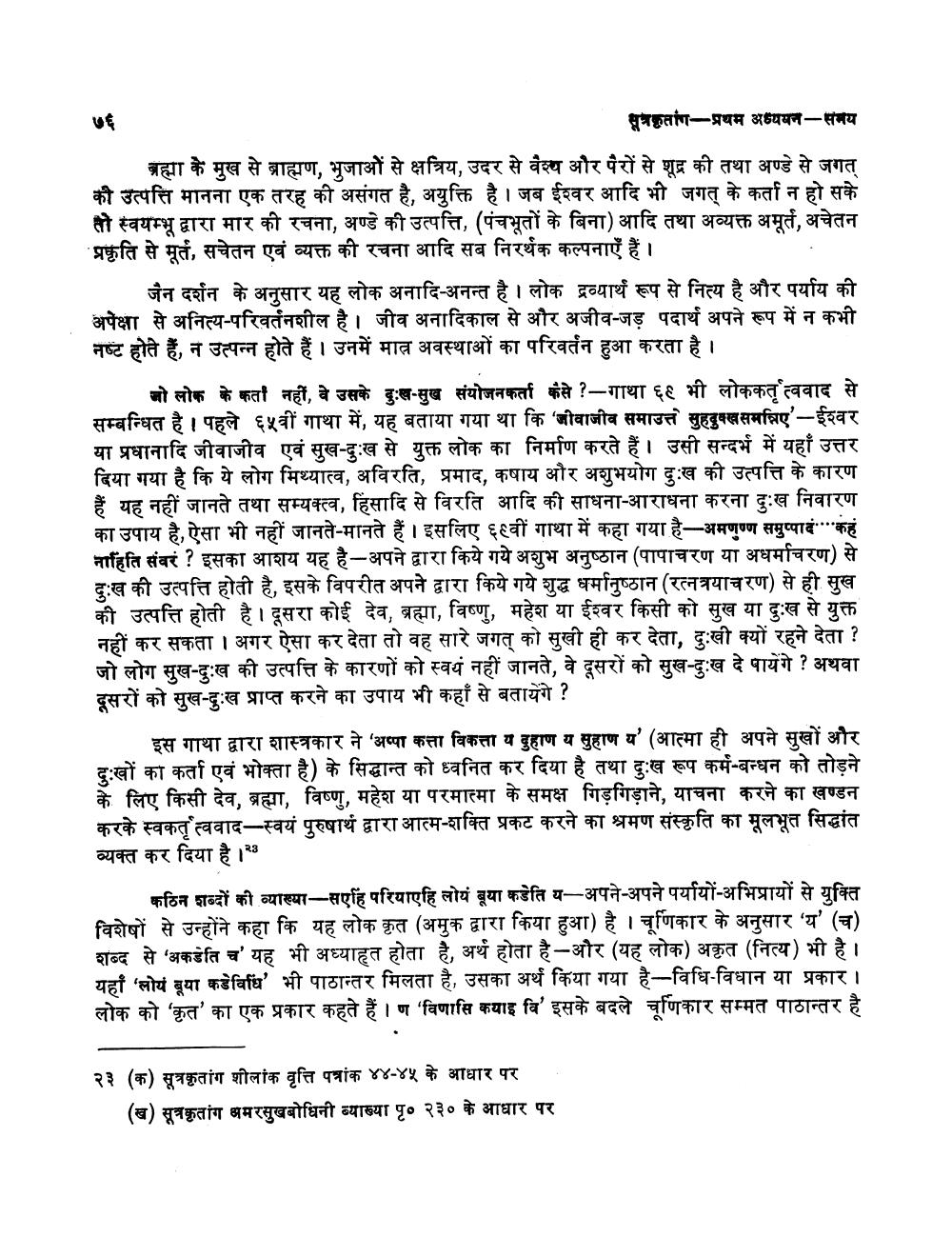________________
७६
सूत्रकृतांग-प्रथम अध्ययन-समय ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैरों से शूद्र की तथा अण्डे से जगत की उत्पत्ति मानना एक तरह की असंगत है, अयुक्ति है। जब ईश्वर आदि भी जगत् के कर्ता न हो सके तो स्वयम्भू द्वारा मार की रचना, अण्डे की उत्पत्ति, (पंचभूतों के बिना) आदि तथा अव्यक्त अमूर्त, अचेतन प्रकृति से मूर्त, सचेतन एवं व्यक्त की रचना आदि सब निरर्थक कल्पनाएँ हैं।
जैन दर्शन के अनुसार यह लोक अनादि-अनन्त है । लोक द्रव्यार्थ रूप से नित्य है और पर्याय की अपेक्षा से अनित्य-परिवर्तनशील है। जीव अनादिकाल से और अजीव-जड़ पदार्थ अपने रूप में न कभी नष्ट होते हैं, न उत्पन्न होते हैं। उनमें मात्र अवस्थाओं का परिवर्तन हुआ करता है।
___ जो लोक के कर्ता नहीं, वे उसके दुःख-सुख संयोजनकर्ता कैसे ?-गाथा ६६ भी लोककर्तृत्ववाद से सम्बन्धित है। पहले ६५वीं गाथा में, यह बताया गया था कि 'जीवाजीव समाउत्तं सुहदुक्खसमन्निए-ईश्वर या प्रधानादि जीवाजीव एवं सुख-दुःख से युक्त लोक का निर्माण करते हैं। उसी सन्दर्भ में यहाँ उत्तर दिया गया है कि ये लोग मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और अशुभयोग दुःख की उत्पत्ति के कारण हैं यह नहीं जानते तथा सम्यक्त्व, हिंसादि से विरति आदि की साधना-आराधना करना दुःख निवारण का उपाय है, ऐसा भी नहीं जानते-मानते हैं। इसलिए ६९वीं गाथा में कहा गया है-अमणुण्ण समुप्पादं कह नाहिति संवरं? इसका आशय यह है-अपने द्वारा किये गये अशुभ अनुष्ठान (पापाचरण या अधर्माचरण) से दुःख की उत्पत्ति होती है, इसके विपरीत अपने द्वारा किये गये शुद्ध धर्मानुष्ठान (रत्नत्रयाचरण) से ही सुख की उत्पत्ति होती है। दूसरा कोई देव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश या ईश्वर किसी को सुख या दुःख से युक्त नहीं कर सकता । अगर ऐसा कर देता तो वह सारे जगत् को सुखी ही कर देता, दुःखी क्यों रहने देता ? जो लोग सुख-दुःख की उत्पत्ति के कारणों को स्वयं नहीं जानते, वे दूसरों को सुख-दुःख दे पायेंगे? अथवा दूसरों को सुख-दुःख प्राप्त करने का उपाय भी कहाँ से बतायेंगे?
इस गाथा द्वारा शास्त्रकार ने 'अप्पा कत्ता विकत्ता य दुहाण य सुहाण य' (आत्मा ही अपने सुखों और दुःखों का कर्ता एवं भोक्ता है) के सिद्धान्त को ध्वनित कर दिया है तथा दुःख रूप कर्म-बन्धन को तोड़ने के लिए किसी देव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश या परमात्मा के समक्ष गिड़गिड़ाने, याचना करने का खण्डन करके स्वकर्तृत्ववाद-स्वयं पुरुषार्थ द्वारा आत्म-शक्ति प्रकट करने का श्रमण संस्कृति का मूलभूत सिद्धांत व्यक्त कर दिया है।
कठिन शब्दों की व्याख्या-सएहि परियाएहि लोयं बूया कडेति य-अपने-अपने पर्यायों-अभिप्रायों से युक्ति विशेषों से उन्होंने कहा कि यह लोक कृत (अमुक द्वारा किया हुआ) है । चूर्णिकार के अनुसार 'य' (च) शब्द से 'अकडेति च' यह भी अध्याहृत होता है, अर्थ होता है-और (यह लोक) अकृत (नित्य) भी है। यहाँ 'लोयं बूया कडेविधि' भी पाठान्तर मिलता है, उसका अर्थ किया गया है-विधि-विधान या प्रकार । लोक को 'कृत' का एक प्रकार कहते हैं । ण 'विणासि कयाइ वि' इसके बदले चूर्णिकार सम्मत पाठान्तर है
२३ (क) सूत्रकृतांग शीलांक वृत्ति पत्रांक ४४-४५ के आधार पर
(ख) सूत्रकृतांग अमरसुखबोधिनी ब्याख्या पृ० २३० के आधार पर