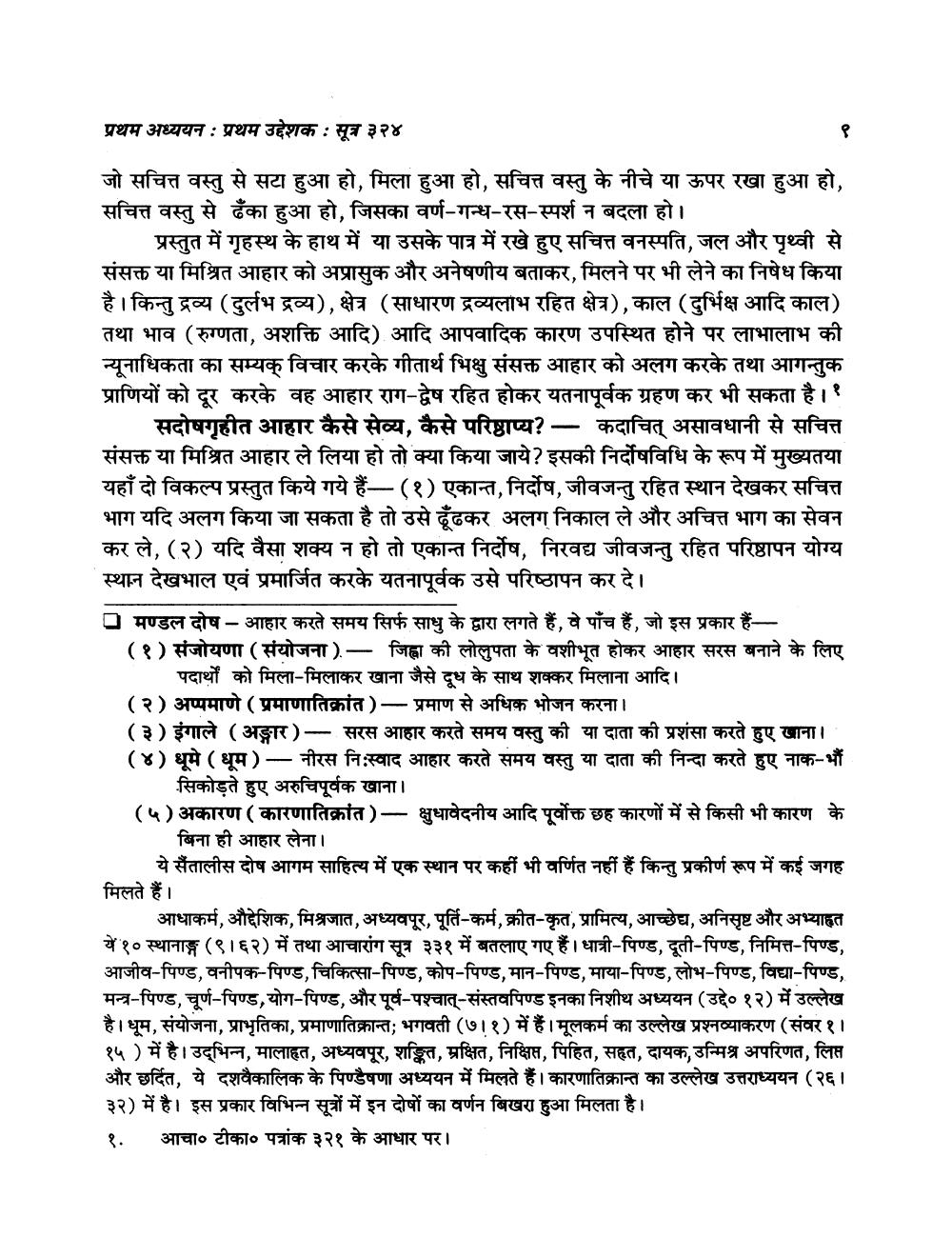________________
प्रथम अध्ययन : प्रथम उद्देशक: सूत्र ३२४
जो सचित्त वस्तु से सटा हुआ हो, मिला हुआ हो, सचित्त वस्तु के नीचे या ऊपर रखा हुआ हो, सचित्त वस्तु से ढंका हुआ हो, जिसका वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्श न बदला हो।
प्रस्तुत में गृहस्थ के हाथ में या उसके पात्र में रखे हुए सचित्त वनस्पति, जल और पृथ्वी से संसक्त या मिश्रित आहार को अप्रासुक और अनेषणीय बताकर, मिलने पर भी लेने का निषेध किया है। किन्तु द्रव्य (दुर्लभ द्रव्य), क्षेत्र (साधारण द्रव्यलाभ रहित क्षेत्र), काल (दुर्भिक्ष आदि काल) तथा भाव (रुग्णता, अशक्ति आदि) आदि आपवादिक कारण उपस्थित होने पर लाभालाभ की न्यूनाधिकता का सम्यक् विचार करके गीतार्थ भिक्षु संसक्त आहार को अलग करके तथा आगन्तुक प्राणियों को दूर करके वह आहार राग-द्वेष रहित होकर यतनापूर्वक ग्रहण कर भी सकता है।
सदोषगृहीत आहार कैसे सेव्य, कैसे परिष्ठाप्य? - कदाचित् असावधानी से सचित्त संसक्त या मिश्रित आहार ले लिया हो तो क्या किया जाये? इसकी निर्दोषविधि के रूप में मुख्यतया यहाँ दो विकल्प प्रस्तुत किये गये हैं-(१) एकान्त, निर्दोष, जीवजन्तु रहित स्थान देखकर सचित्त भाग यदि अलग किया जा सकता है तो उसे ढूँढकर अलग निकाल ले और अचित्त भाग का सेवन कर ले, (२) यदि वैसा शक्य न हो तो एकान्त निर्दोष, निरवद्य जीवजन्तु रहित परिष्ठापन योग्य स्थान देखभाल एवं प्रमार्जित करके यतनापूर्वक उसे परिष्ठापन कर दे। 0 मण्डल दोष - आहार करते समय सिर्फ साधु के द्वारा लगते हैं, वे पाँच हैं, जो इस प्रकार हैं(१) संजोयणा (संयोजना)- जिह्वा की लोलुपता के वशीभूत होकर आहार सरस बनाने के लिए
पदार्थों को मिला-मिलाकर खाना जैसे दूध के साथ शक्कर मिलाना आदि। (२) अप्पमाणे (प्रमाणातिक्रांत)-प्रमाण से अधिक भोजन करना। (३) इंगाले (अङ्गार)- सरस आहार करते समय वस्तु की या दाता की प्रशंसा करते हुए खाना। (४) धूमे (धूम)- नीरस निःस्वाद आहार करते समय वस्तु या दाता की निन्दा करते हुए नाक-भौं
सिकोड़ते हुए अरुचिपूर्वक खाना। (५) अकारण (कारणातिक्रांत)- क्षुधावेदनीय आदि पूर्वोक्त छह कारणों में से किसी भी कारण के
बिना ही आहार लेना।
ये सैंतालीस दोष आगम साहित्य में एक स्थान पर कहीं भी वर्णित नहीं हैं किन्तु प्रकीर्ण रूप में कई जगह मिलते हैं।
आधाकर्म, औद्देशिक, मिश्रजात, अध्यवपूर, पूर्ति-कर्म, क्रीत-कृत, प्रामित्य, आच्छेध, अनिसृष्ट और अभ्याहृत ये १० स्थानाङ्ग (९।६२) में तथा आचारांग सूत्र ३३१ में बतलाए गए हैं। धात्री-पिण्ड, दूती-पिण्ड, निमित्त-पिण्ड, आजीव-पिण्ड, वनीपक-पिण्ड,चिकित्सा-पिण्ड, कोप-पिण्ड, मान-पिण्ड, माया-पिण्ड, लोभ-पिण्ड, विद्या-पिण्ड, मन्त्र-पिण्ड, चूर्ण-पिण्ड, योग-पिण्ड, और पूर्व-पश्चात्-संस्तवपिण्ड इनका निशीथ अध्ययन (उद्दे० १२) में उल्लेख है। धूम, संयोजना, प्राभृतिका, प्रमाणातिक्रान्त; भगवती (७।१) में हैं। मूलकर्म का उल्लेख प्रश्नव्याकरण (संवर १। १५ ) में है। उद्भिन्न, मालाहृत, अध्यवपूर, शङ्कित, म्रक्षित, निक्षिप्त, पिहित, सहृत, दायक, उन्मिश्र अपरिणत, लिप्त और छर्दित, ये दशवैकालिक के पिण्डैषणा अध्ययन में मिलते हैं। कारणातिक्रान्त का उल्लेख उत्तराध्ययन (२६ । ३२) में है। इस प्रकार विभिन्न सूत्रों में इन दोषों का वर्णन बिखरा हुआ मिलता है। १. आचा० टीका० पत्रांक ३२१ के आधार पर।