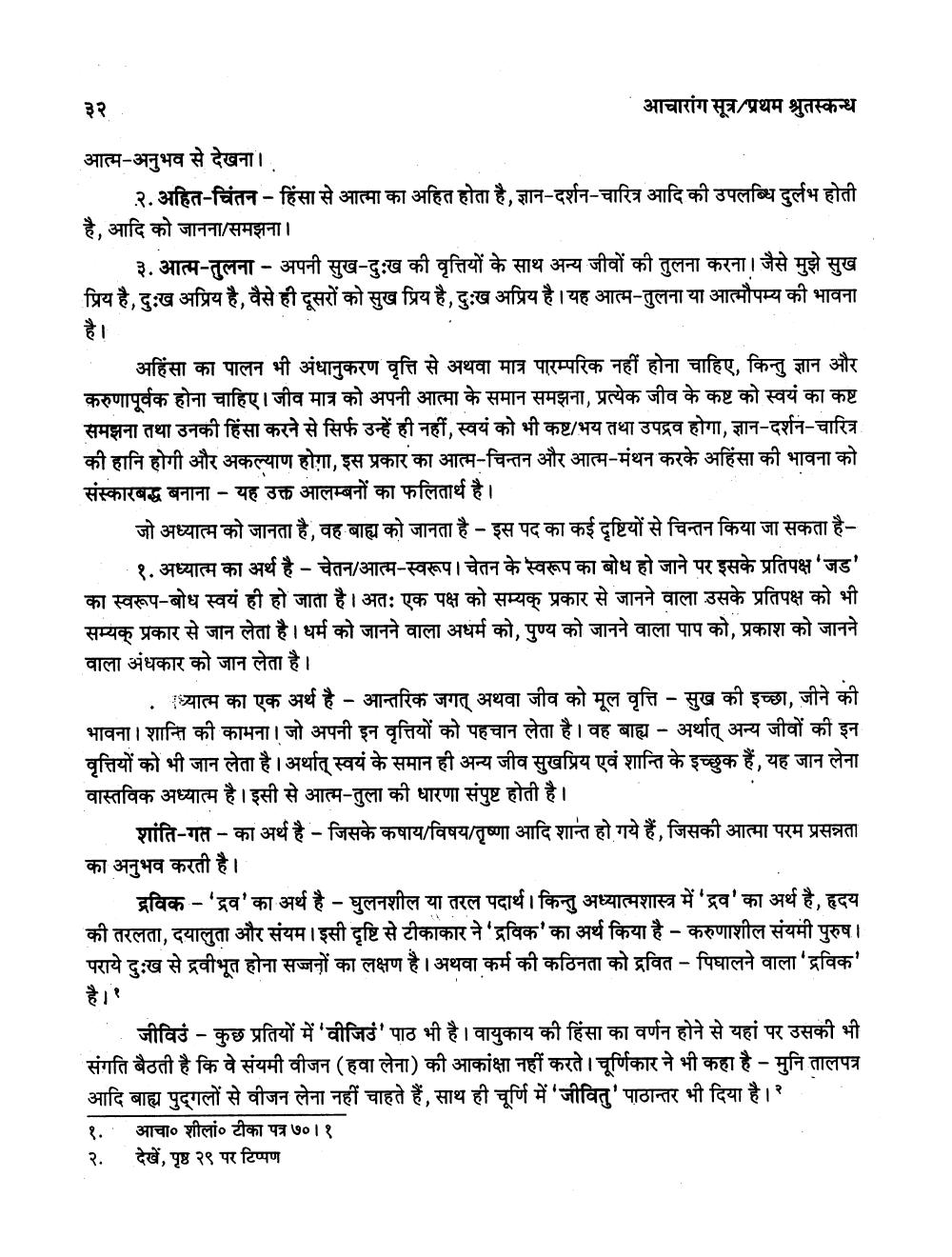________________
३२ .
आचारांग सूत्र/प्रथम श्रुतस्कन्ध
आत्म-अनुभव से देखना।
२.अहित-चिंतन - हिंसा से आत्मा का अहित होता है, ज्ञान-दर्शन-चारित्र आदि की उपलब्धि दुर्लभ होती है, आदि को जानना/समझना।
३. आत्म-तुलना - अपनी सुख-दुःख की वृत्तियों के साथ अन्य जीवों की तुलना करना। जैसे मुझे सुख प्रिय है, दुःख अप्रिय है, वैसे ही दूसरों को सुख प्रिय है, दुःख अप्रिय है । यह आत्म-तुलना या आत्मौपम्य की भावना
- अहिंसा का पालन भी अंधानुकरण वृत्ति से अथवा मात्र पारम्परिक नहीं होना चाहिए, किन्तु ज्ञान और करुणापूर्वक होना चाहिए। जीव मात्र को अपनी आत्मा के समान समझना, प्रत्येक जीव के कष्ट को स्वयं का कष्ट समझना तथा उनकी हिंसा करने से सिर्फ उन्हें ही नहीं, स्वयं को भी कष्ट/भय तथा उपद्रव होगा, ज्ञान-दर्शन-चारित्र की हानि होगी और अकल्याण होगा, इस प्रकार का आत्म-चिन्तन और आत्म-मंथन करके अहिंसा की भावना को संस्कारबद्ध बनाना - यह उक्त आलम्बनों का फलितार्थ है।
जो अध्यात्म को जानता है, वह बाह्य को जानता है - इस पद का कई दृष्टियों से चिन्तन किया जा सकता है
१. अध्यात्म का अर्थ है - चेतन/आत्म-स्वरूप। चेतन के स्वरूप का बोध हो जाने पर इसके प्रतिपक्ष 'जड' का स्वरूप-बोध स्वयं ही हो जाता है। अतः एक पक्ष को सम्यक् प्रकार से जानने वाला उसके प्रतिपक्ष को भी सम्यक् प्रकार से जान लेता है। धर्म को जानने वाला अधर्म को, पुण्य को जानने वाला पाप को, प्रकाश को जानने वाला अंधकार को जान लेता है।
.रध्यात्म का एक अर्थ है - आन्तरिक जगत् अथवा जीव को मूल वृत्ति - सुख की इच्छा, जीने की भावना। शान्ति की कामना । जो अपनी इन वृत्तियों को पहचान लेता है। वह बाह्य - अर्थात् अन्य जीवों की इन वृत्तियों को भी जान लेता है। अर्थात् स्वयं के समान ही अन्य जीव सुखप्रिय एवं शान्ति के इच्छुक हैं, यह जान लेना वास्तविक अध्यात्म है। इसी से आत्म-तुला की धारणा संपुष्ट होती है।
__ शांति-गत - का अर्थ है - जिसके कषाय/विषय/तृष्णा आदि शान्त हो गये हैं, जिसकी आत्मा परम प्रसन्नता का अनुभव करती है।
द्रविक - 'द्रव' का अर्थ है - घुलनशील या तरल पदार्थ। किन्तु अध्यात्मशास्त्र में 'द्रव' का अर्थ है, हृदय की तरलता, दयालुता और संयम । इसी दृष्टि से टीकाकार ने 'द्रविक' का अर्थ किया है - करुणाशील संयमी पुरुष । पराये दुःख से द्रवीभूत होना सज्जनों का लक्षण है । अथवा कर्म की कठिनता को द्रवित - पिघालने वाला 'द्रविक'
- जीविठं - कुछ प्रतियों में 'वीजिउं' पाठ भी है। वायुकाय की हिंसा का वर्णन होने से यहां पर उसकी भी संगति बैठती है कि वे संयमी वीजन (हवा लेना) की आकांक्षा नहीं करते। चूर्णिकार ने भी कहा है - मुनि तालपत्र आदि बाह्य पुद्गलों से वीजन लेना नहीं चाहते हैं, साथ ही चूर्णि में 'जीवितु' पाठान्तर भी दिया है। १. आचा० शीला टीका पत्र ७०।१ २. देखें, पृष्ठ २९ पर टिप्पण