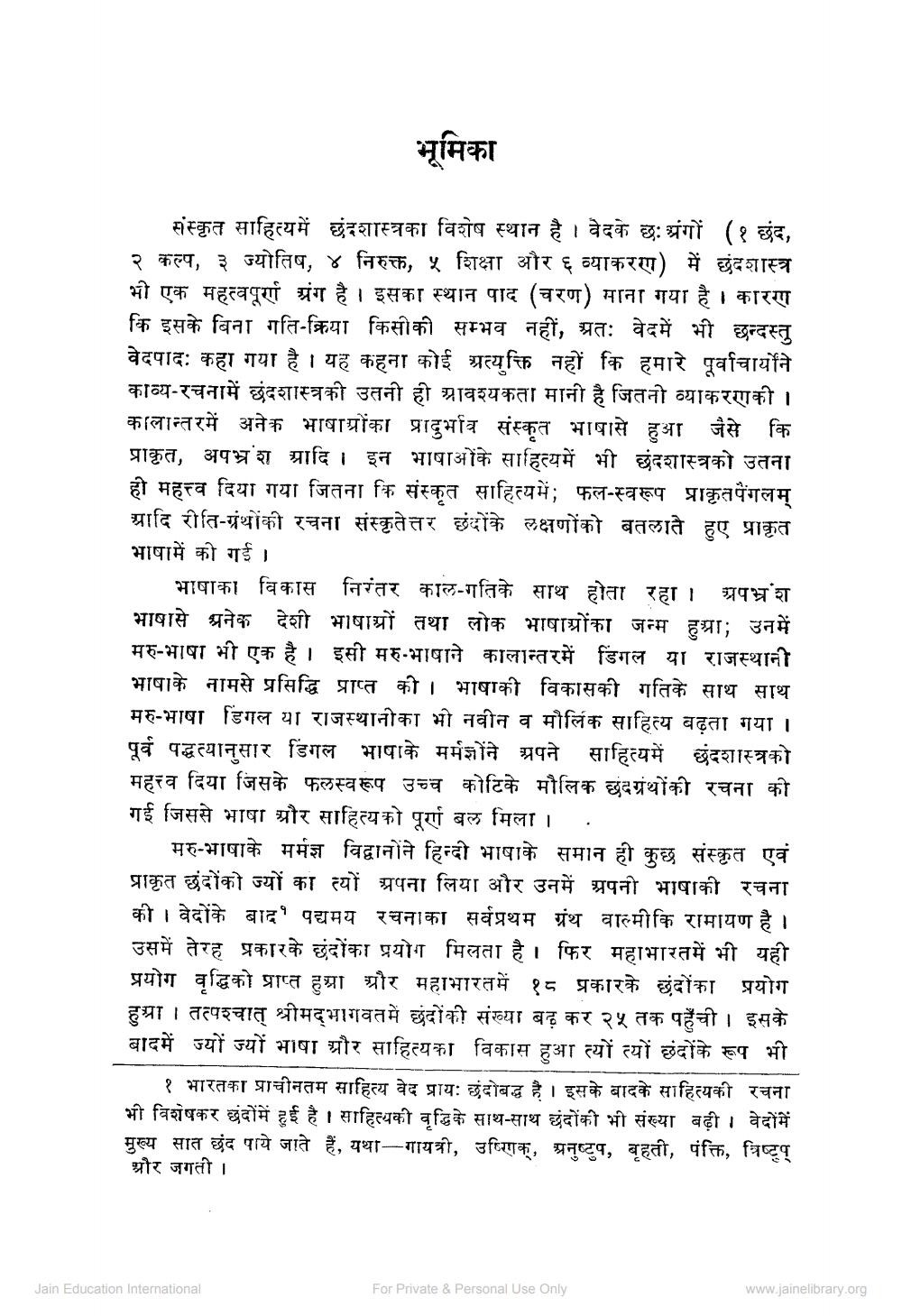________________
भूमिका
संस्कृत साहित्यमें छंदशास्त्रका विशेष स्थान है । वेदके छः अंगों (१ छंद, २ कल्प, ३ ज्योतिष, ४ निरुक्त, ५ शिक्षा और ६ व्याकरण) में छंदशास्त्र भी एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका स्थान पाद (चरण) माना गया है । कारण कि इसके बिना गति-क्रिया किसीकी सम्भव नहीं, अतः वेदमें भी छन्दस्तु वेदपाद: कहा गया है । यह कहना कोई अत्युक्ति नहीं कि हमारे पूर्वाचार्योने काव्य-रचनामें छंदशास्त्रकी उतनी ही आवश्यकता मानी है जितनी व्याकरणकी। कालान्तरमें अनेक भाषागोंका प्रादुर्भाव संस्कृत भाषासे हुआ जैसे कि प्राकृत, अपभ्रश अादि । इन भाषाओंके साहित्यमें भी छंदशास्त्रको उतना ही महत्त्व दिया गया जितना कि संस्कृत साहित्य में ; फल-स्वरूप प्राकृतपैगलम् आदि रीति-ग्रंथोंकी रचना संस्कृतेत्तर छंदोंके लक्षणोंको बतलाते हुए प्राकृत भाषामें की गई।
भाषाका विकास निरंतर काल-गतिके साथ होता रहा। अपभ्रंश भाषासे अनेक देशी भाषाओं तथा लोक भाषाओंका जन्म हुआ; उनमें मरु-भाषा भी एक है। इसी मरु-भाषाने कालान्तरमें डिंगल या राजस्थानी भाषाके नामसे प्रसिद्धि प्राप्त की। भाषाकी विकासको गतिके साथ साथ मरु-भाषा डिंगल या राजस्थानीका भो नवीन व मौलिक साहित्य बढ़ता गया । पूर्व पद्धत्यानुसार डिंगल भाषाके मर्मज्ञोंने अपने साहित्यमें छंदशास्त्रको महत्त्व दिया जिसके फलस्वरूप उच्च कोटिके मौलिक छंदग्रंथों की रचना की गई जिससे भाषा और साहित्य को पूर्ण बल मिला। .
मरु-भाषाके मर्मज्ञ विद्वानोंने हिन्दी भाषाके समान ही कुछ संस्कृत एवं प्राकृत छंदोंको ज्यों का त्यों अपना लिया और उनमें अपनी भाषाकी रचना की। वेदोंके बाद' पद्यमय रचनाका सर्वप्रथम ग्रंथ वाल्मीकि रामायण है। उसमें तेरह प्रकारके छंदोंका प्रयोग मिलता है। फिर महाभारतमें भी यही प्रयोग वृद्धिको प्राप्त हुआ और महाभारतमें १८ प्रकारके छंदोंका प्रयोग हुअा। तत्पश्चात् श्रीमद्भागवतमें छंदों की संख्या बढ़ कर २५ तक पहुँची। इसके बादमें ज्यों ज्यों भाषा और साहित्यका विकास हुआ त्यों त्यों छंदोंके रूप भी
१ भारतका प्राचीनतम साहित्य वेद प्रायः छंदोबद्ध है । इसके बादके साहित्यकी रचना भी विशेषकर छंदोंमें हुई है । साहित्यकी वृद्धि के साथ-साथ छंदोंकी भी संख्या बढ़ी। वेदोंमें मुख्य सात छंद पाये जाते हैं, यथा-गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहती, पंक्ति, त्रिष्टुप् और जगती।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org