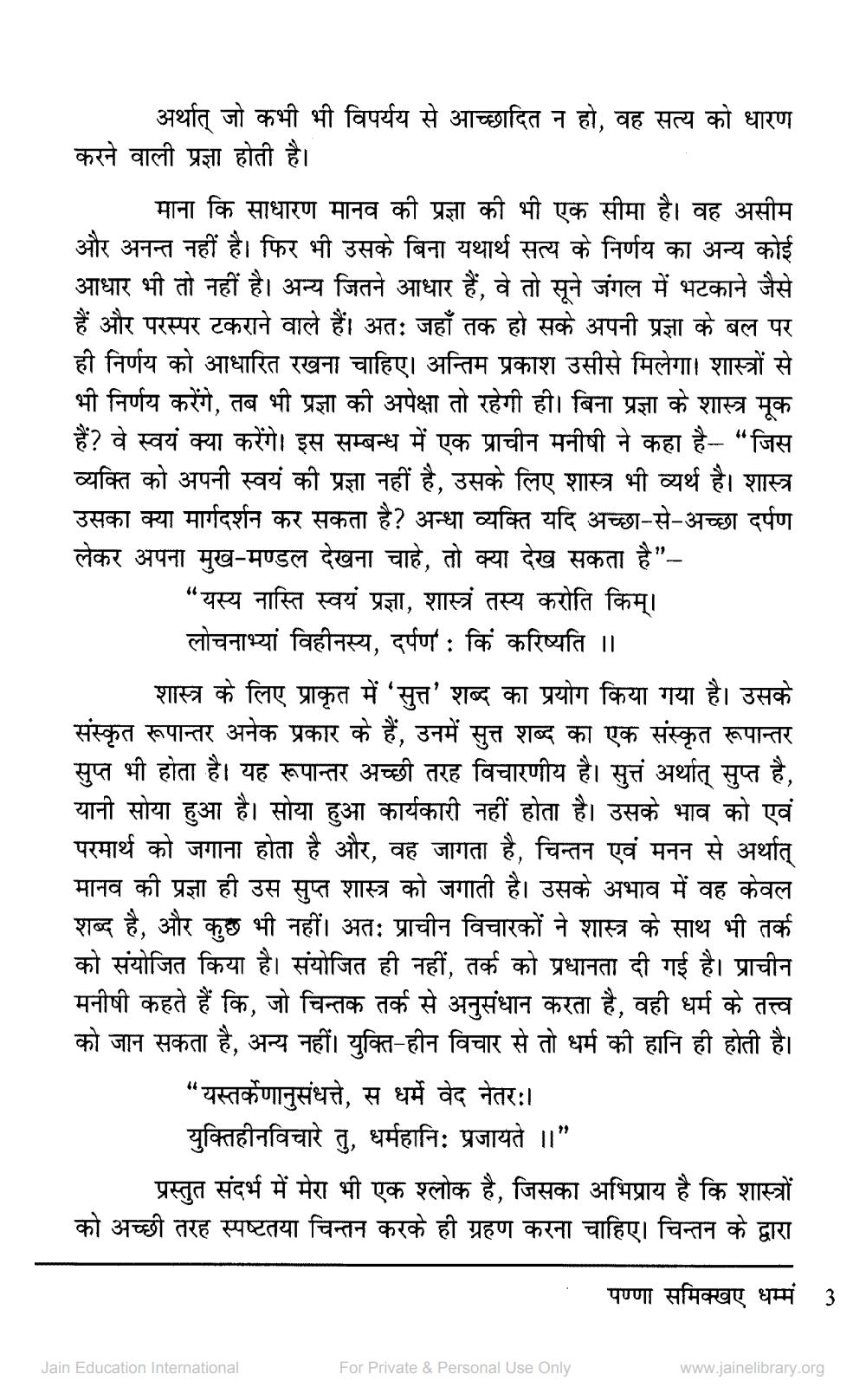________________
अर्थात् जो कभी भी विपर्यय से आच्छादित न हो, वह सत्य को धारण करने वाली प्रज्ञा होती है।
माना कि साधारण मानव की प्रज्ञा की भी एक सीमा है। वह असीम और अनन्त नहीं है। फिर भी उसके बिना यथार्थ सत्य के निर्णय का अन्य कोई आधार भी तो नहीं है। अन्य जितने आधार हैं, वे तो सूने जंगल में भटकाने जैसे हैं और परस्पर टकराने वाले हैं। अतः जहाँ तक हो सके अपनी प्रज्ञा के बल पर ही निर्णय को आधारित रखना चाहिए | अन्तिम प्रकाश उसीसे मिलेगा। शास्त्रों से भी निर्णय करेंगे, तब भी प्रज्ञा की अपेक्षा तो रहेगी ही। बिना प्रज्ञा के शास्त्र मूक हैं? वे स्वयं क्या करेंगे। इस सम्बन्ध में एक प्राचीन मनीषी ने कहा है- “ जिस व्यक्ति को अपनी स्वयं की प्रज्ञा नहीं है, उसके लिए शास्त्र भी व्यर्थ है। शास्त्र उसका क्या मार्गदर्शन कर सकता है? अन्धा व्यक्ति यदि अच्छा-से-अच्छा दर्पण लेकर अपना मुख मण्डल देखना चाहे, तो क्या देख सकता है"
" यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, शास्त्रं तस्य करोति किम् । लोचनाभ्यां विहीनस्य, दर्पण : किं करिष्यति ।।
शास्त्र के लिए प्राकृत में 'सुत्त' शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके संस्कृत रूपान्तर अनेक प्रकार के हैं, उनमें सुत्त शब्द का एक संस्कृत रूपान्तर सुप्त भी होता है। यह रूपान्तर अच्छी तरह विचारणीय है। सुत्तं अर्थात् सुप्त है, यानी सोया हुआ है। सोया हुआ कार्यकारी नहीं होता है। उसके भाव को एवं परमार्थ को जगाना होता है और वह जागता है, चिन्तन एवं मनन से अर्थात् मानव की प्रज्ञा ही उस सुप्त शास्त्र को जगाती है। उसके अभाव में वह केवल शब्द है, और कुछ भी नहीं । अतः प्राचीन विचारकों ने शास्त्र के साथ भी तर्क को संयोजित किया है। संयोजित ही नहीं, तर्क को प्रधानता दी गई है। प्राचीन मनीषी कहते हैं कि, जो चिन्तक तर्क से अनुसंधान करता है, वही धर्म के तत्त्व को जान सकता है, अन्य नहीं । युक्ति - हीन विचार से तो धर्म की हानि ही होती है।
“यस्तर्केणानुसंधत्ते, स धर्मे वेद नेतरः । युक्तिहीनविचारे तु धर्महानिः प्रजायते ।। "
प्रस्तुत संदर्भ में मेरा भी एक श्लोक है, जिसका अभिप्राय है कि शास्त्रों को अच्छी तरह स्पष्टतया चिन्तन करके ही ग्रहण करना चाहिए । चिन्तन के द्वारा
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
पण्णा समिक्ख धम्मं
3
www.jainelibrary.org