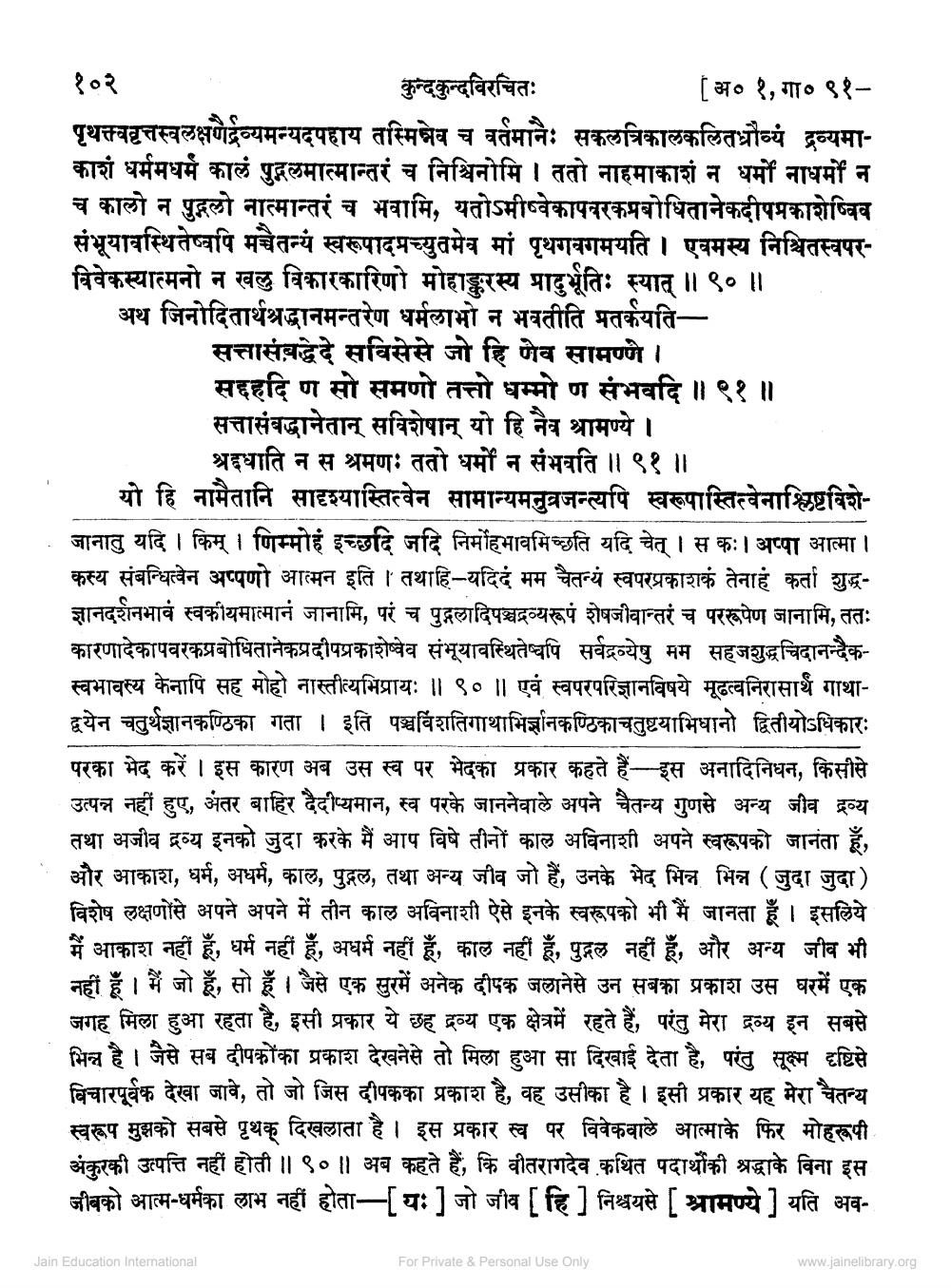________________
१०२
कुन्दकुन्दविरचितः
[अ० १, गा० ९१पृथक्त्ववृत्तस्वलक्षणैर्द्रव्यमन्यदपहाय तस्मिन्नेव च वर्तमानैः सकलत्रिकालकलितध्रौव्यं द्रव्यमाकाशं धर्ममधर्म कालं पुद्गलमात्मान्तरं च निश्चिनोमि । ततो नाहमाकाशं न धर्मों नाधर्मों न च कालो न पुद्गलो नात्मान्तरं च भवामि, यतोऽमीष्वेकापवरकप्रबोधितानेकदीपप्रकाशेष्विव संभूयावस्थितेष्वपि मचैतन्य स्वरूपादमच्युतमेव मां पृथगवगमयति । एवमस्य निश्चितस्वपरविवेकस्यात्मनो न खलु विकारकारिणो मोहाङ्करस्य प्रादुर्भूतिः स्यात् ।। ९० ॥ अथ जिनोदितार्थश्रद्धानमन्तरेण धर्मलाभो न भवतीति प्रतर्कयति
सत्तासंबद्धदे सविसेसे जो हि व सामण्णे । सद्दहदि ण सो समणो तत्तो धम्मो ण संभवदि ॥ ९१ ॥ सत्तासंबद्धानेतान् सविशेषान् यो हि नैव श्रामण्ये ।
श्रद्दधाति न स श्रमणः ततो धर्मों न संभवति ।। ९१ ॥ यो हि नामैतानि सादृश्यास्तित्वेन सामान्यमनुव्रजन्त्यपि स्वरूपास्तित्वेनाश्लिष्टविशेजानातु यदि । किम् । णिम्मोहं इच्छदि जदि निर्मोहभावमिच्छति यदि चेत् । स कः। अप्पा आत्मा । कस्य संबन्धित्वेन अप्पणो आत्मन इति । तथाहि-यदिदं मम चैतन्यं स्वपरप्रकाशकं तेनाहं कर्ता शुद्धज्ञानदर्शनभावं स्वकीयमात्मानं जानामि, परं च पुद्गलादिपञ्चद्रव्यरूपं शेषजीवान्तरं च पररूपेण जानामि, ततः कारणादेकापवरकप्रबोधितानेकप्रदीपप्रकाशेष्वेव संभूयावस्थितेष्वपि सर्वद्रव्येषु मम सहजशुद्धचिदानन्दैकस्वभावस्य केनापि सह मोहो नास्तीत्यभिप्रायः ॥ ९० ॥ एवं स्वपरपरिज्ञानविषये मूढत्वनिरासार्थ गाथाद्वयेन चतुर्थज्ञानकण्ठिका गता । इति पञ्चविंशतिगाथाभिर्ज्ञानकण्ठिकाचतुष्टयाभिधानो द्वितीयोऽधिकारः परका भेद करें । इस कारण अब उस स्व पर भेदका प्रकार कहते हैं-इस अनादिनिधन, किसीसे उत्पन्न नहीं हुए, अंतर बाहिर दैदीप्यमान, स्व परके जाननेवाले अपने चैतन्य गुणसे अन्य जीव द्रव्य तथा अजीव द्रव्य इनको जुदा करके मैं आप विषे तीनों काल अविनाशी अपने स्वरूपको जानता हूँ,
और आकाश, धर्म, अधर्म, काल, पुद्गल, तथा अन्य जीव जो हैं, उनके भेद भिन्न भिन्न (जुदा जुदा) विशेष लक्षणोंसे अपने अपने में तीन काल अविनाशी ऐसे इनके स्वरूपको भी मैं जानता हूँ । इसलिये मैं आकाश नहीं हूँ, धर्म नहीं हूँ, अधर्म नहीं हूँ, काल नहीं हूँ, पुद्गल नहीं हूँ, और अन्य जीव भी नहीं हूँ। मैं जो हूँ, सो हूँ। जैसे एक सुरमें अनेक दीपक जलानेसे उन सबका प्रकाश उस घरमें एक जगह मिला हुआ रहता है, इसी प्रकार ये छह द्रव्य एक क्षेत्रमें रहते हैं, परंतु मेरा द्रव्य इन सबसे भिन्न है । जैसे सब दीपकोंका प्रकाश देखनेसे तो मिला हुआ सा दिखाई देता है, परंतु सूक्ष्म दृष्टिसे विचारपूर्वक देखा जावे, तो जो जिस दीपकका प्रकाश है, वह उसीका है । इसी प्रकार यह मेरा चैतन्य स्वरूप मुझको सबसे पृथक् दिखलाता है। इस प्रकार स्व पर विवेकवाले आत्माके फिर मोहरूपी अंकुरकी उत्पत्ति नहीं होती ॥ ९० ॥ अब कहते हैं, कि वीतरागदेव कथित पदार्थोकी श्रद्धाके विना इस जीबको आत्म-धर्मका लाभ नहीं होता-[यः] जो जीव [हि ] निश्चयसे [श्रामण्ये ] यति अव
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org