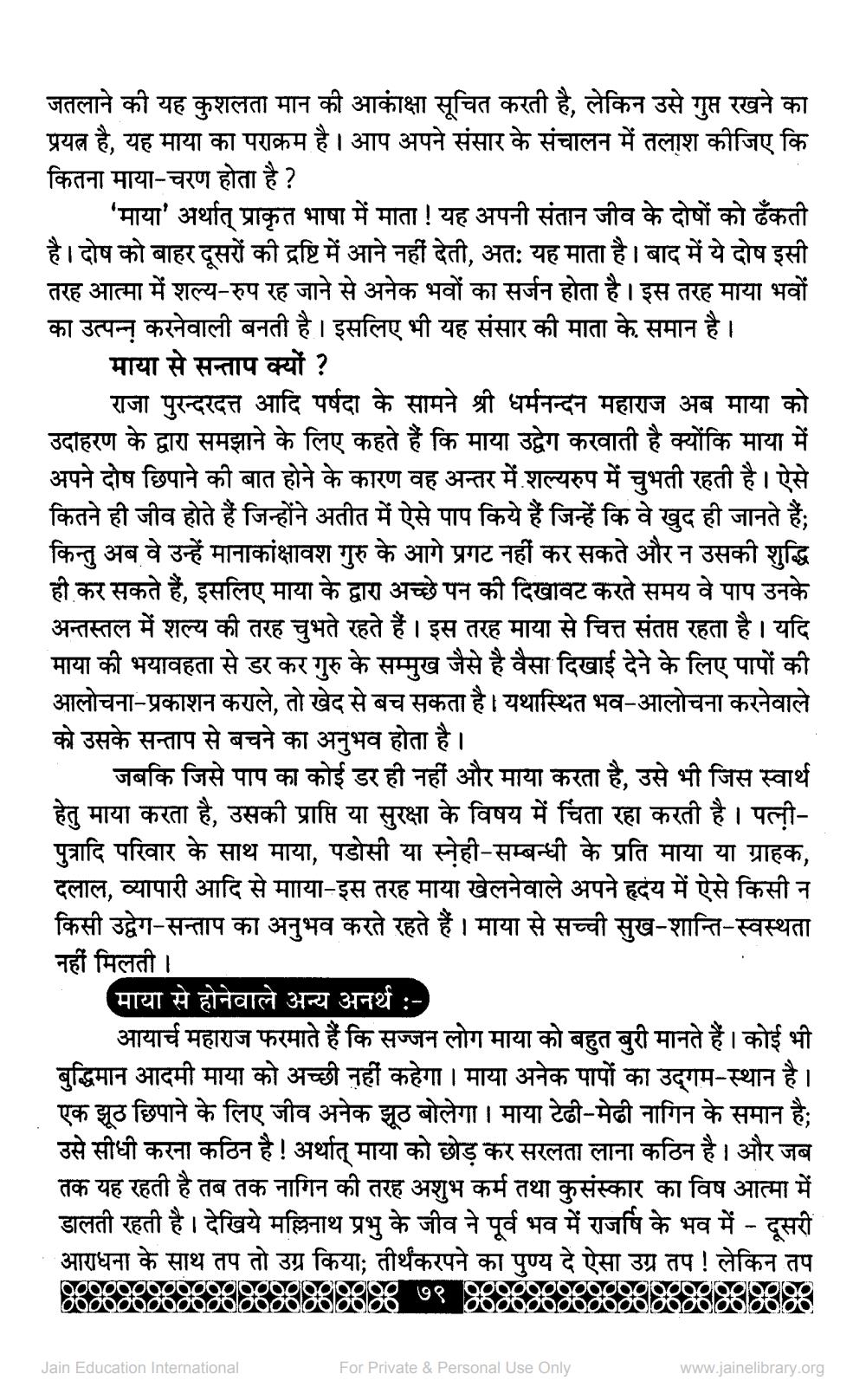________________
जतलाने की यह कुशलता मान की आकाक्षा सूचित करती है, लेकिन उसे गुप्त रखने का प्रयत्न है, यह माया का पराक्रम है। आप अपने संसार के संचालन में तलाश कीजिए कि कितना माया-चरण होता है ?
_ 'माया' अर्थात् प्राकृत भाषा में माता ! यह अपनी संतान जीव के दोषों को ढंकती है। दोष को बाहर दूसरों की द्रष्टि में आने नहीं देती, अत: यह माता है। बाद में ये दोष इसी तरह आत्मा में शल्य-रुप रह जाने से अनेक भवों का सर्जन होता है। इस तरह माया भवों का उत्पन्न करनेवाली बनती है। इसलिए भी यह संसार की माता के समान है।
माया से सन्ताप क्यों ?
राजा पुरन्दरदत्त आदि पर्षदा के सामने श्री धर्मनन्दन महाराज अब माया को उदाहरण के द्वारा समझाने के लिए कहते हैं कि माया उद्वेग करवाती है क्योंकि माया में अपने दोष छिपाने की बात होने के कारण वह अन्तर में शल्यरुप में चुभती रहती है। ऐसे कितने ही जीव होते हैं जिन्होंने अतीत में ऐसे पाप किये हैं जिन्हें कि वे खुद ही जानते हैं; किन्तु अब वे उन्हें मानाकांक्षावश गुरु के आगे प्रगट नहीं कर सकते और न उसकी शुद्धि ही कर सकते हैं, इसलिए माया के द्वारा अच्छे पन की दिखावट करते समय वे पाप उनके अन्तस्तल में शल्य की तरह चुभते रहते हैं। इस तरह माया से चित्त संतप्त रहता है। यदि माया की भयावहता से डर कर गुरु के सम्मुख जैसे है वैसा दिखाई देने के लिए पापों की आलोचना-प्रकाशन कराले, तो खेद से बच सकता है। यथास्थित भव-आलोचना करनेवाले को उसके सन्ताप से बचने का अनुभव होता है।
जबकि जिसे पाप का कोई डर ही नहीं और माया करता है, उसे भी जिस स्वार्थ हेतु माया करता है, उसकी प्राप्ति या सुरक्षा के विषय में चिंता रहा करती है। पत्नीपुत्रादि परिवार के साथ माया, पडोसी या स्नेही-सम्बन्धी के प्रति माया या ग्राहक, दलाल, व्यापारी आदि से माया-इस तरह माया खेलनेवाले अपने हृदय में ऐसे किसी न किसी उद्वेग-सन्ताप का अनुभव करते रहते हैं । माया से सच्ची सुख-शान्ति-स्वस्थता नहीं मिलती।
माया से होनेवाले अन्य अनर्थ :
आयार्च महाराज फरमाते हैं कि सज्जन लोग माया को बहुत बुरी मानते हैं। कोई भी बुद्धिमान आदमी माया को अच्छी नहीं कहेगा। माया अनेक पापों का उद्गम-स्थान है। एक झूठ छिपाने के लिए जीव अनेक झूठ बोलेगा। माया टेढी-मेढी नागिन के समान है; उसे सीधी करना कठिन है ! अर्थात् माया को छोड़ कर सरलता लाना कठिन है। और जब तक यह रहती है तब तक नागिन की तरह अशुभ कर्म तथा कुसंस्कार का विष आत्मा में डालती रहती है। देखिये मल्लिनाथ प्रभु के जीव ने पूर्व भव में राजर्षि के भव में - दूसरी आराधना के साथ तप तो उग्र किया; तीर्थंकरपने का पुण्य दे ऐसा उग्र तप ! लेकिन तप
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org