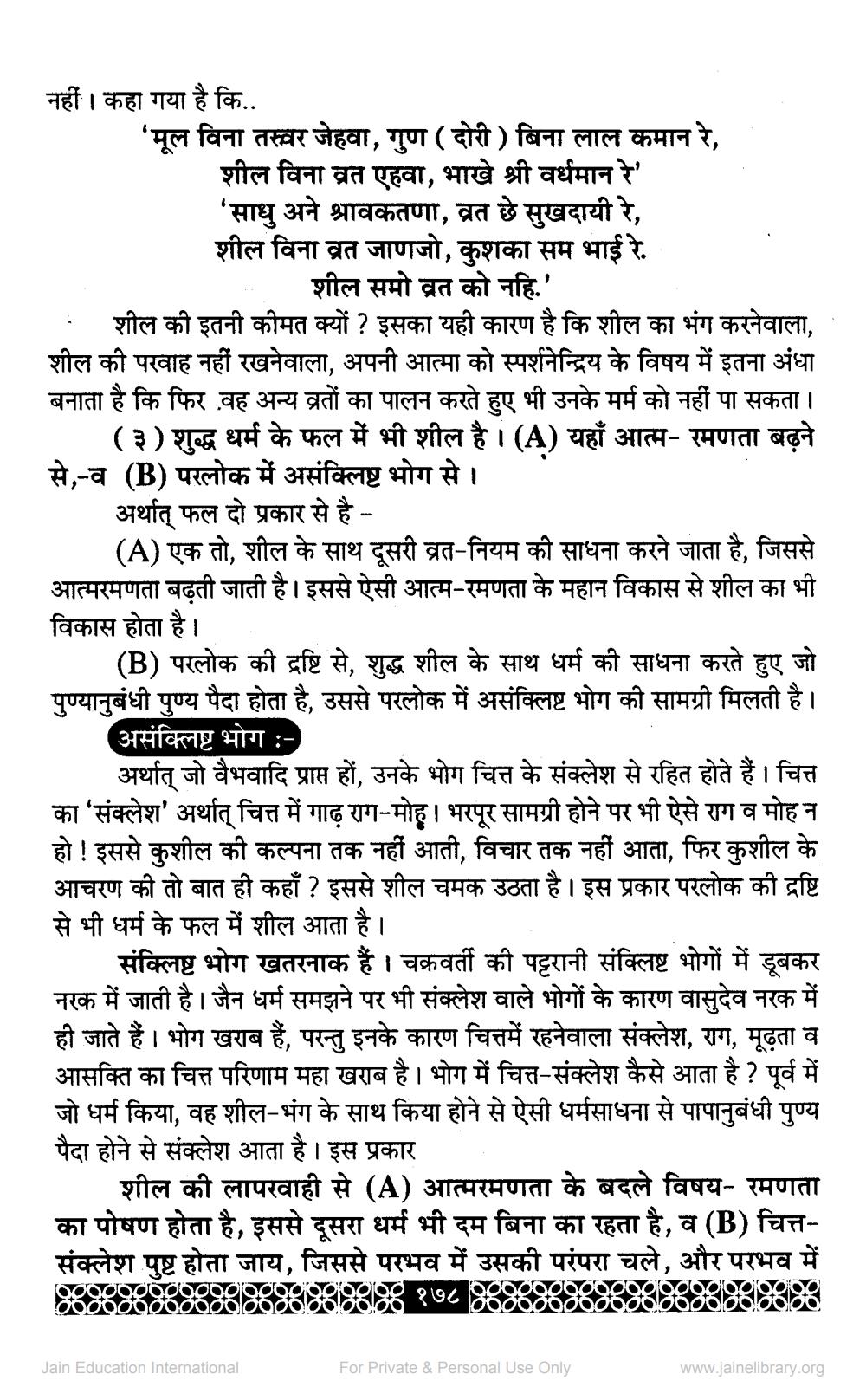________________
नहीं । कहा गया है कि.. 'मूल विना तस्वर जेहवा, गुण (दोरी) बिना लाल कमान रे,
शील विना व्रत एहवा, भाखे श्री वर्धमान रे' 'साधु अने श्रावकतणा, व्रत छ सुखदायी रे, शील विना व्रत जाणजो, कुशका सम भाई रे.
- शील समो व्रत को नहि.' . शील की इतनी कीमत क्यों ? इसका यही कारण है कि शील का भंग करनेवाला, . शील की परवाह नहीं रखनेवाला, अपनी आत्मा को स्पर्शनेन्द्रिय के विषय में इतना अंधा बनाता है कि फिर वह अन्य व्रतों का पालन करते हुए भी उनके मर्म को नहीं पा सकता।
(३) शुद्ध धर्म के फल में भी शील है । (A) यहाँ आत्म- रमणता बढ़ने से,-व (B) परलोक में असंक्लिष्ट भोग से।।
अर्थात् फल दो प्रकार से है -
(A) एक तो, शील के साथ दूसरी व्रत-नियम की साधना करने जाता है, जिससे आत्मरमणता बढ़ती जाती है। इससे ऐसी आत्म-रमणता के महान विकास से शील का भी विकास होता है।
(B) परलोक की द्रष्टि से, शुद्ध शील के साथ धर्म की साधना करते हुए जो पुण्यानुबंधी पुण्य पैदा होता है, उससे परलोक में असंक्लिष्ट भोग की सामग्री मिलती है।
असंक्लिष्ट भोग :
अर्थात् जो वैभवादि प्राप्त हों, उनके भोग चित्त के संक्लेश से रहित होते हैं। चित्त का 'संक्लेश' अर्थात् चित्त में गाढ़ राग-मोह । भरपूर सामग्री होने पर भी ऐसे राग व मोह न हो ! इससे कुशील की कल्पना तक नहीं आती, विचार तक नहीं आता, फिर कुशील के आचरण की तो बात ही कहाँ ? इससे शील चमक उठता है। इस प्रकार परलोक की द्रष्टि से भी धर्म के फल में शील आता है।
संक्लिष्ट भोग खतरनाक हैं । चक्रवर्ती की पट्टरानी संक्लिष्ट भोगों में डूबकर नरक में जाती है। जैन धर्म समझने पर भी संक्लेश वाले भोगों के कारण वासुदेव नरक में ही जाते हैं। भोग खराब हैं, परन्तु इनके कारण चित्तमें रहनेवाला संक्लेश, राग, मूढ़ता व आसक्ति का चित्त परिणाम महा खराब है। भोग में चित्त-संक्लेश कैसे आता है ? पूर्व में जो धर्म किया, वह शील-भंग के साथ किया होने से ऐसी धर्मसाधना से पापानुबंधी पुण्य पैदा होने से संक्लेश आता है। इस प्रकार
शील की लापरवाही से (A) आत्मरमणता के बदले विषय- रमणता का पोषण होता है, इससे दूसरा धर्म भी दम बिना का रहता है, व (B) चित्तसंक्लेश पुष्ट होता जाय, जिससे परभव में उसकी परंपरा चले, और परभव में
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org