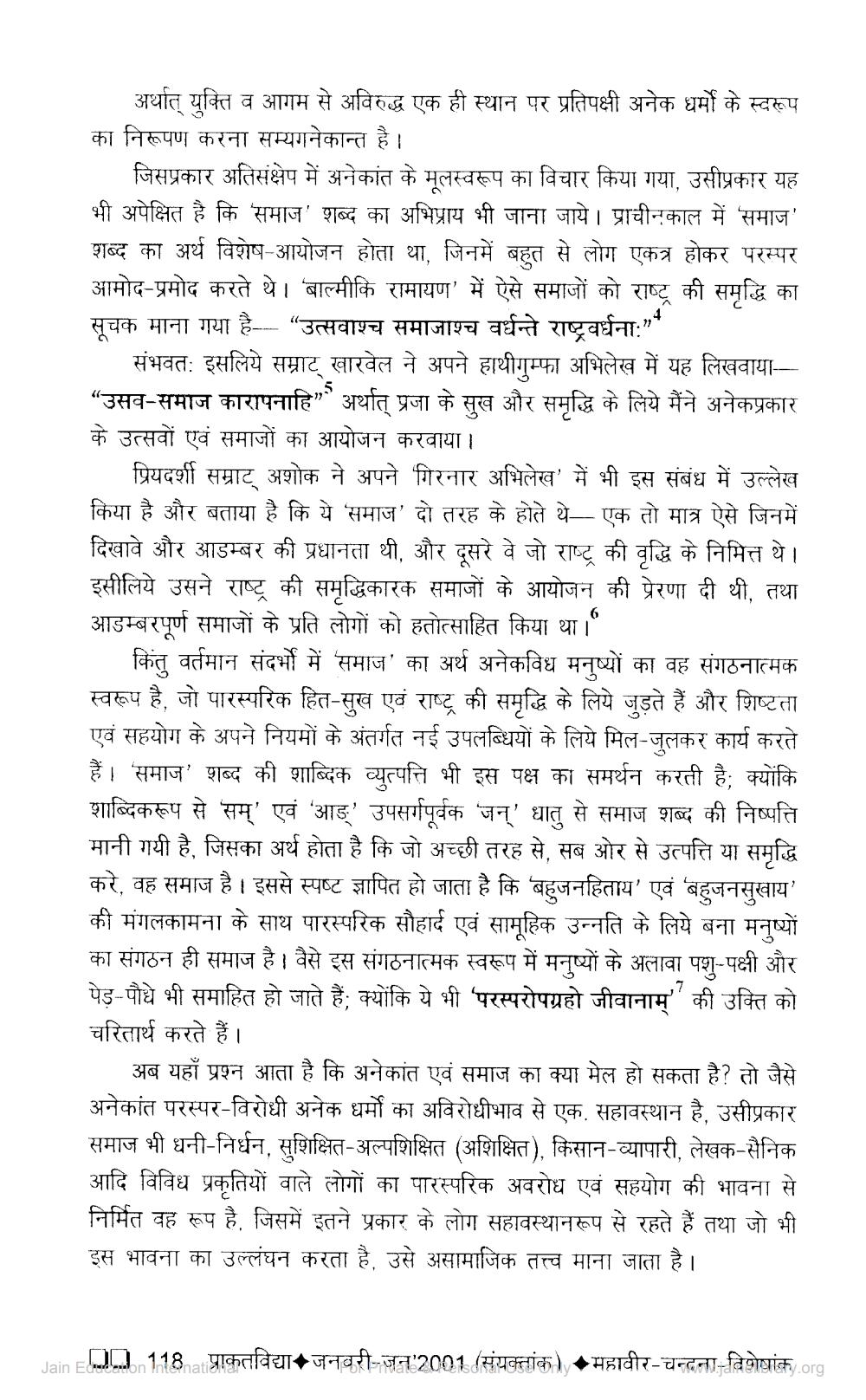________________
अर्थात् युक्ति व आगम से अविरुद्ध एक ही स्थान पर प्रतिपक्षी अनेक धर्मों के स्वरूप का निरूपण करना सम्यगनेकान्त है।
जिसप्रकार अतिसंक्षेप में अनेकांत के मूलस्वरूप का विचार किया गया, उसीप्रकार यह भी अपेक्षित है कि समाज' शब्द का अभिप्राय भी जाना जाये। प्राचीनकाल में 'समाज' शब्द का अर्थ विशेष-आयोजन होता था, जिनमें बहुत से लोग एकत्र होकर परस्पर आमोद-प्रमोद करते थे। बाल्मीकि रामायण' में ऐसे समाजों को राष्ट्र की समृद्धि का सूचक माना गया है- “उत्सवाश्च समाजाश्च वर्धन्ते राष्ट्रवर्धना:""
संभवत: इसलिये सम्राट खारवेल ने अपने हाथीगुम्फा अभिलेख में यह लिखवाया"उसव-समाज कारापनाहि" अर्थात् प्रजा के सुख और समृद्धि के लिये मैंने अनेकप्रकार के उत्सवों एवं समाजों का आयोजन करवाया। __ प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने अपने गिरनार अभिलेख' में भी इस संबंध में उल्लेख किया है और बताया है कि ये समाज' दो तरह के होते थे— एक तो मात्र ऐसे जिनमें दिखावे और आडम्बर की प्रधानता थी, और दूसरे वे जो राष्ट्र की वृद्धि के निमित्त थे। इसीलिये उसने राष्ट्र की समृद्धिकारक समाजों के आयोजन की प्रेरणा दी थी, तथा आडम्बरपूर्ण समाजों के प्रति लोगों को हतोत्साहित किया था।
किंतु वर्तमान संदर्भो में समाज' का अर्थ अनेकविध मनुष्यों का वह संगठनात्मक स्वरूप है, जो पारस्परिक हित-सुख एवं राष्ट्र की समृद्धि के लिये जुड़ते हैं और शिष्टता एवं सहयोग के अपने नियमों के अंतर्गत नई उपलब्धियों के लिये मिल-जुलकर कार्य करते हैं। ‘समाज' शब्द की शाब्दिक व्युत्पत्ति भी इस पक्ष का समर्थन करती है; क्योंकि शाब्दिकरूप से सम्' एवं 'आङ्' उपसर्गपूर्वक जन्' धातु से समाज शब्द की निष्पत्ति मानी गयी है, जिसका अर्थ होता है कि जो अच्छी तरह से, सब ओर से उत्पत्ति या समृद्धि करे, वह समाज है। इससे स्पष्ट ज्ञापित हो जाता है कि 'बहुजनहिताय' एवं 'बहुजनसुखाय' की मंगलकामना के साथ पारस्परिक सौहार्द एवं सामूहिक उन्नति के लिये बना मनुष्यों का संगठन ही समाज है। वैसे इस संगठनात्मक स्वरूप में मनुष्यों के अलावा पशु-पक्षी और पेड़-पौधे भी समाहित हो जाते हैं; क्योंकि ये भी 'परस्परोपग्रहो जीवानाम' की उक्ति को चरितार्थ करते हैं। _अब यहाँ प्रश्न आता है कि अनेकांत एवं समाज का क्या मेल हो सकता है? तो जैसे अनेकांत परस्पर-विरोधी अनेक धर्मो का अविरोधीभाव से एक. सहावस्थान है, उसीप्रकार समाज भी धनी-निर्धन, सुशिक्षित-अल्पशिक्षित (अशिक्षित), किसान-व्यापारी, लेखक-सैनिक आदि विविध प्रकृतियों वाले लोगों का पारस्परिक अवरोध एवं सहयोग की भावना से निर्मित वह रूप है, जिसमें इतने प्रकार के लोग सहावस्थानरूप से रहते हैं तथा जो भी इस भावना का उल्लंघन करता है, उसे असामाजिक तत्त्व माना जाता है।
Jain .. 118 प्राकतविद्या-जनवरी-जन'2001 (संयक्तांक) - महावीर-चन्दना-विशेषांक).org